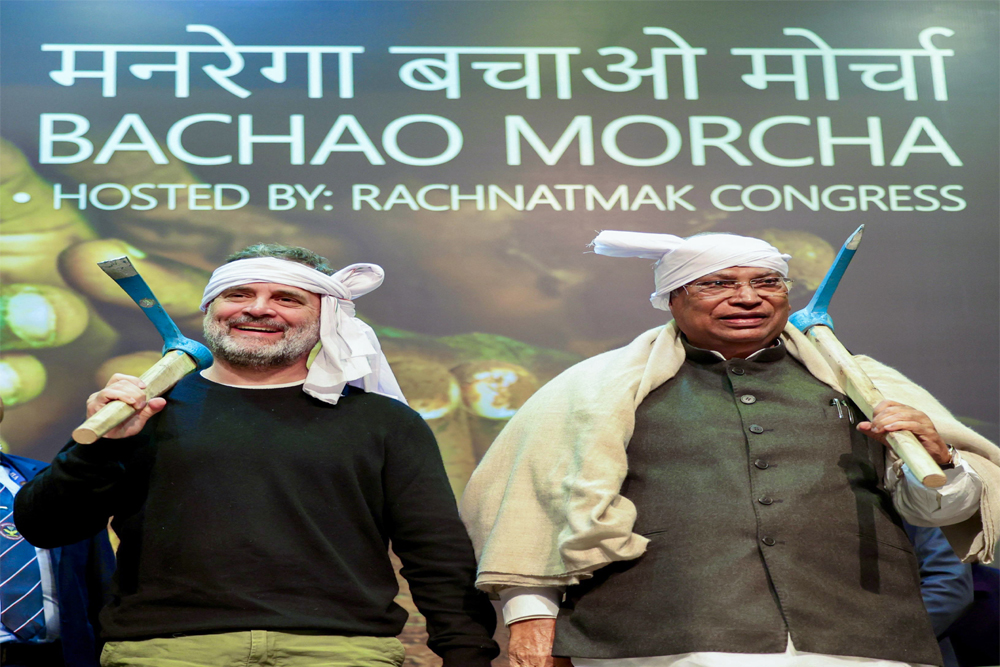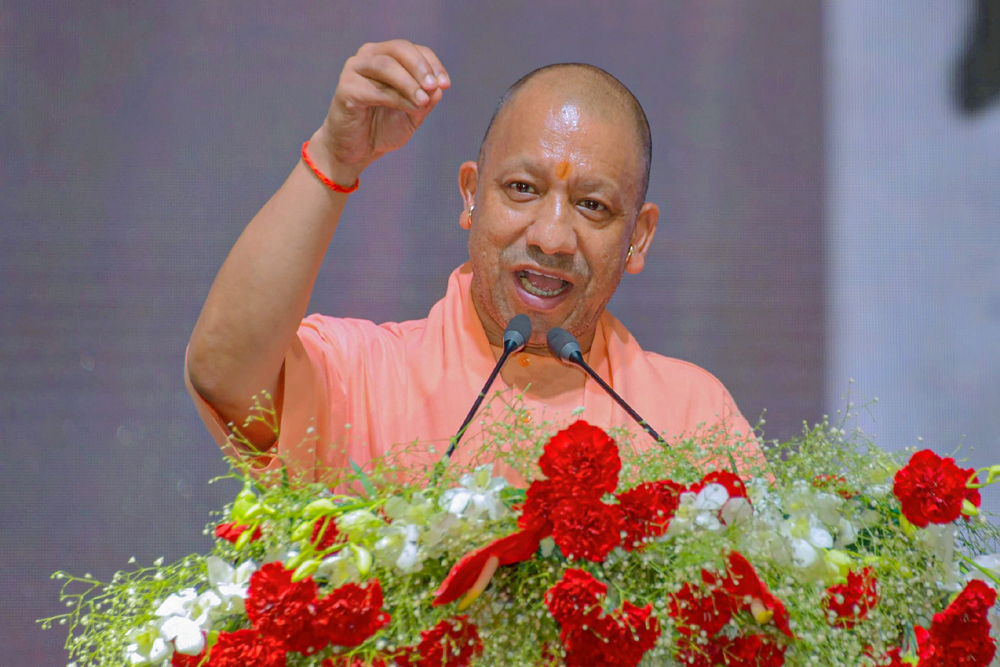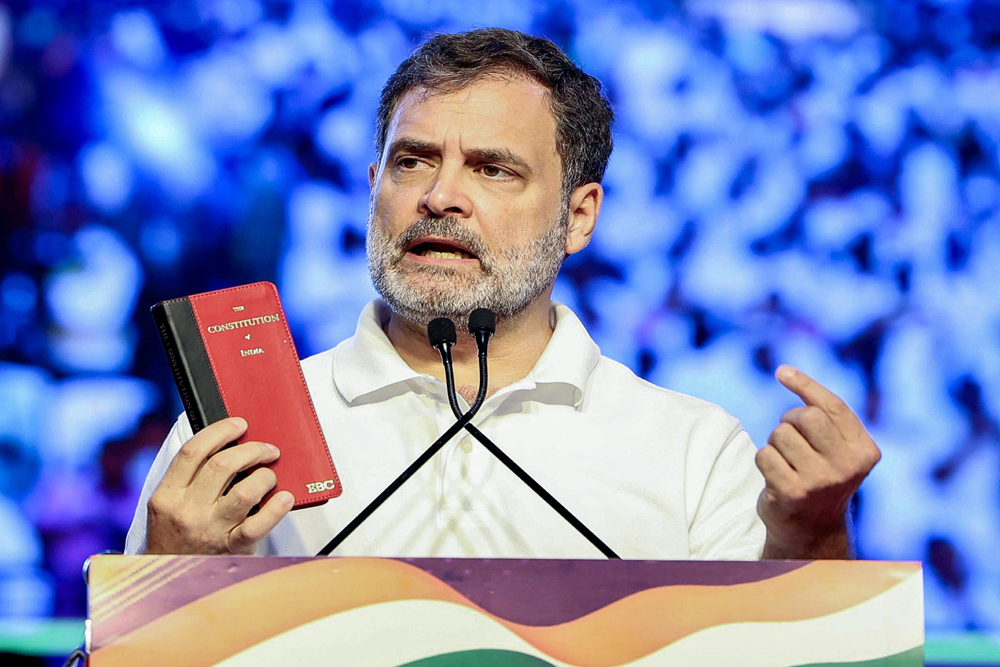दुबई अब महज़ घूमने की एक जगह नहीं है। वह भारत के लोगों का ठिकाना हो गया है। अगर कैलेंडर पर लंबा वीकेंड दिखे, तो तय मानिए कोई न कोई जान-पहचान वाला दुबई के लिए बैग पैक कर चुका होगा। बीते कुछ सालों में यह शहर चुपचाप गोवा और मनाली को पीछे छोड़, शहरी भारतीयों के लिए डिफॉल्ट छुट्टी डेस्टिनेशन बन गया है। अब पहाड़ी कैफ़े की जगह इंस्टाग्राम पर अटलांटिस के पूलसाइड ब्रंच की तस्वीरें छाई रहती हैं। और जब एयर इंडिया दुबई के रिटर्न टिकट उस दाम में देने लगे, जितना श्रीनगर का वन-वे टिकट पड़ता है, तो समझ जाए कि कि रेगिस्तान की उड़ान अब घाटी से भी सस्ती है।
फिर भी, मैं कभी दुबई नहीं गई। ना छुट्टी में, ना काम से, ना ट्रांज़िट में। और आज की ग्लोबल हसल कल्चर में, ये अपने-आप में एक सोशल ऐनोमली लगता है। सच कहूँ तो, मैं दुबई की दीवानगी को समझ नहीं पाई। वो आकर्षण, वो जल्दबाज़ी, वो चमक के पीछे भागना—मुझे कभी समझ नहीं आया। बाकी बहुत से भारतीयों के विपरीत, मुझे दुबई उतना मनभावक, लाभदायक नहीं लगा, जितना अपना दार्जिलिंग या दीव।
लेकिन आज मैं यदि दुबई शहर के बारे में लिख रही हूँ तो जाहिर है कुछ बदला है। एक हेडलाइन ने मेरा ध्यान खींचा: “2025 की पहली छमाही में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 4.6 करोड़ यात्रियों का स्वागत किया, जबकि क्षेत्रीय एयरस्पेस में बाधा भी थी। इसमें से अकेले भारत के 59 लाख यात्री थे।” मतलब बात सिर्फ़ टैक्स-फ्री शॉपिंग या ऊँची इमारतों की नहीं है। यह शहर अब एक मानसिकता बन गया है—एक माइंडसेट। एक ऐसा नज़रिया, जो दिखावे से आगे जाकर कुछ और भी पेश करता है।
मुझे अपने मामा की बात याद आई: “अगर मैंने दो महीने से न्यूज़ नहीं देखी, तब भी मैं बता सकता हूँ किस देश में संकट है—सिर्फ़ यह देखकर कि मेरी बिल्डिंग में कौन नया शिफ्ट हुआ है।” हाल के दिनों में उन्होंने ज़्यादा इज़रायली और फिलिस्तीनी देखे। उससे पहले, रूसी और यूक्रेनी। दुबई अब एक न्यूट्रल ज़ोन बन चुका है—एक भू-राजनीतिक वेटिंग रूम, जहाँ दुनिया के विस्थापित, मोहभंग से भरे और महत्वाकांक्षी लोग आकर रुकते हैं, खुद को फिर से शुरू करते हैं, और फिर थोड़ा और रुक जाते हैं। और इसी सांस्कृतिक मिश्रण में भारतीय सिर्फ़ टूरिस्ट बनकर नहीं आ रहे—वे यहाँ बस भी रहे हैं।
तो आख़िर दुबई इतना आकर्षक क्यों है? क्यों यहाँ बसना अब इतना वाजिब और ज़रूरी सा लगने लगा है?
कभी ये शहर रेगिस्तान के किनारे एक छोटा-सा बंदरगाह था। लेकिन अगर दुबई को समझना है, तो उसकी स्टील और चमक को हटाकर इतिहास में झाँकना होगा। एक समय था जब ये इलाका एक दलदली मैन्ग्रोव क्षेत्र हुआ करता था। फिर आया 1833, जब बनी यास जनजाति के मक्तूम बिन बुत्ती ने यहाँ डेरा डाला और दुबई क्रीक को अपना ठिकाना बना, इसे स्वतंत्र घोषित किया। अल मक्तूम वंश ने व्यापारिक करों को हटाकर भारत और पाकिस्तान से व्यापारियों का स्वागत किया। लेकिन जब जापानी नकली मोतियों ने बाज़ार बिगाड़ा, तब 1966 में तेल की खोज ने दुबई की कहानी को एक नया, काले सोने वाला अध्याय दे दिया।
लेकिन असली क्रांतिकारी मोड़ तेल से नहीं, बल्कि उस पल आया जब तेल की चमक कम होने लगी। तब दुबई टूटा नहीं, उसने खुद को फिर से गढ़ा। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक नया सपना देखा—शहर से बड़े मॉल, खजूर जैसे आकार के आइलैंड्स, और आसमान छूती इमारतें। भविष्य अब तेल से नहीं, पर्यटन से चलेगा। सो अब दुबई की जीडीपी (GDP) का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा टूरिज़्म से आता है—तेल से लगभग दोगुना।
सवाल है अब भी वही, पुरानी दुबई भारतीयों के लिए इतनी आकर्षक क्यों है? इतना ही नहीं अब पश्चिमी दुनिया के लिए भी है? कुछ के लिए यह शहर ग्लैमर है, कुछ के लिए सहूलियत। लेकिन बहुत से भारतीयों के लिए ये है—आकांक्षा बिना बेगानगी के। ये शहर ग्लोबल है, फिर भी अपना-सा लगता है। चिकना है, लेकिन सुलभ भी। शेंगेन वीज़ा जैसी कोई ज़रूरत नहीं। मेट्रो में कोई घूरता नहीं। चाहे आप टेक कंसल्टेंट हों, फ़ैशन इन्फ्लुएंसर या इंदौर से आई एक पाँच लोगों की फ़ैमिली—यहाँ आपके लिए एक जगह है। दुबई आपसे घुलने-मिलने की उम्मीद नहीं करता, वो बस आपको आने देता है।
यहाँ सब कुछ साफ़-सुथरा है, व्यवस्थित है, और अजीब तरह से असरदार। यह ग्लोबल है, लेकिन ठंडा नहीं। यह लक्ज़री है, लेकिन नखरे वाला नहीं। और यह फिनिशिंग टच के बावजूद, कहीं न कहीं भारतीय-सा लगता है।
आज ग्लोबल साउथ से ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स खाड़ी की तरफ़ रुख़ कर रहे हैं। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका से पढ़े-लिखे लोग दुबई को अब मजबूरी में नहीं, पहले विकल्प के तौर पर चुन रहे हैं। वजहें साफ़ हैं—वीज़ा आसान, महत्वाकांक्षा का स्वागत, और सफलता के लिए किसी सांस्कृतिक क्षमा की ज़रूरत नहीं।
खाड़ी की सरकारें भी अब बदली हैं—लॉन्ग टर्म वीज़ा, लचीली रेसिडेंसी, और लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत ख़त्म। खाड़ी अब सिर्फ़ मज़दूरों या यूरोपीय प्रवासियों का अड्डा नहीं, बल्कि इंजीनियर, कलाकार, शिक्षक, वकील, शेफ और एंटरप्रेन्योर के लिए भी खुला है।
पत्रकारों के लिए? शायद अभी तय नहीं। लेकिन इतना तय है कि दुबई अब महज़ एक लेओवर नहीं रहा—यह वह शहर है जहाँ कुछ नया, चमकदार और टिकाऊ बन सकता है। और मैं? मुझे अब भी नहीं पता कि दुबई मेरे भीतर के पत्रकार, उस लेखक जिसे मैं बनना चाहती हूँ, या मेरे पति जो पहले ही फ़ोटोग्राफ़र हैं—उनके लिए क्या रखता है। यह शहर अब हमें आकर्षित करने लगा है, हाँ। लेकिन क्या यह भीतर तक झकझोरता है? इस शहर की चमक के पीछे क्या ऐसे क़िस्सों की जगह है जो ‘क्यूरेटेड’ नहीं हैं? क्या यहां वैसी तस्वीरों की गुंजाइश है जो बिना फ़िल्टर के हों, बिना तमाशे के?
मैं एक करीबी को जानती हूँ जो इस दुबई को अपना घर बनाने का सोच रहा है। और मैं समझ सकती हूँ क्यों? जब एक शहर जो कभी मछलियों और मोतियों का व्यापार करता था, आज सपनों और डिजिटल भविष्य का एक्सपोर्टर बन गया है—तो ये सिर्फ़ ट्रेंड नहीं हो सकता। शायद यह एक बदलाव है। तो क्या मैं जाऊँगी? शायद। लेकिन सिर्फ़ बुर्ज खलीफ़ा की सेल्फ़ी के लिए नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि यह शहर क्यों चर्चा में है—और क्यों, इस बंद होती दुनिया में, दुबई वो जगह बन गया है जो बाहें फैलाकर स्वागत करता है। क्यों लोग एक बार आते हैं, और फिर चुपचाप यहीं बस जाने का फ़ैसला कर लेते हैं।