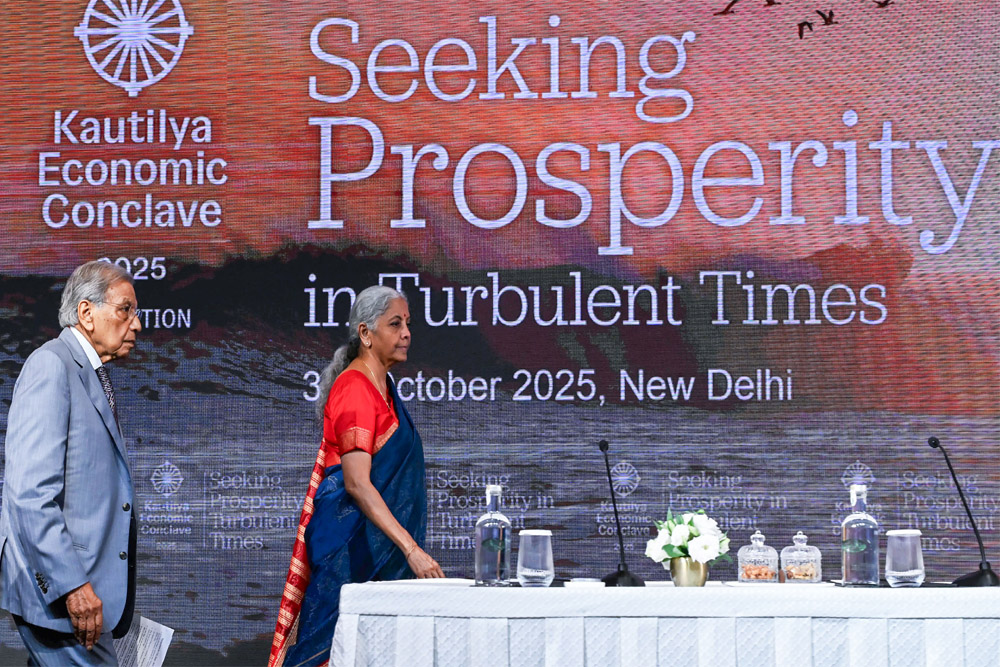बहुत ही अजब दौर में जी रहे है हम। ज़रा नज़र डालिए चारों तरफ—सिर्फ़ अख़बारों की सुर्खियों में नहीं, बल्कि आपके इनबॉक्स में, रात के खाने की मेज़ पर पसरी अजीब चुप्पी में, उन दोस्तों की कसक में जो कभी अपनत्व पर टिके रिश्तों में ढली हुई थी। अब दोस्ती, संबंध असुरक्षा, जलन और अहम की कड़वाहट से भरते जा रहे हैं। आज हर कोई किसी न किसी लड़ाई में उलझा है—व्यक्तिगत, राजनीतिक, और इसीलिए वैश्विक। आख़िर देश भी इंसानों का ही एक बड़ा, बढ़ा-चढ़ा प्रतिबिंब है?
दुनिया आज हर पैमाने पर युद्ध में उलझी हुई है—कहीं बड़ा युद्ध, कहीं छोटा; एक तरफ समुद्री उकसावे, दूसरी तरफ़ सीमाओं के पार मंडराते ड्रोन, या सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले। ग़ज़ा से लेकर यूक्रेन, यमन से म्यांमार, लाल सागर की लहरों से लेकर ताइवान और दक्षिण कोरिया के आसमान तक—दुनिया या तो युद्ध में है या उसके किनारे खड़ी और भयभीत। तभी कूटनीति की भाषा अब और तेज़, और उसके इरादे अब ज्यादा ही धुंधले, खोखले होते जा रहे हैं।
तो यह सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है कि क्या हम स्थाई लड़ाई-झगड़ों, दुश्मनियों के समय में है या उसमें प्रवेश कर रहे हैं और वह भी बिना अहसास के या ठीक से महसूस किए बिना? किसी समय दुनिया मान रही थी कि शीत युद्ध, तनाव, तनातनी सब पीछे छूट चुका है। मतलब दुनिया ने अपना सबसे बुरा दौर देख लिया है। हम संतुष्ट थे—अपने व्यक्तिगत विकास, अपने देश की तरक़्क़ी से। लोकतंत्र, अपनी तमाम खामियों के बावजूद, एक तरह का संबल था। पड़ोसियों से रिश्ते सहज भले न हों, पर संवादपूर्ण थे। व्यापार फल-फूल रहा था, पूंजी घूम रही थी, देशों के बीच आवाजाही पर निगरानी तो थी, पर हर दस्तक संदेह की तरह नहीं देखी जाती थी।
मेरी पीढ़ी जो, एयरपोर्ट लॉन्ज़ और विदेशी डिग्रियों के बीच पली-बढ़ी का भूमंडलीकरण के जोश में साफ लगा था कि शीत युद्ध की परछाइयाँ अब पुरानी अलमारियों में बंद हो चुकी हैं। उदार लोकतंत्र और व्यापार समझौते भविष्य में स्थिरता बनाए रखेंगे। लेकिन कहां है वह स्थिरता, अमनचैन? अब सभी को साफ दिख रहा कि समझ नाज़ुक है और भूलक्कड़ भी। और चुपचाप दुनिया बदल गई। हम भी, पीढिया भी।
आज की हवा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की कूटनीति जैसी नहीं, बल्कि उन्नीसवीं सदी के यूरोप जैसी लगती है—जहाँ साम्राज्य टकराते थे, गठबंधन खोखले होते थे और हर हाथ मिलाने में एक छुपी हुई साजिश, तलवार का खटका होता था। तब ब्रितानी साम्राज्य था, फ़्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी थे। आज वह शतरंज की बिसात अमेरिका, चीन, रूस, योरोप, इजराइल और एक नए तेवर वाले पश्चिम एशिया के हाथ में है।
हम फिर उसी दौर में आ पहुँचे हैं जहां वर्चस्व की होड़ है तो गुटबाज़ियाँ, राष्ट्रवाद का जोश, और दोस्तियों के पर्दे में छुपी दुश्मनियों की परते है। हर देश अपनी आरामगाह से झटका खाकर बाहर आ गया है। कल सुबह ही कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा संघर्ष हुआ। इस लेख के लिखे जाने तक, थाईलैंड ने कंबोडिया से लगती सारी सीमाएँ बंद कर दी। और अपने F-16 लड़ाकू विमान सीमा पर तैनात कर दिए थे। कुछ ही महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी थी।
रूस और यूक्रेन की लड़ाई थमी नहीं है—लाशें अब भी गिर रही हैं। इजराइल युद्ध में है—ईरान से, सीरिया से, हमास से, लेबनान से; और सच तो यह है कि जब तक उसे सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा, वह पूरे पश्चिम एशिया से भिड़ने को तैयार है। और फिर चीन तथा अमेरिका हैं—एक शीत युद्ध में फंसे हुए, जो कभी धीमा होता है, तो कभी उबलने लगता है—इस पर निर्भर करता है कि व्हाइट हाउस में कौन बैठा है।
पर इस नए युद्धकाल में लड़ाइयाँ सिर्फ़ ज़मीन पर ही नहीं लड़ी जा रहीं। वे कोड में लिपटी हैं, क्लाउड में छिपी हैं। साइबरस्पेस में, व्यापार प्रतिबंधों में, रणनीतिक कर्ज़ जाल में, प्रॉक्सी मिलिशिया और ड्रोन हमलों में। इन लड़ाईयों को मीडिया चैनलों पर लड़ा जा रहा हैं, सोशल मीडिया पर, मुद्रा अवमूल्यन में, तकनीकी गलियारों में। पर हैं वे युद्ध ही—थकावट के युद्ध, वर्चस्व के युद्ध, कथानक और कल्पना में भी जंग।
और जैसा कि हर टकराव के दौर में होता है, सबसे पहले पिसती हैं कमज़ोर और छोटी राज्य व्यवस्थाएँ। अस्थिर देश मोहरे बन जाते हैं। शांति-स्थापन का दावा धीरे-धीरे भागीदारी में बदलता है। क़ानून की परिभाषाएँ दबाव में लचकने लगती हैं। हम भले ही किसी घोषित “विश्व युद्ध–3” की स्थिति में नही हों, पर हम निश्चित ही उस दौर में हैं जिसे फ़रीद ज़कारिया ‘एज ऑफ रिवोल्यूशन्स’ कहते हैं। या जैसा मार्क लियोनार्ड लिखते हैं—‘The Age of Unpeace’, जहाँ “जुड़ाव ही टकराव की वजह बनता है।”
जितना अधिक हम जुड़े हैं, उतने ही कमज़ोर हो गए हैं। सभी के लिए लिए यह दौर ‘टूटन का युग’ है—fractures और fissures का।
हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध के अंत की 80वीं वर्षगाँठ पर YouGov के एक सर्वे में, बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के नागरिकों ने माना कि उन्हें लगता है, अगले दस वर्षों में तीसरा और शायद और भी ज़्यादा विनाशकारी युद्ध छिड़ सकता है। ज़्यादातर ने इसके लिए रूस को दोषी ठहराया।
पर यह नज़रिया बहुत संकीर्ण है। अस्थिरता एक देश से नहीं, हर तरफ़ से आ रही है। क्योंकि आज की दुनिया अब दो ध्रुवीय नहीं, बल्कि बेरहम बहुध्रुवीय हो चुकी है। US और USSR की तरह साफ़-सुथरे खेमे नहीं बचे। टकराव अब सबके बीच है। जैसे- चीन बनाम पश्चिम, रूस बनाम नेटो, भारत बनाम चीन और पाकिस्तान, ईरान बनाम इजराइल, सऊदी बनाम ईरान, इजराइल बनाम पूरा मध्य एशिया।
हर रंगमंच की अपनी पीड़ा है, अपनी ऐतिहासिक स्मृति, और हिंसा की अपनी सीमा। रोकथाम के पुराने बंदोबस्त (deterrence) और कूटनीति के ढांचे अब थके-हारे से लगते हैं। संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूटीओ (WTO) जैसे बहुपक्षीय संस्थान चरमराने लगे हैं। व्यापार की संधियाँ टूट रही हैं। जाहिर है “नियम आधारित व्यवस्था” जैसे शब्द अब गंभीर नहीं बल्कि दिखावे के लगते हैं।
लेकिन चलिए अब ज़ूम आउट की बजाय जरा उल्टा ज़रा भीतर झाँके—अपने आसपास के समाज, निजी संसार में। हमारे घरों की नाराज़गी, सड़कों की आक्रामकता, दोस्तियों की चुप्पी—क्या ये सब एक ही कहानी नहीं हैं? पैमाना भले अलग है। पर अविश्वास और असुरक्षा जब हमारी आपसी समझ को परिभाषित करने लगे, तो इसमें क्या आश्चर्य कि देश और देशों के रिश्तों में भी वही होने लगें? दुनिया सिर्फ़ बाहर युद्ध में नहीं है। हमारे, सामाजित रिश्तों, भीड़ के भीतर भी संघर्ष भले है। आज समय ही ऐसा है—जहाँ हर पल किसी टकराव की आशंका हमारे सिर पर मंडराने लगती है। और यदि हमने अभी रुककर सोचना नहीं सीखा, तो हम जल्द ही सब कुछ के प्रति असंवेदनशील हो जाएँगे।
यों मुड़कर देखने का मोह ज़रूर है लेकिन शायद अब यह समय है कि और गहराई से देखे, समझे।
समय सिर्फ़ यह नहीं पूछने का है कि “क्या हो रहा है?” बल्कि यह पूछने का है कि “क्यों होने दे रहे हैं हम?” क्योंकि झगड़े छोटे हो या जंगी युद्ध, सिर्फ़ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते।
वे हर जगह पनपते हैं। और अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है, तो वह यह है कि जब युद्ध के नगाड़े धीमे-धीमे बजने लगें, तो ध्यान से सुनिए। सबसे ज़ोर का धमाका बाद में आता है।
इतिहास की सबसे अहम सीख यही है कि गढ़ना और बिगाड़ना दोनों हमारे हाथ में होता है।