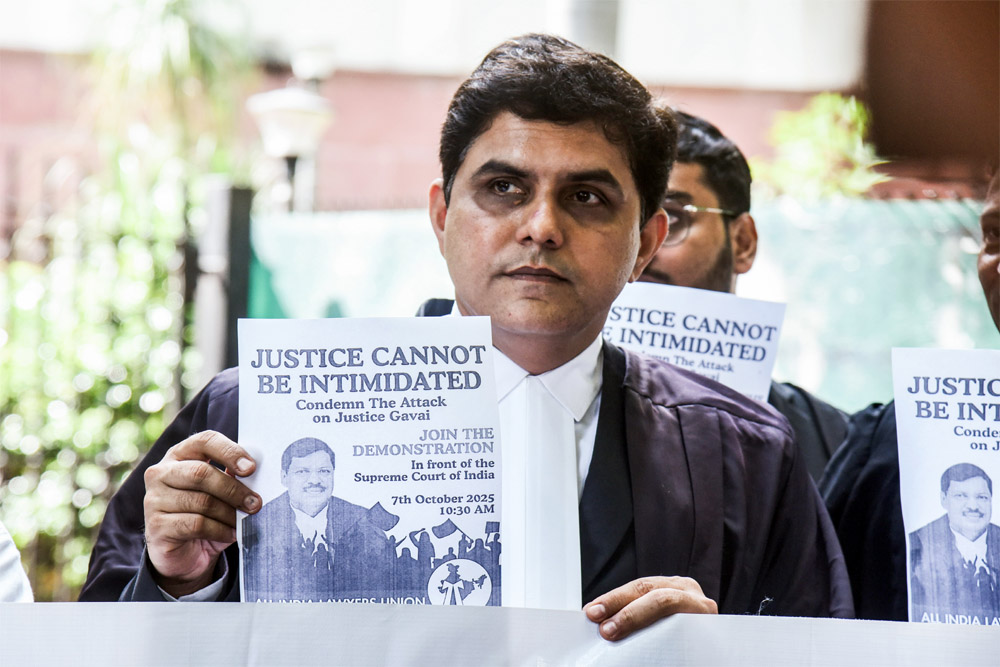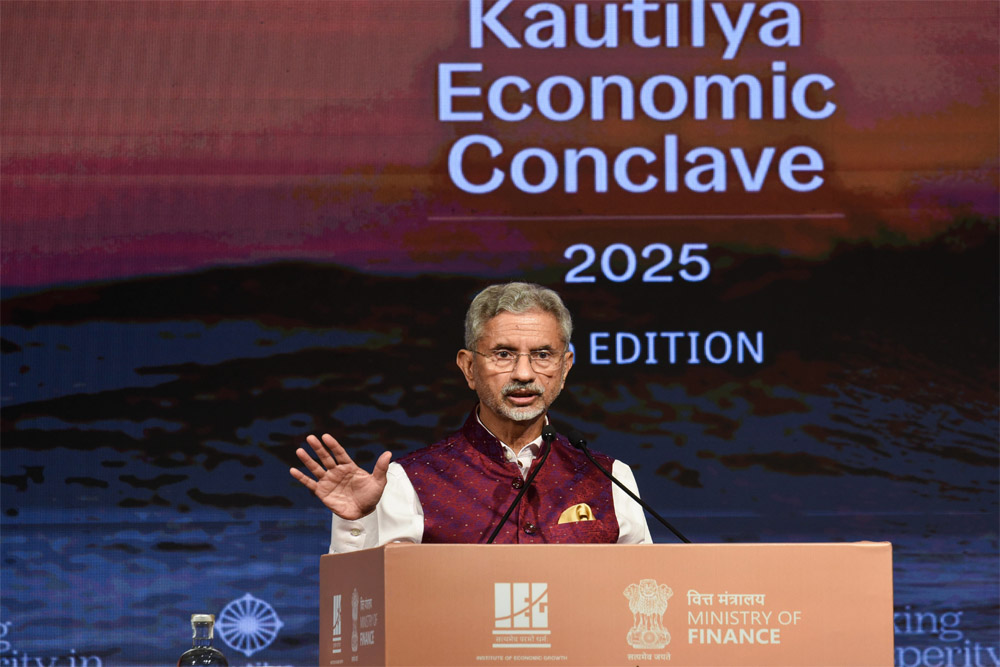समस्या रोजगार की सरकारी परिभाषा है। भारत में जो परिभाषा अपनाई गई है, वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए भारत में जो आंकड़ा दिया जाता है, उनकी तुलना अन्य देशों के आंकड़ों से नहीं की जा सकती।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 50 ऐसे अर्थशास्त्रियों के बीच सर्वे किया, जो भारत सरकार से संबंधित किसी पद पर नहीं हैं। सर्वे में इन ‘स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों’ से भारत में बेरोजगारी की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष यह निकला कि भारत सरकार का बेरोजगारी संबंधी आंकड़ा सही नहीं है। बल्कि इन आंकड़ों के जरिए बेरोजगारी और अर्ध-रोजगार की गंभीर स्थिति पर परदा डाला जा रहा है। अर्थशास्त्रियों में आम राय उभरी कि भारत भले दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था हो (इस वर्ष जनवरी-मार्च में आर्थिक वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रही), मगर ये आर्थिक वृद्धि दर पर्याप्त संख्या में नियमित वेतन वाली नौकरियां पैदा करने में नाकाम है। जबकि हर वर्ष लाखों की संख्या में नौजवान रोजगार बाजार में प्रवेश कर रहे हैँ।
सर्वे में शामिल 37 अर्थशास्त्रियों ने राय जताई कि सरकार के आंकड़े जितनी बेरोजगारी बताते हैं, असल में ये दर उससे दोगुना तक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत थी। विशेषज्ञों के मुताबिक समस्या रोजगार की सरकारी परिभाषा है। भारत में जो परिभाषा अपनाई गई है, वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए भारत में जो आंकड़ा दिया जाता है, उनकी तुलना अन्य देशों के आंकड़ों से नहीं की जा सकती। भारत में हफ्ते में एक घंटा काम करने वाले व्यक्ति को रोजगार-शुदा मान लिया जाता है। उधर कृषि जैसे घरेलू कारोबार में हाथ बंटाने वाली महिलाओं को भी रोजगार-शुदा माना जाता है, जबकि उन्हें काम के बदले कोई भुगतान नहीं होता।
तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव की यह टिप्पणी महत्त्वपूर्ण हैः ‘बेरोजगारी हमारी एक बड़ी चुनौती है और मैं नहीं मानता कि सरकारी आकंड़े जमीनी स्थिति की सही झलक देते हैं।’ ऐसा नहीं है कि यह बात पहली बार सामने आई हो। दरअसल, भारत सरकार के रोजगार संबंधी तथा अन्य आर्थिक आंकड़ों पर संदेह का साया लगातार गहराता गया है। मगर उनसे मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर, जैसाकि एक विशेषज्ञ ने कई वर्ष पहले कहा था, मौजूदा सरकार का मकसद अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि आर्थिक सुर्खियों को चमकाना भर है।