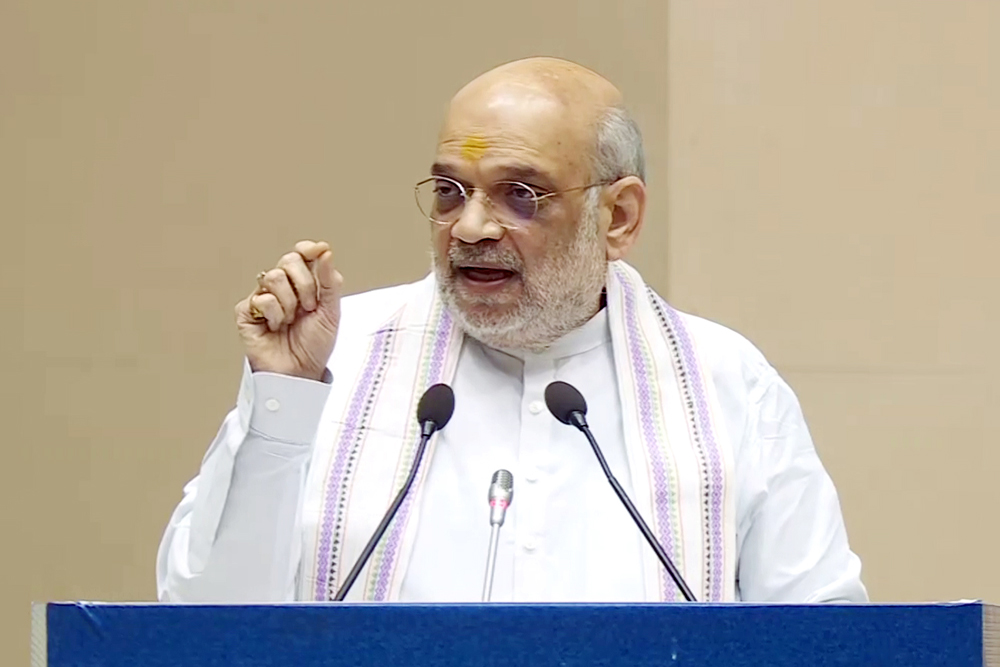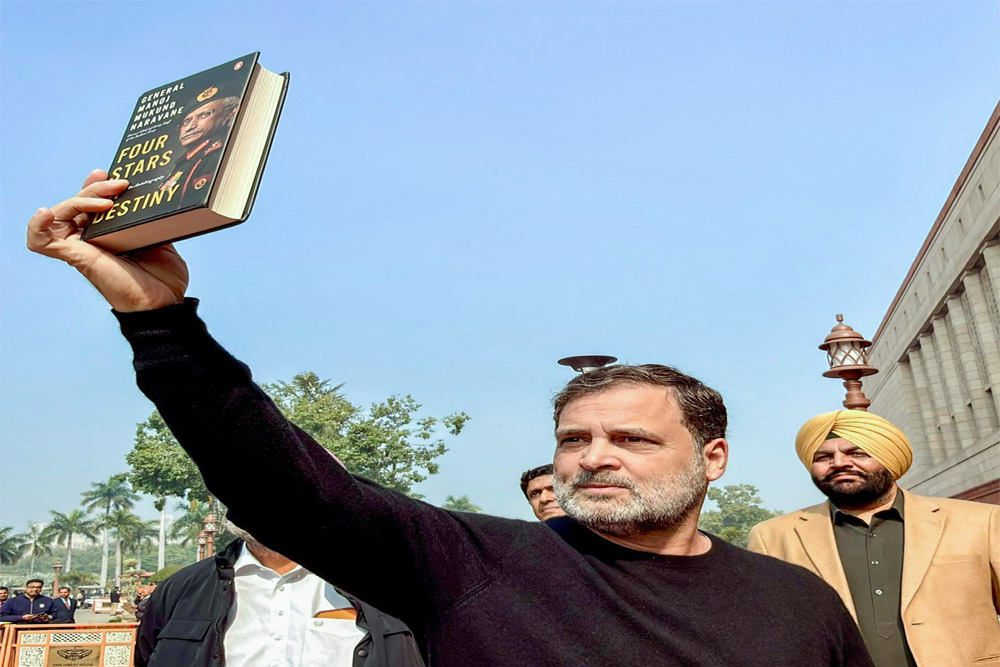कथित जातीय उत्पीड़न के मामले अक्सर सामने आते हैं। मामला शांत होने तक हर बार यही चर्चा होती है कि आज भी किस हद तक जातिगत भेदभाव फैला हुआ है। मगर ऐसी चर्चाएं कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचतीं।
हरियाणा कैडर के आईपीएस वाई. पूरन कुमार की आत्म-हत्या को संस्थागत जातीय उत्पीड़न की मिसाल बताया गया है। कुमार ने सात अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने 15 वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए। स्वाभाविक है कि मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इसी समय मध्य प्रदेश की एक घटना भी सुर्खियों में है। इसके मुताबिक दमोह जिले में एक ओबीसी युवक को कथित रूप से जबरन एक ब्राह्मण व्यक्ति का पैर धोकर पानी पिलाया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक संगठनों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया।
ये घटनाएं कोई अजूबा नहीं हैं। अक्सर विभिन्न क्षेत्र के संस्थानों से लेकर गांव-देहात तक से कथित जातीय उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। जब तक मामला शांत नहीं होता, उसको लेकर यही चर्चा होती है कि भारतीय समाज में आज भी जातिवाद और जातिगत भेदभाव फैला हुआ है। मगर ऐसी चर्चाएं कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचतीं। कुछ जातियों को उत्पीड़क बता कर या “सदियों से मौजूद जातीय उत्पीड़न” की चर्चा कर “इंसाफ के पैरोकार” आगे बढ़ जाते हैं। वे यह सवाल नहीं उठाते कि सौ-डेढ़ सौ साल से इसी तरह का विमर्श जारी रहने, संविधान में तमाम भेदभाव खत्म करने के स्पष्ट प्रावधान होने और साढ़े तीन दशक से “सामाजिक न्याय” की राजनीति के हावी रहने के बावजूद हालात क्यों नहीं बदले हैं?
ये कठिन और असहज करने वाले प्रश्न हैं। इनकी तह में जाने पर नजर आएगा कि खुद किस तरह जातिगत पहचान और प्रतिनिधित्व को “सामाजिक न्याय” का पर्याय बना कर इसके पैरोकारों ने सारा विमर्श जातिवाद पर केंद्रित कर दिया है। इससे वंचित समूहों के बीच व्यापक एकता और समाज के आधुनिकीकरण की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। नतीजतन, “जाति के विनाश” का वह लक्ष्य पीछे छूट गया है, जिसे केंद्र में रखकर आधुनिक भारत के निर्माण की परियोजना शुरू की गई थी। इससे कुछ नेता-परिवारों और मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को अवश्य लाभ हुआ है, मगर जातिवाद या जमीनी स्तर पर जातीय भेदभाव को खत्म करने का मार्ग और बाधित ही हुआ है।