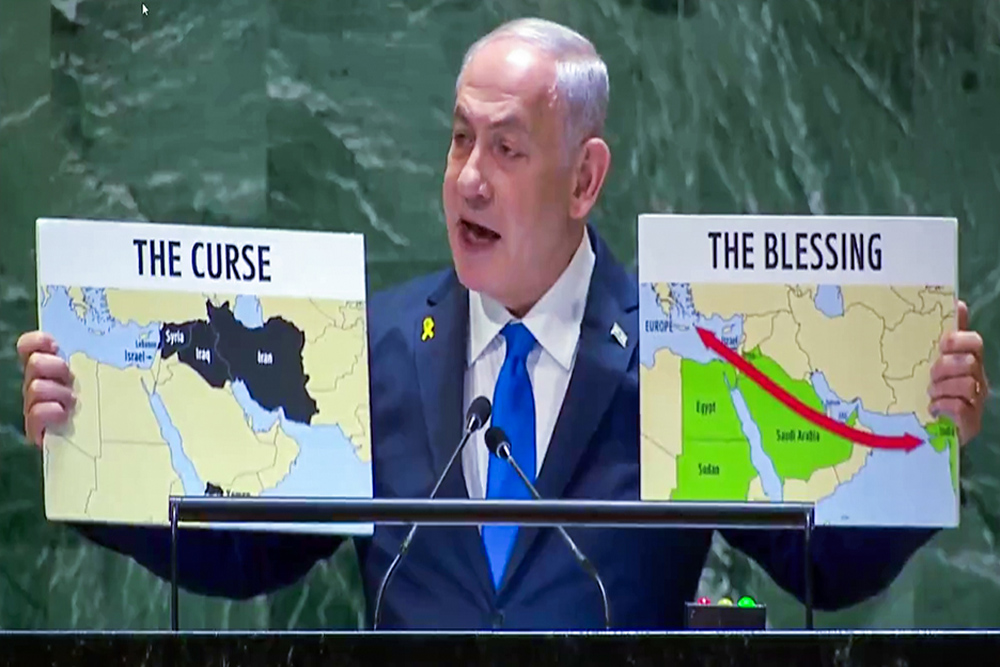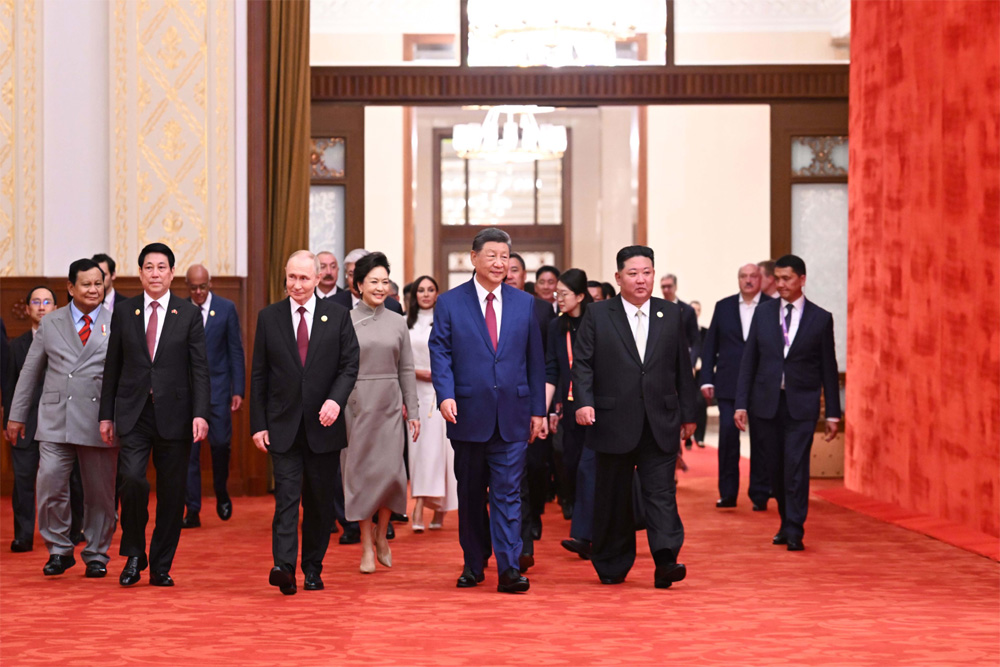“कश्मीर की फिर से कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए क्योंकि वह बदलता नही वह तो हिंसा और आतंक की ज़मीन है।”
यह वाक्य मैंने दिल्ली के एक ‘बौद्धिक’ की ज़ुबान से से सुना है, वो जिसने खुद कश्मीर को सिर्फ दूर से देखा है, और उसे हमेशा आंदोलन, संघर्ष में ही फंसा समझा है। उसके लिए कश्मीर एक सूबा, भूमि नहीं बल्कि एक रूपक है। जहाँ खूबसूरती और कांटेदार तारें इतनी गुथमगुथा है कि कविता बन जाए। जहाँ हर धमाका एक नया कॉलम, एक नई बहस जन्म देता है। तभी कश्मीर को फिर से, नए अंदाज में सोचना, उसकी कल्पना करना उसके लिए और उन जैसे कई बुद्धीजीवियों के लिए अपने नैरेटिव को खो बैठना है। अगर कश्मीर में संर्घष और खून-खराबा बंद हुआ मान ले, आम जीवन में अमन-चैन आया माने तो तब लुटियन दिल्ली के ड्रॉइंग रूम में बातें किस पर होंगी?
छह साल हो गए उस बड़े, विवादित और निर्णायक फ़ैसले को—जब अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया गया। लेकिन क्या तब से कश्मीर को देखने का हमारा नज़रिया बदला है? क्या हम उस थके हुए मुहावरे—संघर्ष क्षेत्र, खोया स्वर्ग—से आगे निकल पाए हैं? क्या हम वादी को अब प्रतीक नहीं, एक असल जगह की तरह देखने लगे हैं?
क्योंकि अब यह कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं रही। अब बात ज़मीन की नहीं, बल्कि नज़रिए की है। हम कश्मीर को कैसे देखते हैं—या नहीं देखते हैं—यह असली सवाल है। यह सोच की लड़ाई है।
कई दशकों से कश्मीर भारत की सामूहिक कल्पना में एक अमूर्त विचार रहा है—एक घाव जिसे रोया जाए, एक ट्रॉफी जिसे दिखाया जाए, एक मंच जहाँ ग़ुस्सा खेला जाए। न्यूज़रूम से लेकर थिंक टैंक और टॉक शो तक, कश्मीर को अक्सर ‘अभिनय’ की तरह पेश किया गया, समझने की कोशिश कम हुई। हिंसा, अशांति, अराजकता ठीक लगती है—वह प्राइमटाइम और ट्विटर के एल्गोरिद्म को खिलाती है। जबकि शांति, सबकुछ सामान्य होने की बात असहज कर देती है— कश्मीर घाटी राय नहीं, सहानुभूति माँगती है। इसीलिए वादी को अक्सर दो रंगों में ही समेटा गया है: खून या मातम, पीड़ित या गुनहगार। कश्मीर की कई कहानियाँ हैं—हर एक को अलग-अलग ढंग से सुनाया गया, सजाया गया, दोहराया गया, पर शायद ही कभी नया जोड़ा गया।
हकीकत है कि हम सब कश्मीर पर बोलते हैं, पर कश्मीर से शायद ही कभी।
इतिहास हमें बताता है—कानून एक रात में बदल सकते हैं, लेकिन मानसिकता बदलने में समय लगता है। दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद खत्म हुआ, सामाजिक दीवारें फिर भी बरकरार रहीं। बर्लिन की दीवार गिरी, लेकिन ‘वेस्सी’ और ‘ओस्सी’ के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी वर्षों तक बनी रही। भारत की चुनौती भी कुछ अलग नहीं। कागज़ पर कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन हमारी कल्पना में, आज भी वो ज्यों का त्यों है।
फिल्में भी इस सोच को तोड़ नहीं सकीं। ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘आर्टिकल 370’ जैसी फिल्में वादी को एक मंच बना देती हैं—शोक, क्रोध और प्रतिशोध का। सिनेमा कम, आत्ममंथन ज़्यादा। पर इनमें वो सब ग़ायब है, जो किसी जगह को जीने लायक बनाता है। हम शायद ही कभी देखते हैं कि कश्मीरी लोग कैसे रोज़ जीते हैं, कैसे सांस लेते हैं। मैं आज भी एक ऐसी कहानी ढूंढ रही हूँ जहाँ कश्मीर शोक में नहीं, बल्कि आशा में हो। जहाँ मोहब्बत पोलो मार्केट की परछाई में फूले, जहाँ शायरी डल के किनारे कॉफी के साथ बहे।
हम कश्मीर को एक समाज नहीं, एक तमाशा मानना ज़्यादा सहज पाते हैं।
राजनीति भी उसी पुरानी स्क्रिप्ट से चिपकी हुई है। जो लोग दशकों से कश्मीर के दर्द पर अपने करियर बनाते रहे, उनके लिए यह बदलाव पचाना आसान नहीं। दिल्ली की तुष्टीकरण नीति ने श्रीनगर की शिकायतों की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक पोषित किया। पीड़ित होना एक आदत हो गई। जबकि अनुच्छेद 370 का अंत सिर्फ स्वायत्तता नहीं बल्कि एक पूरे ‘प्रणालीगत महत्वहीनता’ के ढांचे को हिला गया है। पार्टियाँ उस दर्द को अब चुनावी नारों में बदलने लगीं। दिल्ली के अभिजात्य वर्ग ने भी ‘विशेष दर्जा खत्म होने’ पर आंसू बहाए, बिना यह पूछे कि वह दर्जा आख़िर लेकर क्या आया?
कश्मीर की त्रासदी महज़ राजनीतिक विफलता नहीं थी—यह एक गलत समझ थी। एक ऐसा इलाक़ा जो दबिस से शासित रहा, लेकिन उससे भी खतरनाक रूप से गलत समझा गया—भावनात्मक, बौद्धिक और नैतिक रूप से।
और फिर भी, छह साल बाद, एक शांत सच उभरने लगा है। प्रदर्शन में नहीं, ठहराव में। ग़ुस्से में नहीं, आत्मचिंतन में। पहले वादी हड़तालों और कर्फ्यू की धुन पर चलती थी। स्कूलों के बंद रहने के दिन ज़्यादा होते थे। पूरा मोहल्ला ‘कनेक्शन’ की फुसफुसाहट के नीचे जीता था। डर कोई पल नहीं, एक माहौल था। 2017 में एक मौजूदा विधायक ने एक परिवार का मज़ाक उड़ाया, जिसके सदस्य J&K पुलिस में भर्ती हुए थे—”हिंदुस्तान ने आपके बाप को इस्तेमाल किया”—ये दिखाने के लिए कि कैसे पुनः एकीकरण को भी उपहास का विषय बनाया जा सकता है।
आज उस हवा में फर्क है। विकास दिखता है। स्टार्टअप्स फल-फूल रहे हैं। पुराना दोबारा बनाया जा रहा है; नया बिंदास आधुनिक है। जो पत्थरबाज़ कभी विद्रोही माने जाते थे, वही अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सराहना करते हैं। लड़कियाँ अब गोल्फ खेलना सीख रही हैं, कैफ़े ग़ैर-राजनीतिक बातचीतों से गुलज़ार हैं। हाँ, डर पूरी तरह नहीं गया है—पर अब वो मौसम नहीं तय करता। क्या यह शांति है? शायद नहीं। पर यह वो अशांति, अराजकता भी नहीं, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी।
और तभी, जब कुछ सकारात्मक आकार लेने लगता है, कल्पना फिर घोंट दी जाती है।
दो महीने पहले, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनिर ने फिर एक रटा-रटाया भाषण दिया। वही पुराने नारे, वही ऊंची आवाज़ें—”हमारा धर्म, हमारी रिवायतें, हमारे मक़सद अलग हैं… हम दो कौमें हैं।” शोर ज़रूर था, पर ऊर्जा नहीं। एक स्क्रिप्ट जो दशकों से नहीं बदली क्योंकि रावलपिंडी बदलना नहीं चाहता। पाकिस्तान के लिए कश्मीर लोग नहीं, एक बहाना है—अपनी अंदरूनी सड़न से ध्यान हटाने का ज़रिया।
और उसके कुछ ही दिनों बाद, कश्मीर का मूड फिर गहराने लगा। डर और दुःख की परछाई हवा में घुल गई। भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर फिर एक मनोवैज्ञानिक टकराव में उलझ गए और एक झटके में, कश्मीर फिर ‘संभावना’ से ‘संकट’ में बदल गया। सुर्खियों से विकास गायब, डर लौट आया। और वो पुरानी, बेरहम फुसफुसाहट फिर लौट आई—कश्मीर बदल नहीं सकता। कश्मीर को लहूलुहान रहना होगा।
यहीं सोच कर दरवाज़े फिर बंद हो जाते हैं। जो धीमी सी उम्मीद उगने लगी थी, उसे डर फिर कुचल देता है। लेकिन इस बार, वह पूरी तरह मिट नहीं गई।
क्योंकि कुछ अड़ियल, इस बार टिक गया है।
हर तरफ से उकसावे के बावजूद, कश्मीर ने खुद को हताशा में नहीं डुबोया। कुछ शांत, स्थायी आकार ले रहा है। विरोध में नहीं, ठहराव में। ग़ुस्से में नहीं, सवालों में। युवा कश्मीरी अब सवाल करने लगे हैं—हम किन नेताओं की विरासतों को आज भी मनाते हैं जिन्होंने हमें भ्रम में डाला? हम लड़ किसके लिए रहे थे—और हमारे लिए कौन लड़ रहा था? इस तरह सोचना भी बदलाव को झलकाता है एकजुटता के पलों में। जब पहलगाम में आतंकवाद ने हमला किया, कश्मीर ने बाकी देश के साथ शोक मनाया—विरोध नहीं, साझे दुःख में। शायद यही है असली बदलाव। ना कानूनों में, ना नारों में—बल्कि दुःख के साझेपन में।
पर देश के ज़्यादातर हिस्सों में यह बदलाव अब भी पंजीकृत नहीं हुआ है। कश्मीर अब भी एक तारांकन चिन्ह के साथ आता है। उसे अब भी या तो ग़ुस्से में या मातम में देखा जाता है—सिर्फ जीते हुए नहीं।
और स्पष्ट कर दें—यह अनुच्छेद 370 का शोकगीत नहीं है, और ना ही अंध राष्ट्रवाद का भजन। यह एक नज़रिए की पुनरावृत्ति है। असली एकीकरण झंडों या टूरिज़्म वीडियोज़ से नहीं आएगा। वह तब आएगा जब किसी कश्मीरी की महत्वाकांक्षा को ‘सामान्य’ माना जाएगा, ‘असाधारण’ नहीं। जब दिल्ली स्थिरता को एक प्रदर्शन नहीं, एक स्थिति मानेगी। जब कश्मीर अपनी आवाज़ उन्हीं लोगों को नहीं देगा जो उसकी पीड़ा से फलते-फूलते हैं। जब कश्मीर के बदलाव की कहानियाँ चमत्कार नहीं, क्षण बनकर बताई जाएंगी। और जब भारत, कश्मीर के लिए बोलना बंद करके, उसे सुनना शुरू करेगा।
क्योंकि जब तक हम खुद कश्मीर को ले कर फिर से कल्पना नहीं करते, दुनिया भी नहीं करेगी। छह साल में क़ानून ज़रूर बदला है। लेकिन मानसिकता? वो अब भी अंतिम मोर्चा है। और जब तक हम कश्मीर को सिर्फ उसके सबसे बुरे दिन से देखेंगे तब तक हम कभी उसकी सबसे अच्छी सुबह की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे।