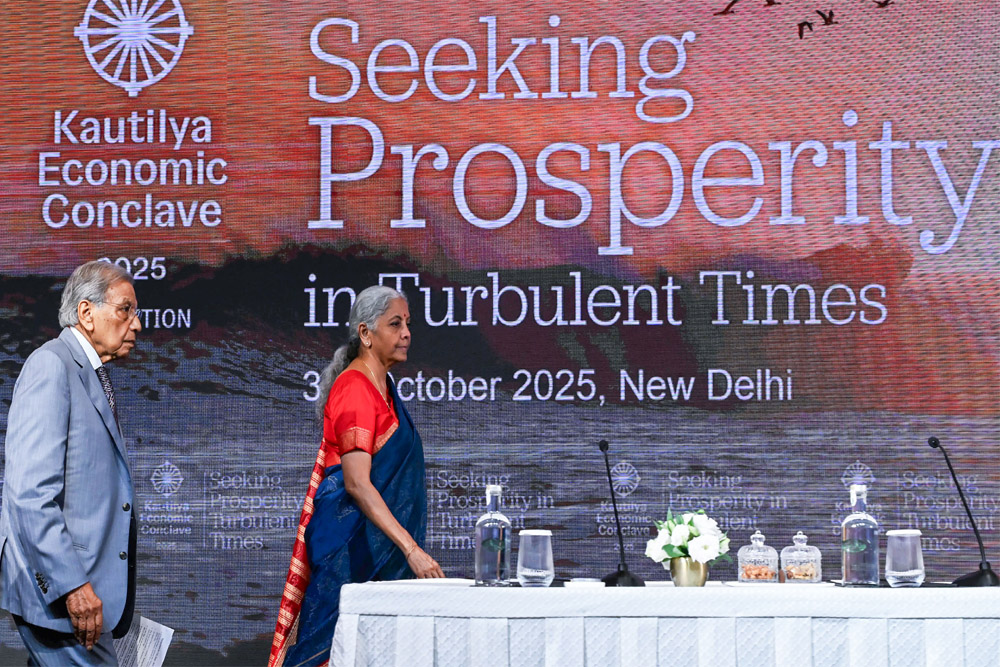कुछ दिनों से मैं मुंबई में हूँ। यह महानगर उभरते भारत की झिलमिलाहट बतलाता हुआ है। काँच की इमारतें मानसून के आसमान को छूती हैं। नया कोस्टल रोड अरब सागर पर किसी रिबन की तरह खुलता चला जाता है। यह वही शहर है जो न्यूयॉर्क बनने का सपना देखता है। तभी लगातार निर्माणाधीन स्काइलाइन, वॉल स्ट्रीट के ब्रोकरों जैसी दौड़-भाग, ब्रॉडवे जितने चमकीले फिल्म सितारे, और वे कैफ़े, जहाँ स्टार्टअप की बातें गूँजती रहती हैं। मुंबई उस वैश्विक चमक को छूना चाहती है और वह न कभी सोता है और न थमता है। हमेशा भागता है, हमेशा ऊपर उठने को तत्पर।
फिर भी, चमक फीकी-सी लगी। शायद एक वजह लगातार बरसात थी। लगातार भारी बादल, चिपचिपी नमी जो देह से चिपकी रहती है, वे गड्ढे जो पूरी गाड़ियों को खचरा बना देते हैं, या फिर वह ट्रैफ़िक जो शहर की साँस रोक देता है। लेकिन बारिश और मौसम के नखरे तो न्यूयॉर्क भी जानता है। वहाँ की चमक इतनी आसानी से नहीं छिलती। यहाँ तक कि जब ट्रंप व्हाइट हाउस में लौटकर वॉल स्ट्रीट को टैरिफ़ युद्ध और व्यापारिक धमकियों से हिलाते हैं, तब भी न्यूयॉर्क अपनी चमक नहीं खोता। उसका स्काइलाइन लगातार दमकता है, उसकी धुन अब भी कायम है। मुंबई, इसके उलट, कहीं ज़्यादा नाज़ुक लगा।ह—मानो पहली बारिश ही इसके ग्लैमर को बहा ले गई हो। दरअसल उसकी चमक को अनिश्चितताओं का बोझ धो डाल रहा है।
आज का भारत भी ऐसे ही एक बड़े बादल से ढका हुआ है—अनिश्चितता, जो अब इस देश का नया मौसम बन गई है।
यह बिना चेतावनी आता है, अंतहीन टिकता है, और बाकी हर मौसम को अपने रंग में ढाल देता है। मानसून, जो कभी राहत लाता था, अब ख़तरे की आहट है। उत्तराखंड से हिमाचल, कश्मीर तक—बादल फटने की खबरें बिना रुके आती हैं, नदियाँ राक्षसों की तरह उफनती हैं, कीचड़-पानी घरों और उम्मीदों दोनों को बहा ले जाता है। जिन देवताओं को हमने लंबे समय तक हल्के में लिया था, वे अब हिसाब वसूल रहे हैं। न्यूयॉर्क भी तूफ़ानों को जानता है—सबवे में पानी भरने वाले हरिकेन, सड़कों को जकड़ देने वाले बर्फ़ीले तूफ़ान—लेकिन उसका आत्मविश्वास टिकता है। वहाँ ढाँचा झुकता है, फिर उठता है, फिर से बनता है। भारत में, हर बारिश मानो ढहने जैसा महसूस होती है। फ़र्क़ सिर्फ़ भूगोल का नहीं, भरोसे का है।
आसमान की मार ही काफ़ी न थी कि वॉशिंगटन से लगी चोट भारत के लिए और गहरी है। डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ़ लगाना महज़ आर्थिक झटका नहीं था, यह वह गड़गड़ाहट थी जिसने एक दशक से बुने गए भ्रम को चकनाचूर कर दिया। “हाउडी मोदी” के रंगारंग आयोजन से लेकर साझेदारी की तमाम तस्वीरों तक, भारत को यक़ीन था कि वह अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पर ट्रंप की राजनीति की ठंडी गणित में साझेदारी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ उसका स्वार्थ शुरू होता है।
और असर सिर्फ़ सैद्धांतिक नहीं है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (FIEO) ने मंगलवार को कहा कि तिरुप्पुर, नोएडा और सूरत के वस्त्र-निर्माता उत्पादन रोक चुके हैं। “यह क्षेत्र वियतनाम और बांग्लादेश जैसे सस्ते प्रतिद्वंद्वियों के सामने पिछड़ रहा है। जहाँ तक समुद्री उत्पादों का सवाल है, ख़ासतौर पर झींगे, जिन्हें अमेरिकी बाज़ार लगभग 40% तक खाता है, उसके लिए टैरिफ़ वृद्धि का मारक मतलब है। स्टॉक के नुकसान, सप्लाई चेन का टूटना और किसानों की दुर्दशा,” FIEO अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने चेताया है। इस टैरिफ़ दीवार ने सूरत के हीरा तराशने वालों से लेकर आंध्र के झींगा किसानों, तिरुप्पुर के वस्त्र श्रमिकों और पुणे की मशीनरी इकाइयों तक, लाखों की रोज़ी-रोटी पर वार किया है। रुपये का मूल्य गिरा है, शेयर बाज़ार डगमगाए हैं, विकास दर के अनुमान घट चुके हैं। और एक ही झटके में भारत दुनिया के सबसे अधिक टैरिफ़ लगे देशों में गिना जाने लगा है।
जबकि वॉल स्ट्रीट अभी भी बमबम है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अब भी वैश्विक धड़कन तय कर रहा है। उसकी अस्थिरता में भी एक दृढ़ता झलकती है। जबकि मुंबई का बाज़ार, इसके विपरीत, हर टैरिफ़ हेडलाइन पर काँप जाता है। एक शहर निश्चितता पर चलता है, दूसरा उम्मीद पर।
और फिर भी, इस दरार, संकट के बीच प्रधानमंत्री अपनी लय में चलते हैं। मेट्रो और हाइवे के रिबन काटना। नारे दोहराना मानो कोई मंत्र हों: मेक इन इंडिया। मेक फ़ॉर द वर्ल्ड। दिवाली से पहले बड़े टैक्स तोहफ़ों का वादा—एक सरल जीएसटी प्रणाली, “उपभोग को मुक्त करने” के लिए। पर यह सब एक और जुमला ही लगता है—मानो नारे दोहराने से हक़ीक़त बदल जाएगी।
लेकिन शब्दों का खेल जो हो रहा है, वह सच नहीं ढक सकता। टैक्स में छूट या जीएसटी में छोटे सुधार उपभोग को थोड़ा सहला सकते हैं, पर 50% टैरिफ़ दीवार के झटके को नहीं रोक सकते। वे उन दरवाज़ों को नहीं खोल सकते जो अमेरिका ने बंद कर दिए हैं। वे उन निर्यातकों को नहीं बचा सकते जिनकी फैक्टरियाँ आज बंद हो रही हैं। मोदी के वादे की “निश्चितता” और भारत की जीती-जागती “अनिश्चितता” के बीच की खाई अब और गहरी हो गई है।
मध्यवर्ग के लिए यह अनिश्चितता और भी निजी रूप लिए होती है। मुंबई में मैंने शायद ही किसी से मुलाक़ात की हो जो जीवन से संतुष्ट दिखे—बिल असहनीय हैं, किराए अकल्पनीय और खर्चे लगातार सिर चढ़ते हुए। दिल्ली से भी ज़्यादा बोझिल और बेमुरव्वत लगता है यहाँ का जीवन। दिल्ली में घर खरीदना मिलेनियल के लिए सपना है, तो मुंबई में यह नामुमकिन-सा है। जगह की ऐसी किल्लत कि अमीर से ग़रीब तक सभी एक-दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं—छतें और दीवारें तकरीबन धकेल रही हों, निजता उतनी ही दुर्लभ है जितनी जगह। छोटी-सी ख़ुशी भी अब फिज़ूलखर्ची लगती है। टैक्सी की सवारी जेब चीर सकती है। कैफ़े लियोपोल्ड में पास्ता की एक प्लेट अब ₹800 से ऊपर है—यह महज़ खाना नहीं, बल्कि एक बयान लगता है। वही कैफ़े, जो अब सिर्फ़ कैफ़े नहीं रहा, बल्कि 26/11 की यादों और शांताराम की पंक्तियों से एक स्मारक बन गया है। मुंबई के इस एक कोने में ग्लैमर और ग़म, चाहत और थकान, सब भीड़ की तरह साथ रहते हैं।
यही धीरे-धीरे भारत की कहानी बन रही है। महँगाई घरों को खा रही है, रोज़गार अटक-अटककर चल रहा है। कभी एक परिवार हर 3–4 साल में कार बदल सकता था, अब एक दशक लग जाता है। कभी “विंडो शॉपिंग” शौक था, अब मजबूरी है। हर तीसरा युवा “फ़्रीलांसर” है—चुनाव से नहीं, बल्कि इसलिए कि पक्की नौकरियाँ ही ग़ायब हो गई हैं। सरकार तक अब न लोगों को स्थायी रूप से रखती है, न गाड़ियों को—सब भाड़े पर। विकल्प भी घटे हैं। कभी मुंबई की उड़ान के लिए जेट एयरवेज़, किंगफ़िशर, एयर इंडिया, इंडिगो में से चुन सकते थे, अब दो विकल्प बचे हैं। कभी टेलीकॉम में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल सभी थे—अब फ़ोन अपने आप जियो से जुड़ता है क्योंकि बाक़ी नेटवर्क बस नाममात्र हैं। ग्यारह साल के नारों की गूँज रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी-छोटी झुँझलाहटों से टकराती है। ग़रीब के लिए चोट और गहरी है—कम शिफ़्टें, कम निर्यात, कम रक़म।
और सबसे ज़्यादा जो कुतरता है, वह है भरोसा। मोदी की राजनीति “अपरिहार्यता” के भाव पर खड़ी रही है—भारत की नियति एक विश्वगुरु के रूप में, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के रूप में। लेकिन ट्रंप के टैरिफ़ ने इस आभा को फाड़ दिया। अगर अमेरिका अपने “सबसे मज़बूत साझेदार” के साथ ऐसा कर सकता है, तो कौन-सी निश्चितता बची है?
राष्ट्र की अपनी निश्चितता भी बिखरती दिखती है। संसद अब लगभग रंगमंच है, अदालतें दबाव में डगमगाती हुई और मीडिया सवाल से ज़्यादा प्रतिध्वनि है। जो संस्थाएँ बाज़ारों को संभालनी चाहिए थीं, वे अविश्वास पैदा करती हैं। लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की जो मचान दशकों से खड़ी थी, वह अब पतली और भुरभुरी हो गई है।
अनिश्चितता अब इतनी व्याप्त (pervasive) हो चुकी है कि स्थिरता भी छलावा लगती है। पिछली बार भारत ऐसी धुंध में कोविड के समय दाख़िल हुआ था, जब पूरी दुनिया उसी तूफ़ान में थी। तब कम से कम हम अकेले नहीं थे। आज की अनिश्चितता ज़्यादा अकेली है, ज़्यादा खोखली। क्योंकि तब और अब के बीच का असली फ़र्क़ भरोसा है—और भरोसा ढह रहा है। संस्थाएँ अब आश्वस्त नहीं करतीं, नेता प्रेरित नहीं करते, सच अब भरोसा नहीं जगाता। भरोसे के बिना, निश्चितता भी अनिश्चित हो जाती है।
भारत से कहा जा रहा है कि अपनी नियति का उत्सव मनाए, खुद को अजेय समझे। मुंबई से कहा जा रहा है कि वह अगला न्यूयॉर्क बनेगा। दिल्ली अब भी सत्ता का मंच है—चौड़ी सड़कें, राजनीतिक आडंबर, लाल क़िले से गूँजते वादे। पर सच्चाई यह है कि कोई भी अपने किरदार पर खरा नहीं उतर रहा।
न्यूयॉर्क का आत्मविश्वास काँच की इमारतों या तटीय सड़कों से नहीं आता, बल्कि भरोसे से आता है—प्रणालियों में, संस्थाओं में, कल में। दिल्ली की भव्यता नारों से नहीं, बल्कि उस निश्चितता से आती है कि सत्ता वहीं टिकेगी। मुंबई में सपने हैं, पर साथ में चिपचिपी बारिशें, टूटती सड़कों, असंभव किराए और लियोपोल्ड का पास्ता—जिसका स्वाद ग्लैमर और ग़म दोनों का है।
आख़िरकार, दिल्ली, मुंबई और न्यूयॉर्क—तीनों शहर एक ही विरोधाभास खोलते हैं: भारत क्या बनना चाहता है, भारत क्या होने का दिखावा करता है, और भारत वास्तव में क्या है। यह देश सस्पेंस में जी रहा है—जिसकी चमक हर अगली बारिश, हर अगले टैरिफ़, हर अगले संकट से धुल जाने को तैयार रहती है।
अनिश्चितता, जो कभी छाया भर थी, अब इस देश का स्थायी मौसम बन चुकी है।