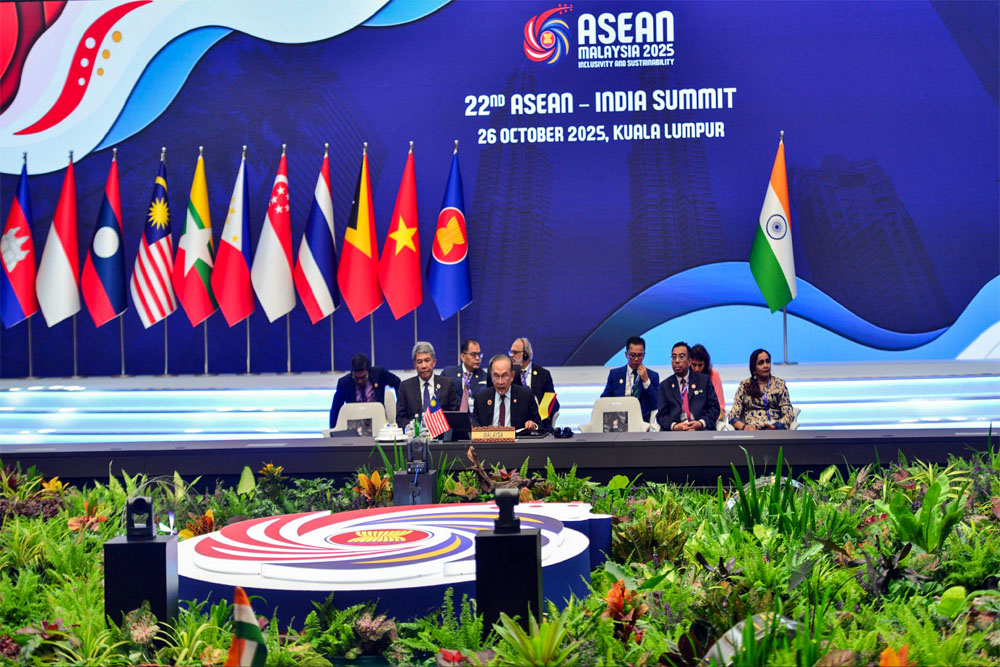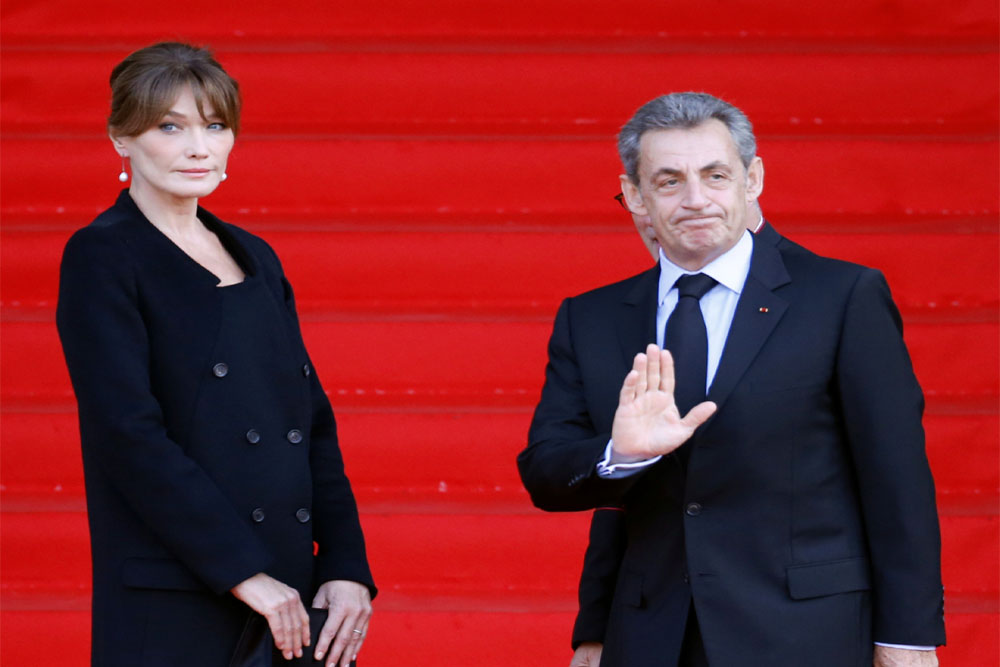डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे तीस साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करेंगे। उधर पाकिस्तान ने धमकी दी है कि तालिबान को फिर से गुफ़ाओं में धकेलने के लिए वह अपने जखीरे का “एक अंश” खोल देगा। ग़ाज़ा में एक और रात रॉकेटों के आसमान तले गुज़री। इज़राइल की ताज़ा हवाई बमबारी में सौ से अधिक लोग मारे गए, जबकि युद्धविराम फिर लड़खड़ा रहा है। हरिकेन मेलिसा ने कैरेबियन को सपाट कर दिया। और अपने घर में, राजधानी दिल्ली की हवा घुटन भरे धूसर रंग में बदलती जा रही है। बिहार का चुनावी तापमान धुंध के साथ तालमेल में अलग ऊपर चढ़ रहा है।
और ये सब सिर्फ़ बीते कल की ख़बरे है।
एक पत्रकार के तौर पर यह सब थकाने वाला है।
इन दिनों एक अजीब-सी घबराहट आ बैठती है, हर सुबह लैपटॉप खोलते ही। और क्या लिखूँ जो पहले किसी शोक-स्वर में न कहा जा चुका हो? ऐसी कौन-सी नई बात लिखूँ जो लोकतंत्र, मर्यादा और उम्मीद के एक और शोकपत्र जैसी न लगे? मैं साइट्स, वायर कॉपियाँ खंगालती हूँ—ऐसी कहानी की तलाश में जो अर्थपूर्ण हो पर निराशाजनक नहीं, तात्कालिक हो पर उन्मत्त नहीं। कुछ जो किसी अंत की गंध न दे।
पर अर्थ ही दुर्लभ हो गया है। ख़बर अब खिड़की से ज़्यादा आईने जैसी लगती है—दोहराव की मार से दरकता हुआ आईना। यह थकान सिर्फ़ निजी नहीं, संरचनात्मक है। दस साल पुरानी बासी कहानियाँ मैगज़ीन दफ़्तरों में फिर से गर्म की जा रही हैं और “नए दौर” की ताज़ा राय बनकर परोसी जा रही हैं। टीवी स्टूडियो और अख़बारों के ब्रांड अपने-अपने पैनल, अवॉर्ड और फ़ोरम रचकर ख़ुद ही “ख़बर” बनाने लगे हैं—जहाँ पत्रकारिता और मार्केटिंग की रेखा धुँधली पड़ जाती है।
गलती सिर्फ़ सत्ता या उद्योग की नहीं बल्कि पत्रकार भी दोषी हैं। कुछ समय पहले एक पत्रकार मिले जो पूरी ईमानदारी से सरकार की उस नीति का बचाव कर रहे थे जिसमें पत्रकारों का नेताओं के साथ यात्रा करना ख़त्म कर दिया गया है। उनका तर्क था—अगर राज्य के ख़र्च पर कोई पत्रकार आधिकारिक दौरे पर जाए और बाद में आलोचनात्मक लिख दे तो नेता को “धोखा” महसूस होना स्वाभाविक है। तर्क सादा था—और सिहराने वाला। मतलब सरकार पैसा दे तो पत्रकार “ठीक बर्ताव” करे। कौन-सा तर्क दिया जाए इसके आगे? यह भूलते हुए कि वह पैसा जनता का है—आपका, मेरा, सबका। और यह भी कि पत्रकार का काम वही पूछना है जिसे सत्ता छिपाना चाहती है; सत्ता की जय-जयकार दोहराना नहीं।
कभी रिपोर्टिंग का मतलब था साक्षी होना। शोर आने से पहले सच को शांत, सधे ढंग से दर्ज करना। अब शोर पहले आता है, कहानी पीछे-पीछे हाँफती है—अगर पहुँच पाए तो। हम अब यह नहीं पूछते कि क्या महत्त्वपूर्ण है; पूछते हैं, क्या क्लिक होगा? यह गिरावट सिर्फ़ संस्थानों से नहीं, लेखन तक उतर आया है। विचार लेख—जो कभी विचार जगाने के लिए होते थे—अब प्रदर्शन बनते जा रहे हैं; प्रासंगिक लगने की दौड़, चिंतन की जगह लेती जा रही है। संपादकीय पन्ना—जो कभी अख़बार का विवेक-स्तंभ था—अब किसी और कंटेंट फ़ीड की तरह स्क्रोल होता है। हम मनाने के लिए नहीं बहस करते बल्कि ट्रेंड करने के लिए करते हैं। जबकि कभी पत्रकारिता आईना थी।
आज की पत्रकारिता अहसान और भय के भार तले धीमे-धीमे झुकती है। चुप्पी को “बैलेंस” कहा जाता है; सच बोलना “ऐक्टिविज़्म” ठहराया जाता है। बीट्स, इको-चैम्बर्स बन गई हैं; प्रेस कॉन्फ़्रेंस—प्रदर्शन। सवाल करने की वृत्ति, समूह में शामिल होने की प्रवृत्ति से बदल दी गई है। क्योंकि आज के माहौल में जो ख़बर सचमुच ख़बर है—बिना फिल्टर, असुविधाजनक, अनस्क्रिप्टेड—अक्सर छुई ही नहीं जाती। नस तक पहुँचना जोखिम है; शोर को कवर करना सुरक्षित। जब सत्ता ही सुर्ख़ियाँ फंड करे तो “निष्पक्षता” भी प्रतिरोध बन जाती है और सच तो ऐसी देयता, जिस पर टैक्स भी लग सकता है।
यही वजह है कि पत्रकार अब जीने के लिए लिखते हैं, सूचित करने के लिए नहीं।
मुझे लगा था कोविड सबसे बुरा वक़्त था। जब मौत ही एकमात्र ख़बर थी। घड़ी जैसे अंत से ठीक पहले रुक गई थी। पर उसके बाद जो आया, वह और अजीब था—सुर्ख़ियों में खुलती स्लो-मोशन प्रलय। बाढ़ें, युद्ध, अकाल, तख़्तापलट—संकट की भाषा और धाराप्रवाह, और स्थायी हो गई। महामारी ने समय को स्थिर किया; उसके बाद का दौर हमें रिप्ले में कैद कर गया—वही शोक, नए चेहरे। और जब दुनिया इस अंतहीन रील में घूम रही है, मैं ख़ुद को लिखते हुए पाती हूँ। उस अर्थ की खोज में जो एक अर्थहीन करने पर आमादा समय से बचा सके। राजनीति रंगमंच लगती है, सत्ता—प्रदर्शन। नेता पॉपुलिस्ट बनते हैं, पॉपुलिस्ट पैग़ंबर; हर प्रेस कॉन्फ़्रेंस परफ़ॉर्मेंस आर्ट। कई दिन तो समझ नहीं आता कि मैं इतिहास कवर कर रही हूँ या पैरोडी।
एक उपभोक्ता के रूप में ख़बर मुझे तोड़ देती है। पत्रकार के रूप में मैं और भी थक जाती हूँ। फिर उस थकान को रोज़ शब्दों में अनुवाद करने को विवश।
उलझन में, एक शाम कॉफ़ी पर मैंने एक दोस्त से कहा—“सोचती हूँ, कुछ हल्की-फुल्की, नर्म-सी किताबें पढ़ना शुरू करूँ—जेन आयर, लिटिल वीमेन, यहाँ तक कि चिकन सूप फ़ॉर द सोल। शायद कुछ जापानी कहानियाँ—ख़ामोश कैफ़े और मामूली दयालुताओं पर।” वह मुझे अजीब नज़र से देखने लगी। पर मैं मज़ाक नहीं कर रही थी। ज़रूरत है—हल्केपन की, कोमलता की; ऐसी कहानियों की जिनमें न पॉलिसी ब्रीफ हो, न हताहतों की गिनती। क्योंकि युद्धों, पागलों, विदूषकों, जलवायु पतन, और तीस की उम्र में शुगर–दिल की घबराहट के बीच मैंने शायद साधारण आनंद का चेहरा ही भूल दिया है।
और मैं अकेली नहीं। बहुत-से लोग चुपचाप ख़बरों से ट्यून आउट हो रहे हैं—उदासीनता से नहीं, थकान से—खून बहाती सुर्ख़ियों, चीख़ते डिबेट, और अंतिम-सी लगती सच्चाइयों से थककर। वे सांस लेना चाहते हैं—बुलेटिनों के बीच नहीं, बस सांस लेना चाहते हैं।
मेरे लिए, चाहे मैं जेन आयर फिर से पढ़ना शुरू कर दूँ, दिनचर्या तो बनी रहेगी ही। लैपटॉप खोलना, वायर पढ़ना, शोर छानना—इस उम्मीद में कि कोई ऐसी कहानी मिल जाए जिसमें धुएँ और मलबे की नहीं, रोशनी और झिलमिल की गंध हो। या शायद वे नर्म, हास्य-भरी किताबें मुझे उन विदूषक–पॉपुलिस्ट–पैग़ंबरों को थोड़ी और हँसी से देखने की क्षमता दे दें—मेरे लिखने में हल्कापन, आपके पढ़ने में राहत। और शायद पत्रकारिता अब इसी ओर जा रही है—ब्रेकिंग की दीवानगी नहीं, छोटी कृपाओं की तलाश: कोई टुकड़ा, कोई चमक, कोई याद दिलाहट कि अभी कुछ बचा है।
क्योंकि अगर दुनिया पैरोडी बनने पर आमादा है, तो शायद आख़िर में ईमानदारी यही है—हल्की, समझदार हँसी के साथ लिखते रहना।