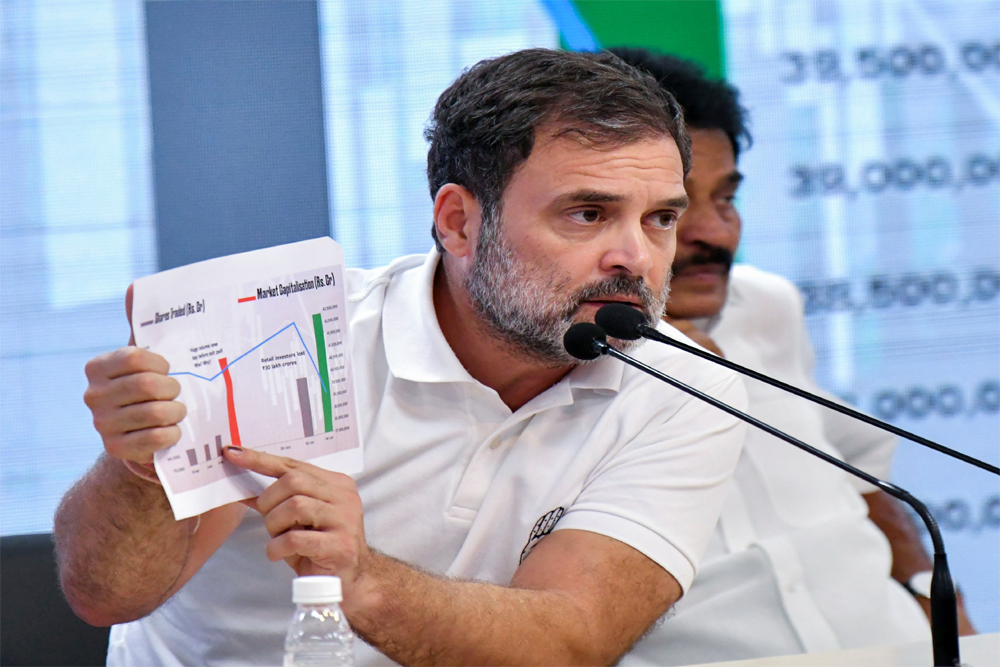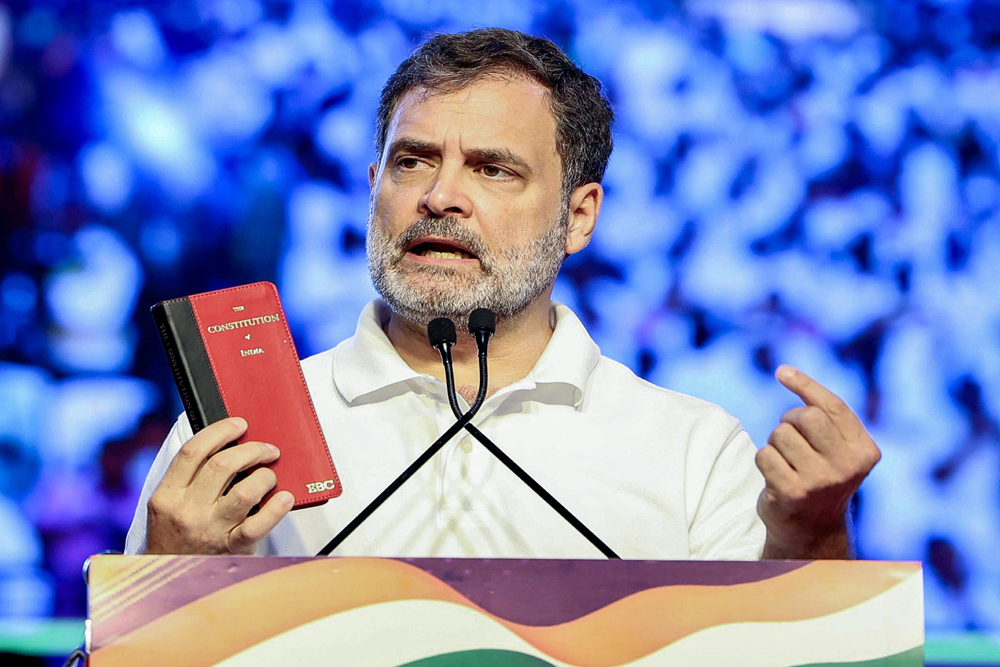क्या जलवायु चिंता से शुरू कोप (COP) सम्मेलन कुछ मायने रखता हैं? या सिर्फ बस एक नौटंकी है?
यह प्रश्न अब स्थाई है पर बेचैन करने वाला, आवश्यक भी, मगर अनुत्तरित। क्या COP सम्मेलन से तनिक भी कुछ बदलता हैं? फिलहाल ब्राज़ील के बेले (Belém) में COP30 की तैयारी हो रही है। सो “पार्टियों का सम्मेलन”, एक और संस्करण, वायदों का एक और जमावड़ा और शोक में डूबी धरती के बीच नए फोटो-ऑप्स। कभी COP एक उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था, एक आदर्श प्रयोग के रूप में। यह वह दुर्लभ मंच था जहाँ अमीर और ग़रीब, लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी, सभी देशों के नेता एक साथ बैठते थे और पृथ्वी के भविष्य पर विचार होता था क्योंकि पर्यावरण, वातावरण की कोई सीमा नहीं है। न ही समुद्रों के बढ़ते तापमान की कोई विचारधारा। जलवायु परिवर्तन वह संकट था जिसने मनुष्य को साफ बता रखा है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठो, क्योंकि पूरी पृथ्वी के अस्तित्व का प्रश्न है।
पर जैसे-जैसे धरती और गर्म, तथा ठंडी, और भीगी व सूखी होती गई, जैसे-जैसे बाढ़ें गहरी और जंगल राख में बदलते गए, COP की भाव-भंगिमा भी बदली। अब वह रूपांतरण, कार्य योजनाओं का नहीं बल्कि दिखावे व प्रदर्शन का मंच बन गया है। महत्त्वाकांक्षाओं, लफ्फाजी से भरा सम्मेलन जबकि क्रियान्वयन से खाली।
मतलब वादों, वचनबद्धताओं का रंगमंच, जहाँ ताली ज्यादा बजती है, जवाबदेही कम। और फिर भी, हम हर साल सम्मेलन के लिए जुट आते हैं।
इस नवंबर, 6 से 21 तारीख तक, दुनिया बेलें में अमेज़न के मुहाने पर जुटेगी । शायद कोई और शहर जलवायु कूटनीति के विरोधाभासों को इतनी स्पष्टता से नहीं दिखाता। यह सम्मेलन जो दुनिया के सबसे नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्र के बीच हो रहा है, पर उसी तंत्र को काटकर बनाए गए ढांचे पर। राज्य सरकार ने नेताओं के स्वागत के लिए एक नई चार लेन की सड़क बनाई है, जिसके लिए हज़ारों एकड़ संरक्षित वर्षावन साफ़ कर दिए गए। सरकार इसे “सस्टेनेबल” कहती है। संरक्षणवादी इसे सही नाम देते हैं संरक्षण के नाम पर विनाश। इस बीच, बढ़ती होटल दरों ने ग्लोबल साउथ के कई प्रतिनिधिमंडलों के लिए रहना लगभग असंभव बना दिया है। बेलें के कई मज़दूर इलाकों को खाली कराया जा रहा है ताकि राजनयिकों और लॉबिस्टों के काफ़िले को जगह मिले।
सम्मेलन शुरू होने से पहले ही इसकी दरारें दिखने लगी हैं, कौन बोल सकता है, और किसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। और इन हरे बैनरों के पीछे छिपा है एक गहरा, खतरनाक इंकार, विज्ञान का नहीं, आर्थिक परिणामों का। अब “यह सच नहीं” का इनकार नहीं रहा, बल्कि “यह पूँजी को नहीं छेड़ सकता” वाला इनकार है।
इस साल का COP “ग्लोबल साउथ COP” कहा जा रहा है, पहला सम्मेलन जो अमेज़न में हो रहा है, जिसे “धरती के फेफड़े” कहा जाता है। प्रतीकात्मक रूप से यह समावेश का वादा करता है, पर समावेश समानता नहीं है। क्योंकि जब ग्लोबल साउथ पहुंचेगा, कर्ज़, सूखा और जलवायु असमानता के बोझ के साथ, तो ग्लोबल नॉर्थ आएगा आंकड़ों और पॉवरपॉइंट्स के साथ। उनकी भाषा होगी प्रतिशतों में, लोगों में नहीं। उनके सूत्र होंगे “नेट ज़ीरो बाय 2050”, जबकि दक्षिण के लिए सवाल है “2025 तक कौन ज़िंदा रहेगा? वे बोलेंगे “ऑफ़सेट मार्केट्स” और “क्लाइमेट फ़ाइनेंस” की भाषा में, ऐसे सौदों में जो उत्तर को सुकून खरीदने देते हैं जबकि दक्षिण अपने जंगल, अपने तट, अपनी साँसें खोता है। उनकी एक्सेल शीट्स चमकेंगी, पर वे इतिहास नहीं दिखाएंगी, सदियों की लूट, उपनिवेशवाद, औद्योगिक लालच का इतिहास। उत्तर गणना करता है “गीगाटन” में, दक्षिण गणना करता है “बर्बाद फ़सलों, डूबे खेतों और प्रवासी मज़दूरों” में।
COP30 में फिर “फ़ंडिंग फ़ॉर्मूले”, पर मुआवज़े की बात नहीं होगी। वह कहेगा “अनुकूलन ज़रूरी है”, पर यह नहीं बताएगा, कौन किसके अनुकूल हो? और विडंबना यह कि दक्षिण के कई छोटे देश, जो सबसे अधिक जलवायु त्रासदियों से जूझ रहे हैं, शायद इस बार सम्मेलन तक पहुँच भी न पाएं, क्योंकि बेलें के होटल अब उनके लिए भी महंगे हो चुके हैं। तो सवाल उठता है, अगर पहुँच ही विशेषाधिकार है, तो फिर आवाज़ कहाँ से आएगी?
और फिर भी, इसी असंतुलन में अवसर छिपा है। भारत चाहे तो सिर्फ़ भाग नहीं ले, नेतृत्व करे। आख़िरकार, यह वही भारत है जिसने खुद को “विश्वगुरु” कहा है, दुनिया का नैतिक पथप्रदर्शक। पिछले साल G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को “ग्लोबल साउथ की आवाज़” के रूप में पेश किया था। पर अगर यह नेतृत्व सिर्फ़ भाषण नहीं, बल्कि दृष्टि बनना है, तो हमें वह कहना होगा जो बाकी नहीं कह रहे, कि क्लाइमेट एड अक्सर छलावा है। “ग्रीन फ़ाइनेंस” एक नए कार्बन उपनिवेशवाद में बदल रहा है, सततता की भाषा में लिपटा, पर असमानता की मुद्रा में व्यापार करता हुआ। नेतृत्व का अर्थ सिर्फ़ मंच पर नारे नहीं, बल्कि उन व्यवस्थाओं को चुनौती देना है जो प्रदूषण से मुनाफ़ा कमाती हैं जबकि ग़रीब डूबते, जलते और दम तोड़ते हैं।
अगर भारत “विश्वगुरु” बनना चाहता है, तो शुरुआत अपने घर से करनी होगी। काग़ज़ी जंगल नहीं, असली हरियाली से। बायोफ्यूल के वादे नहीं, बसें चलाने से। नेट-ज़ीरो के नारे नहीं, उत्सर्जन नियंत्रण से। घोषणाओं की परिषदें नहीं, रीढ़वाले शासन से। नेतृत्व का पहला कर्तव्य है, अपने ही गलियारों का धुआँ साफ़ करना। कोयला लॉबी से, “ग्रीनवॉशिंग” की फ़ाइलों से, और उस शांत इंकार से जो “विकास” का नाम लेकर चल रहा है।
सचमुच दुनिया को अब प्रदर्शन नहीं, साँस लेने लायक राजनीति चाहिए।
जलवायु संकट अब गिनती बन चुका है, शरीरों की गिनती। WHO और Lancet Countdown की ताज़ा रिपोर्ट बताती है: बढ़ता वैश्विक तापमान अब हर मिनट में एक जान ले रहा है। शब्दशः। पिछले वर्ष 5.46 लाख ताप-संबंधी मौतें दर्ज की गईं — 1990 के दशक से 23% की वृद्धि। जंगलों की आग से लेकर डेंगू के फैलाव तक, निर्माण स्थलों पर हीटस्ट्रोक से लेकर सूखे खेतों तक, यह अब धीमी त्रासदी नहीं, तेज़ी से बढ़ता प्रलय है। फिर भी, सरकारें अब भी जीवाश्म ईंधन पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करती हैं। सिर्फ़ 2023 में यह सब्सिडी 956 अरब डॉलर तक पहुँची, जबकि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश
अब भी उस सहायता का इंतज़ार कर रहे हैं जो या तो देर से आती है या शर्तों में बंधी होती है, किसी और की मुद्रा में, किसी और की मंशा से। अगर हर मिनट मरती एक ज़िंदगी भी कार्यवाही नहीं जगाती, तो फिर क्या करेगा?
शायद एक और COP नहीं। शायद एक और प्रेस रिलीज़ नहीं। शायद एक और मंच नहीं जो “क्लाइमेट सिंबलिज़्म” में लिपटा हो।
और फिर भी, दुनिया लौटती है। क्योंकि विरोधाभासों के बावजूद, COP ही वे आख़िरी मंच हैं जहाँ हर देश — अमीर या ग़रीब — अभी भी जीवित रहने की बहस में बैठता है। जहाँ ग्लोबल साउथ के पास अभी भी एक माइक है, कमज़ोर, क्षणिक, पर मौजूद। क्योंकि अभिनय भी कभी-कभी दबाव बनाता है। और मंच भी कभी-कभी इतिहास की दिशा बदल देता है।
तो क्या COP मायने रखते हैं? हाँ, अगर हम उन्हें मायने देने की हिम्मत करें। क्योंकि यह अब भी वह मंच है जहाँ इतिहास पूरा नहीं हुआ। जहाँ शक्तिशाली देशों को, भले क्षणभर के लिए, अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जलवायु संकट अब भविष्य का नहीं,
वर्तमान का प्रश्न है, कौन बचेगा, कौन नहीं। और यही आज की बातचीत का असली केंद्र है। COP तभी मायने रखेंगे, जब उनके बाद कोई, कहीं, वास्तव में, हल्की साँस ले सके। न सिद्धांत में, बल्कि सच्चाई में। जब वे वार्षिक बहाने नहीं, नैतिक निर्णय बन जाएँ।