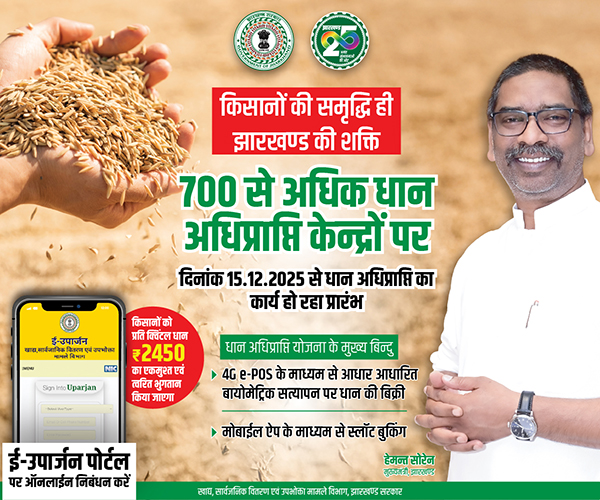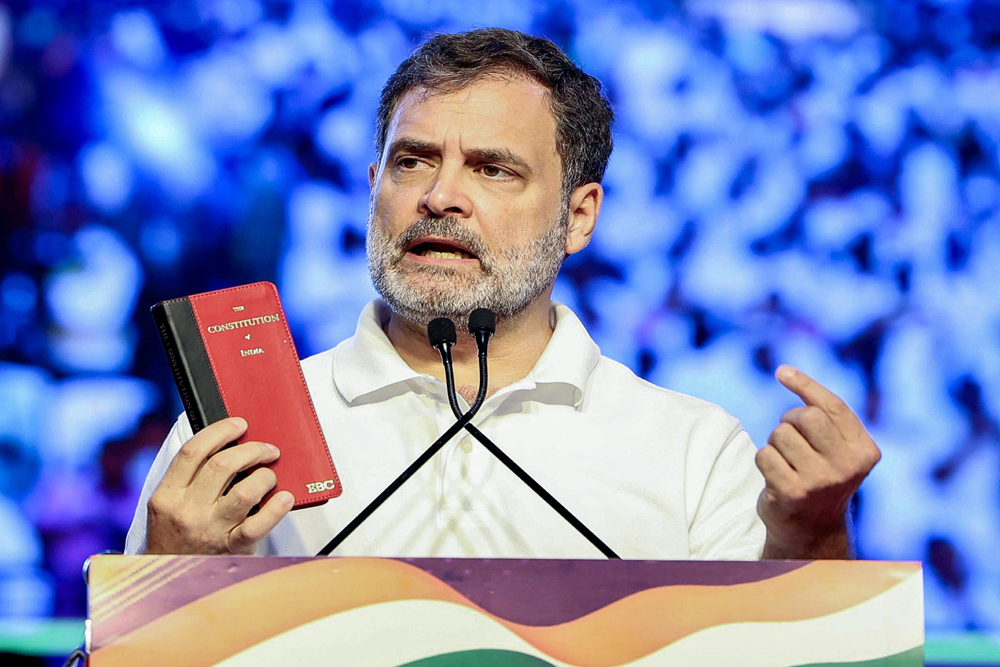और इसलिए नहीं क्योंकि हम एक संतुष्ट, आत्मसंतोषी देश बन चुके हैं बल्कि इसलिए कि हम विरोध करना ही भूल गए हैं।पिछले एक हफ़्ते से ज़्यादा समय से दिल्ली अपनी ही हवा में घुट रही है। कुछ चिंतित नागरिकों ने इसलिए इंडिया गेट पर एकत्र होकर विरोध दर्ज करने का निर्णय लिया। यह प्रदर्शन तमाशा नहीं था, एक वक्तव्य था सोच-समझकर किया गया, शांति में दृढ़, और अपने संदेश में तात्कालिक। न कोई नारे, न सड़कें जाम। बस चुपचाप उठे हुए पोस्टर, जिन पर सवाल स्याही से लिखे थे: “हम सांस क्यों नहीं ले पा रहे?”, “ज़िम्मेदार कौन है?”, “नीति कहाँ है?”
पर वह भी इस लोकतंत्र को ज़्यादा लगा। तीस मिनट में ही पुलिस पहुँच गई। गिरफ़्तारियाँ शुरू हुईं। हवा, जो पहले ही धूल और ज़हरीले कणों से भारी थी, अब एक और बोझ ढो रही थी, उस लोकतंत्र का जो सवालों को ख़तरा मानता है। और फिर भी, सबसे चुभने वाली बात यह नहीं थी कि पुलिस ने कार्रवाई की, बल्कि यह कि किसी को परवाह नहीं थी। कोई आगे नहीं आया। बस X और इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने वीडियो शेयर किए, सही हैशटैग लगाए, और आगे बढ़ गए। विरोध भी अब ‘फ़ीड’ की तरह है, कुछ घंटों की गूंज, फिर सोमवार सुबह तक सब भुला दिया गया।
और तब लगा क्या यह वही देश है जिसकी गलियाँ कभी प्रतिरोध की नब्ज़ से भरी रहती थी? आपातकाल के विरोध तक की हिम्मत से लेकर मंडल आंदोलन तक, निर्भया से अन्ना हज़ारे तक, विरोध कभी भारत की एक जीवंतता थी, एक नैतिक परीक्षण। सड़कें बोलती थीं और सत्ता सुनने को मजबूर होती थी। वह विरोध प्रतीकात्मक नहीं था, रूपांतरणकारी था। उसने व्यवस्था को हिलाया ही नहीं, बदला भी। संसद जब पीठ फेर लेती थी, तब सड़क ही जनता की संसद बन जाती थी। संविधान तब सिर्फ़ किताब में नहीं, आत्मा में जिया जाता था।
आज विरोध केवल अभिनय है, बिना विश्वास का, बिना परिणाम का। नारे हैं पर नज़र नहीं। ग़ुस्सा है पर गहराई नहीं। यह आंदोलन नहीं, एल्गोरिद्म के शोर हैं जो ट्रेंड में आते हैं और मुरझा जाते हैं। क्योंकि बदला केवल राज्य का नियंत्रण नहीं, हमारी सोच की सुस्ती भी है। आज की असहमति एक परिधान है, आत्मा के बिना। यह सिर्फ़ राजनीतिक संकट नहीं, एक बौद्धिक पतन है विचार की भूमि में सड़न। हम अक्सर “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” की बात करते हैं, पर भूल जाते हैं कि अभिव्यक्ति सोच की उपज है। असली शुरुआत विचार की स्वतंत्रता से होती है।
150 साल पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस सच्चाई को कहीं ज़्यादा गहराई से समझा था। स्वतंत्रता के अपने तर्क में उन्होंने भाषण से नहीं, विचार और विमर्श की आज़ादी से शुरुआत की। उनके लिए ‘फ्री स्पीच’ मंज़िल नहीं, साधन था, सत्य की सामूहिक खोज का। सोचने की आज़ादी के बिना बोलने की आज़ादी एक नाटक है। क्योंकि सोचना कठिन है। वह आत्म-संशय माँगता है, तैयारी माँगता है, आलोचना झेलने का साहस माँगता है। तब मिल ने चेताया था, यदि हम पूर्वाग्रह, डर, या सत्ता की निष्ठा में बंधे हैं, तो हमारी आवाज़ स्वतंत्र नहीं, प्रोग्राम्ड है। और आज हम वहीं खड़े हैं।
भारत में विरोध अब तर्क का नहीं, ताप का अभिनय है। हम विचार से पहले प्रतिक्रिया देते हैं, पढ़ने से पहले पोस्ट करते हैं, समझे बिना ग़ुस्सा दिखाते हैं। हमारी सोच अब हमारी नहीं रही, वह क्यूरेटेड है, फ़ीड की तरह चुनी हुई, कुछ सुविधाजनक, कुछ भयकारी। लोगों को लगातार बताया गया कि हिंदू ख़तरे में हैं, और यह डर दोहराते-दोहराते वास्तविकता का रूप लेने लगा। सांख्यिकीय, जनसांख्यिकीय, राजनीतिक किसी भी दृष्टि से हिंदू कभी ख़तरे में नहीं थे, पर यह धारणा अब ‘सत्य’ बन गई है। और अब सत्ता पर सवाल उठाना ‘अहिंदू’, ‘राष्ट्रविरोधी’, ‘विदेशी एजेंडा’ कह दिया जाता है। यह हमारे समय का नैतिक उलटफेर है जहाँ सरकार के प्रति वफ़ादारी ही देशभक्ति है, और असहमति देशद्रोह। और इसीलिए हम असहमति को स्क्रॉल कर आगे बढ़ जाते हैं। छात्रों को राष्ट्रविरोधी कहते हैं। संविधान लिए महिलाओं को अराजक बताकर नकार देते हैं।
किसानों को अपमानित करते हैं। हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें याद रखना सिखाया ही नहीं गया। इसलिए हमारे विरोध टिकते नहीं।
क्योंकि वे विचार से नहीं, थकान से बने हैं। और विरोध केवल सड़कों पर आने का नाम नहीं यह जानने का नाम है कि आप क्यों खड़े हैं।
पोस्टर से ज़्यादा ज़रूरी है आपका यक़ीन।
इसीलिए जब नेपाल की जेन ज़ी सड़कों पर उतरी, तो भारत के बुद्धिजीवियों में उम्मीद की लहर सी उठी। कहा गया, “शायद भारत का युवावर्ग भी उठ खड़ा होगा।” यह उत्साह कुछ देर टिका। राहुल गांधी ने भी यही कहा, कि भारत का जेन ज़ी अब अन्याय और निगरानी के ख़िलाफ़ बोलेगा।
जब ज़ोहरन ममदानी जीते, तो उनका भाषण भारत में एक प्रतीक-सा बन गया, कविता और नीति का संगम। मानो हमने पल भर को विश्वास कर लिया हो कि हम भी ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं।
पर भीतर सब जानते हैं भारत का नेपाल क्षण नहीं आने वाला। हमारा ज़ोहरन ममदानी नहीं पैदा होगा। क्योंकि हमने वह सोच विकसित ही नहीं की जो विरोध को जन्म देती है। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ तभी है जब विचार स्वतंत्र हों। हमने न अपने स्कूलों में, न अपने घरों में, न अपने राजनीतिक विमर्श में वह बौद्धिक साहस सिखाया है। हमने याद करना सीखा, प्रश्न पूछना नहीं। हमने प्रदर्शन सीखा, ठहराव नहीं।
हम व्यक्त करना जानते हैं, समझना नहीं। हम नैतिक, मानसिक, और राजनीतिक रूप से तैयार नहीं हैं, तब खड़े होने के लिए जब सब झुक रहे हों।
जॉन स्टुअर्ट मिल ने चेताया था, जो बिना परखे मानते हैं, वे सबसे बड़े ख़तरे हैं। और जब यही सामान्य हो जाए, तब विरोध खोखला हो जाता है, नागरिकता औपचारिक, और लोकतंत्र संचालित।
भारत ने विरोध इसलिए नहीं छोड़ा कि वह खुश है। उसने छोड़ा है क्योंकि वह असहमति की भाषा ही भूल गया है। हमने मौलिक सोच की आदत खो दी है। हमने न सिर्फ़ अपने तथ्य, बल्कि अपनी संवेदना और अपने मानदंड भी आउटसोर्स कर दिए हैं। आज लोकतंत्र केवल राज्य के दमन से नहीं, नागरिक की समर्पणवृत्ति से भी घिरा है। हमने साहस के बदले सुविधा चुनी है। चुप्पी के बदले जटिलता से भागना चुना है। और इसीलिए सत्ता को रस्सी कसने के सारे कारण मिल गए हैं। कल फिर शायद कुछ लोग इंडिया गेट पर इकट्ठे होंगे। वे पोस्टर उठाएँगे, कुछ नारे देंगे, और लौट जाएँगे।
बाक़ी देश न देखेगा, न मानेगा कि हवा ज़हरीली है। और जब तक हम फिर से सोचने की आज़ादी नहीं सीखते — पढ़ने, बहस करने, संशय पालने की क्षमता नहीं लौटाते — तब तक हमारे विरोध क्षणिक रहेंगे, हमारा आक्रोश सुविधाओं में समा जाएगा, और हमारा लोकतंत्र आज्ञाकारिता को सहमति समझता रहेगा।