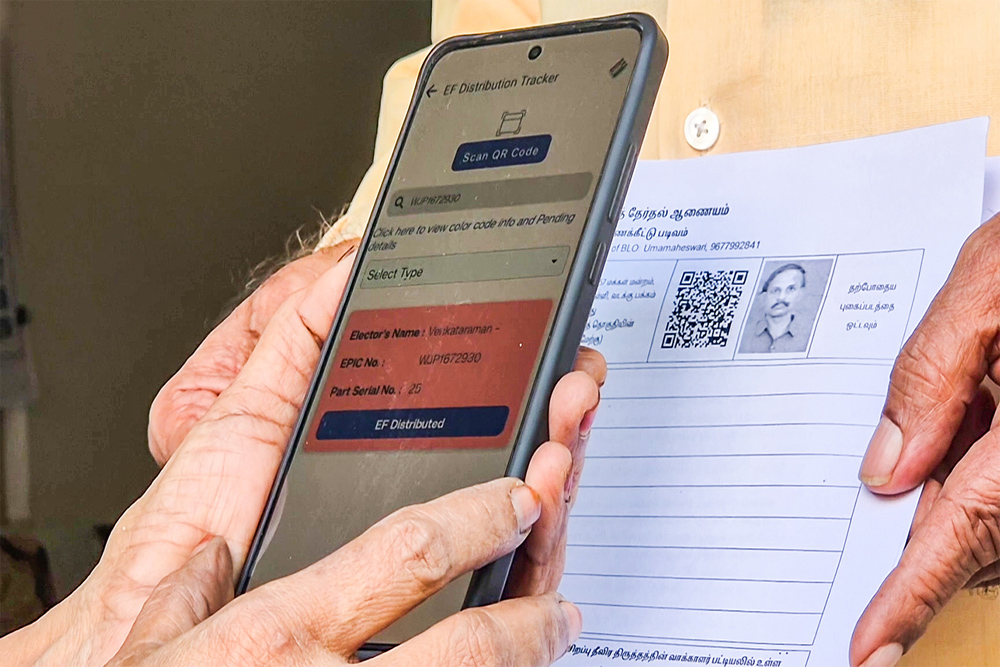विद्वानों के अनुसार उस समय विनायक को विघ्न डालने वाले जीव माना जाता था, जिन्हें शांत करने के लिए पूजा की जाती थी। बाद में यही विनायक विघ्नों के नाशक और मंगलकर्ता हो गए। गृहसूत्रों में विनायक को भूपति, भूतपति, भूतानापति और भुवनपति की उपाधियां दी गई हैं। माना जाता है कि मूलतः मूषक रुद्र का वाहन था, पर उत्तरवैदिक काल में वह गणेश का वाहन मान लिया गया और धीरे-धीरे गणेश रुद्र से स्वतंत्र देवता बन गए।
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से श्रीगणेश की भक्ति और भव्य पूजन की परंपरा शुरू हो जाती है। यह गणेशोत्सव चतुर्दशी तक चलता है और प्रतिमा विसर्जन के बाद इसका समापन होता है। मान्यता है कि गणपति के नाम-स्मरण, ध्यान-जप और आराधना से मन शुद्ध होता है, इच्छाएँ पूरी होती हैं, दुख-दुर्गति दूर होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। उनकी प्रसन्नता से घर-परिवार और समाज में निरंतर आनंद और मंगल का विस्तार होता है। भारत में किसी भी धार्मिक, मांगलिक या शुभ कार्य का आरंभ बिना गणपति पूजन के नहीं होता। यही कारण है कि मंदिरों से लेकर घर-दुकानों और व्यवसायिक स्थलों तक, हर जगह श्रीगणेश की प्रतिमा या प्रतीक चिह्न स्थापित दिखाई देते हैं। दीपावली पर भी लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा अनिवार्य मानी गई है।
‘गण’ शब्द का मूल अर्थ है – संख्या या समूह। इसके आगे ‘ईश’ या ‘पति’ जोड़ने से गणेश और गणपति शब्द बने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि गणेश यानी वह जो प्रकृति और जीव-जगत के सभी प्रख्यात पदार्थों का स्वामी और पालनकर्ता है। वेद मंत्रों में भी इसका संकेत मिलता है। पर आश्चर्य है कि तैंतीस वैदिक देवताओं की सूची में गणेश का सीधा उल्लेख नहीं है। फिर भी ऋग्वेद 2/23/1 और तैत्तिरीय संहिता 2/3/14/3 के मंत्र— “गणानां त्वा गणपतिं हवामहे…”—को विद्वान गणेश से जोड़ते हैं। इसमें ब्रह्मणस्पति को देवगणों और कवियों का स्वामी कहा गया है।
ब्रह्मणस्पति का अर्थ है मंत्रों का स्वामी, और यह उपाधि बृहस्पति को दी गई है। सायणाचार्य ने इसका अर्थ किया—देवगणों का स्वामी, यानी गणपति। शुक्ल यजुर्वेद 16/25 में भी गणपति शब्द आया है—“नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च…”—जहां देवताओं के अनुचरों और उनके अधिपतियों को नमस्कार किया गया है। महीधर ने इसके भाष्य में गणपति को देवों के अनुचरों का पालक बताया। शुक्ल यजुर्वेद 23/19 में भी गणपति का उल्लेख मिलता है, पर वहां देवता अश्व माने गए हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद और अन्य आचार्यों के अनुसार वैदिक देवताओं में गणेश का प्रत्यक्ष नाम नहीं आता, हालांकि आज उसी मंत्र का पाठ गणेश पूजन में होता है।
श्वेताश्वेतर उपनिषद जैसे प्राचीन उपनिषदों में गणेश का नाम नहीं है, पर गणपत्युपनिषद में गणपति, एकदन्त, वक्रतुंड, लम्बोदर और शिवपुत्र नाम से उनकी स्तुति मिलती है। तैत्तिरीय आरण्यक का मंत्र “तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि…” गणेश से जोड़ा गया है और इसका जप करने वाले को विघ्नों से मुक्ति और धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की प्राप्ति का विधान बताया गया है। यहां दन्ति और वक्रतुंड नाम गणेश की ओर संकेत करते हैं।
गृहसूत्रों में विनायक का उल्लेख स्पष्ट मिलता है। बोधायन गृहसूत्र 3/3/10 में विनायक की पूजा विधि बताई गई है। विद्वानों के अनुसार उस समय विनायक को विघ्न डालने वाले जीव माना जाता था, जिन्हें शांत करने के लिए पूजा की जाती थी। बाद में यही विनायक विघ्नों के नाशक और मंगलकर्ता हो गए। गृहसूत्रों में विनायक को भूपति, भूतपति, भूतानापति और भुवनपति की उपाधियां दी गई हैं। माना जाता है कि मूलतः मूषक रुद्र का वाहन था, पर उत्तरवैदिक काल में वह गणेश का वाहन मान लिया गया और धीरे-धीरे गणेश रुद्र से स्वतंत्र देवता बन गए।
महाभारत में गणेश और स्कंद को मानव शक्तियों के अधिपति कहा गया। धर्मसूत्रों में भी विनायक और स्कंद दोनों को शिवपुत्र के रूप में मान्यता दी गई और इनके लिए तर्पण का विधान हुआ। आगे चलकर विनायक गणेश कहलाए और वक्रतुंड, एकदन्त, लम्बोदर और विघ्नविनाशक नामों से प्रसिद्ध हुए।
आज गणेश पंचदेवों—विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश—में केवल सम्मिलित ही नहीं, बल्कि आदिपूज्य हैं। आरंभ में जिन्हें विघ्नों और बाधाओं का देवता माना गया, वही कालांतर में विघ्नराज से मंगलकर्ता, विघ्नपति हो गए। अब लोग उन्हें न सिर्फ विघ्न टालने के लिए बल्कि सिद्धि और सफलता पाने के लिए भी पूजते हैं।
पुराणों—जैसे पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मवैवर्त, स्कन्द, शिव और वराह पुराण—में गणेश के स्वरूप, जन्म, महिमा, व्रत-पूजन, मंत्र और लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। यहां उन्हें केवल शिव-पार्वती के पुत्र ही नहीं, बल्कि परब्रह्म, परमेश्वर और आदिपूज्य घोषित किया गया है।