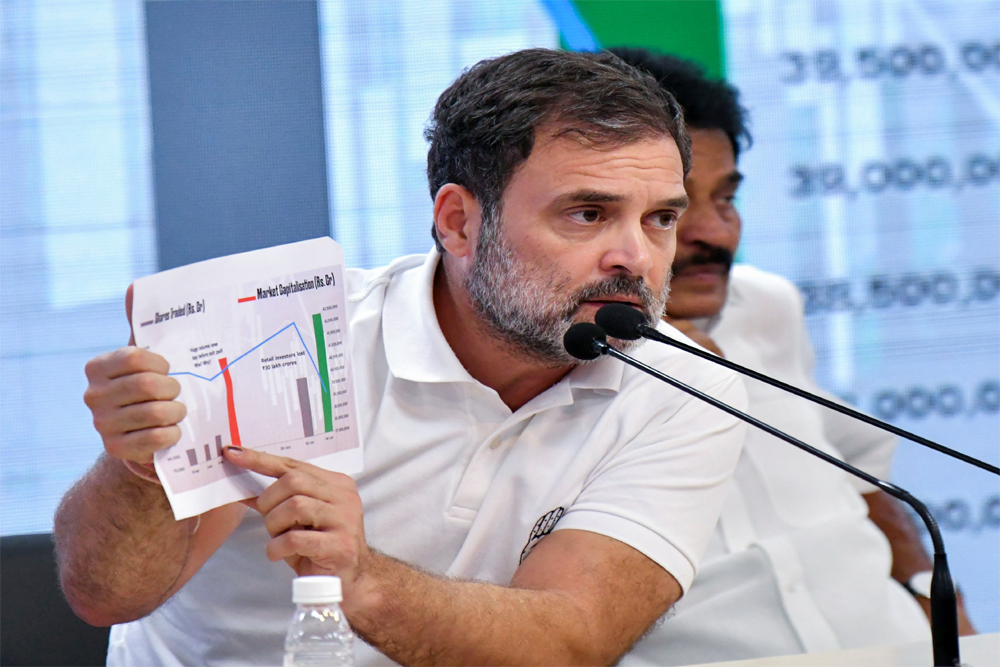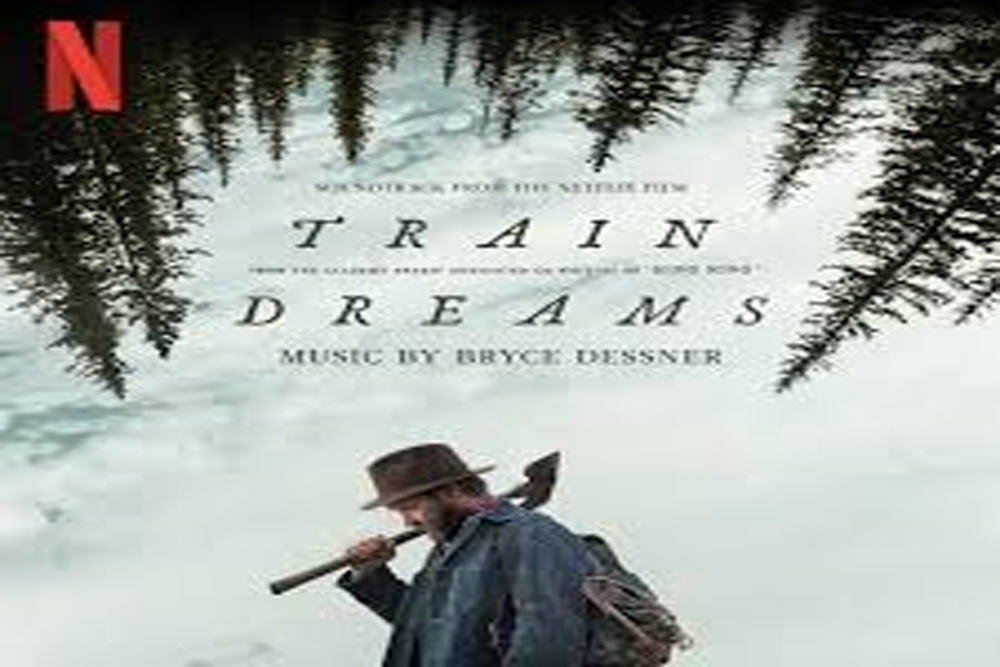विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है जिसका अर्थ है- सबके साथ मैत्री अथवा प्रेम। लेकिन वसिष्ठ द्वारा कामधेनु न देने पर उनसे शत्रुता, युद्ध और फिर पराजय की घटना के कारण वे अपकीर्ति के शिकार भी हुए। ऋग्वेद में अनेक मंत्रों से सिद्ध होता है कि विश्वामित्र यज्ञों में पुरोहित का कार्य करते थे, और वृत्ति के संबंध में इनमें तथा वशिष्ठ में बहुत समय तक बराबर झगड़े- बखेड़े होते रहते थे। वे एक दूजे के धुर विरोधी थे।
24 अक्टूबर – कार्तिक शुक्ल तृतीया- ऋषि विश्वामित्र जयंती
कुशिक गोत्रोत्पन्न कौशिक वंशीय राजा गाधि के पुत्र विश्वामित्र न केवल बड़े ही प्रतापी, पराक्रमी व प्रजावत्सल नरेश और तेजस्वी महापुरुष थे, बल्कि वैदिक काल के विख्यात ऋषि, महान विद्वान, 62 सूक्तों वाले ऋग्वेद के तीसरे मंडल और उसमें अंकित गायत्री मंत्र के द्रष्टा व पुरुषार्थ से ब्राह्मणत्व को सिद्ध करने वाले ब्रह्मर्षि भी थे। कान्यकुब्ज के पुरुवंशी महाराज गाधि के पुत्र विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर भी अपने तपोबल से ब्रह्मर्षियों में परिगणित हुए। इनका पहला क्षत्रिय नाम विश्वरथ था, जो ब्राह्मणत्व प्राप्त करने पर विश्वामित्र हो गया। ब्रह्रर्षि विश्वामित्र गाधिज, गाधेय और कौशिक भी कहे जाते हैं।
विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है जिसका अर्थ है- सबके साथ मैत्री अथवा प्रेम। लेकिन वसिष्ठ द्वारा कामधेनु न देने पर उनसे शत्रुता, युद्ध और फिर पराजय की घटना के कारण वे अपकीर्ति के शिकार भी हुए। ऋग्वेद में अनेक मंत्रों से सिद्ध होता है कि विश्वामित्र यज्ञों में पुरोहित का कार्य करते थे, और वृत्ति के संबंध में इनमें तथा वशिष्ठ में बहुत समय तक बराबर झगड़े- बखेड़े होते रहते थे। वे एक दूजे के धुर विरोधी थे।
वैदिक ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण, पुराणों, उपनिषदों आदि में अंकित प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की प्रचलित कथाओं के अवगाहन से स्पष्ट होता है कि विश्वामित्र भारत को समरस समाज, समदर्शी न्याय व्यवस्था और सर्वजन हितकारी गणतंत्र के रूप में देखना चाहते थे। उनकी समूची साधना और निष्काम तपोबल का महान लक्ष्य है- आर्यावर्त से आसुरी वृत्तियों का संहार। श्रीराम और लक्ष्मण उनके इस लक्ष्य में भागीदार बनते हैं और असुरों का संहार कर विश्वामित्र की आकांक्षा को गति देते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में राम-लक्ष्मण की दीक्षा से लेकर सीता स्वयंवर तक की कथा अपनी तार्किकता, सामाजिक प्रतिबद्धता तथा समकालीन चिंतनशीलता के कारण प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के भीतर स्वराज की स्थापना का विलक्षण विमर्श प्रस्तुत करता है।
गौतम ऋषि का अपराध बोध हो अथवा अहल्या का प्रायश्चित्त, परशुराम की भारत चिंता हो अथवा देवराज इंद्र की आसुरी वृत्तियां हों, मेनका के अपूर्व सौन्दर्य में छिपे कारुणिक प्रश्न हों अथवा उसके समक्ष निरुत्तर खड़े ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हों, सभी गाथाएं कथासूत्रों के माध्यम से जीवन, समय और समाज पर सभी दृष्टियों से गंभीर व महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। अहल्या, इंद्र और शची के प्रकरण अत्यंत रहस्यमयी चिंतन से दीक्षित करते प्रतीत होते हैं।
ऋषि विश्वामित्र का जीवनचरित एक साधारण क्षत्रिय राजा से शुरू होकर स्वाभिमान, अहंकार, आत्मसंघर्ष, गहन तप और अंततः ब्रह्मज्ञान के मार्ग से होकर ब्रह्मर्षि पद तक पहुंचने की कथा है, जो भारतीय संस्कृति में ब्राह्मणत्व की संकल्पना के प्राणतत्व- ब्राह्मण का अर्थ जन्मना जाति अर्थात केवल जाति विशेष नहीं, बल्कि ब्रह्मज्ञान, तपस्या, संयम, और सत्य के मार्ग पर चलने में सन्निहित है, के सिद्धांत को अक्षरशः सिद्ध करती है। राजर्षि से ब्रह्मर्षि पद प्राप्ति तक के उनके जीवनवृत से ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मणत्व की संकल्पना के इस प्राणतत्त्व पर बिलकुल खरे उतरते दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति में वे एक विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी नजर आते हैं। इस रूप में वे आत्मसंयम, तपस्या और स्वाभिमान के आदर्श हैं। उनका ब्राह्मणत्व उन्हें जन्म से नहीं, अपितु तप और साधना से प्राप्त हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय परंपरा में ज्ञान और आत्मविकास जन्म से उंचा मूल्य रखते हैं। विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय राजा गाधि के घर में हुआ। वे कौशिक वंश के सदस्य होने के कारण कौशिक कहे गए। वे राज्य, शक्ति और वैभव से पूर्ण यशस्वी राजा थे। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।
वशिष्ठ से मुलाक़ात, उनके आवभगत के लिए वशिष्ठ द्वारा नियुक्त कामधेनु गौ से प्रभावित होकर उसकी मांग करना, और वशिष्ठ के इंकार करने पर उनसे संघर्ष की घटना ने उन्हें राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने की मार्ग पर स्वतः ही चलायमान कर दिया और उन्हें यह समझ में आ गया कि शस्त्रबल से कोई भी ब्राह्मणत्व को नहीं छीन सकता। उनके भीतर की ज्वाला धधक रही थी। बहुत सोच विचारकर उन्होंने तप के बल से इसे अर्जित करने का निर्णय लिया। यहीं से एक राजा का हृदय तपस्वी में बदलने लगा। और फिर विश्वामित्र की तपयात्रा, परीक्षा, विघ्न और अंततः ब्रह्मर्षित्व की सिद्धि की राह पर चल निकली, लेकिन यह यात्रा उतनी सरल, सुगम, सीधी और आसान नहीं थी। उनके द्वारा राजसी जीवन, ऐश्वर्य और वैभव को त्याग कर चुना गया तप और साधना का मार्ग निरंतर परीक्षा, विघ्न और आत्म संघर्ष से भरा हुआ था। प्रारंभ में उनका उद्देश्य केवल आत्मकल्याण नहीं, बल्कि यह सिद्ध करना था कि तप, संयम और संकल्प के बल पर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस महान संकल्प के मार्ग में बार-बार इंद्र द्वारा मेनका अप्सरा प्रकरण आदि कृत्यों से बाधाएं उत्पन्न की गईं।
विश्वामित्र भी सुंदरता, कांति, स्वर, राग, सौंदर्य और आकर्षण की प्रतिमूर्ति अप्सरा मेनका के मोह से अपने को बचा न सके। दोनों के प्रेम के प्रतिफल में शकुन्तला की प्राप्ति के बाद ही वे मेनका के मोह जाल से मुक्त हो सके और फिर उन्हें अपने पराजय, पराभव का अनुभव हुआ। लेकिन विश्वामित्र के लिए यह पराजय नहीं, बल्कि सीख थी। उनका तप भंग हुआ, लेकिन यह कोई स्थायी पतन नहीं था। उन्होंने मेनका को विदा और अपनी पुत्री शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ कर अपनी नवीन आत्मबोध की खोज की मार्ग का अवलंबन किया। अब तक उन्हें यह समझ में आ चुका था कि ब्रह्मर्षि बनने के लिए केवल तप नहीं, बल्कि विकारों की शुद्धि भी आवश्यक है। विषय, वासनाओं से परे होना भी आवश्यक है। इसके साथ ही उनकी साधना बाह्य नियंत्रण से अंतरात्मा की विजय की एक नए मार्ग पर चल पड़ी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। और न केवल शरीर पर, बल्कि मन, वाणी और अहंकार पर भी नियंत्रण किया। इस तप के प्रभाव से ही उन्हें ब्रह्मा, शिव और अन्य देवों से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्र
ह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वायव्य, वज्र, आदि अनेक देवास्त्र उनके अधीन हो गए। अस्त्रों को चलाना ही नहीं, बल्कि उन्हें वापस लेना अर्थात संहरण विद्या की शिक्षा भी उन्हें प्राप्त हो गया। इस ज्ञान के कारण ही उन्हें सर्वास्त्रगुरु की उपाधि प्राप्त हुई। शनैः- शनैः विश्वामित्र ब्राह्मणों और राजाओं के समकक्ष आगे आकर शास्त्रों के ज्ञाता माने जाने लगे। ऋषियों की सभा में मान-सम्मान प्राप्त करने लगे। धर्म, दर्शन, वेद, मंत्र, यज्ञ और ध्यान में सिद्ध हुए। लेकिन उनका लक्ष्य तो वशिष्ठ के समकक्ष स्वीकार होना था। जो अभी पूर्ण नहीं हुआ था। और इसके लिए अहंकार का पूर्ण विसर्जन किया जाना आवश्यक था। संस्कृत के एक प्रख्यात सुभाषितानि -अहंकार ही बंधन है, और उसका त्याग ही मोक्ष है। – को स्वीकार कर ब्रह्मर्षि बनने से पहले विश्वामित्र को भी अपने अहंकार, अपने मैं को त्यागना पड़ा। और कठोर तपस्या के पश्चात विश्वामित्र का यह त्याग तब सिद्ध हुआ जब उन्होंने ब्रह्मा और अन्य देवताओं के समक्ष प्रत्यक्षतः प्रार्थना करते हुए यह स्वीकार किया कि उन्हें कोई पद अथवा स्वर्ग की इच्छा नहीं, न ही वेदों में अपना नाम जोड़ने की आकांक्षा है।
उन्हें स्पष्ट अपनी इच्छा जताते हुए कहना पड़ा कि यदि मेरी साधना सफल है, तो महर्षि वशिष्ठ मुझे ब्राह्मर्षि के रूप में स्वीकार करें। तब तक विश्वामित्र ने सारी इच्छाएं, काम, क्रोध, और अहंकार को जीत लिया था। उन्होंने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तब जाकर स्वयं देवताओं और ऋषियों ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की। प्रारंभ में विश्वामित्र को ब्राह्मण मानने से मना कर देने वाले स्वयं जन्मना ब्राह्मण तथा सप्तऋषियों में से एक ऋषि वशिष्ठ ने भी अपने पुराने और धुर विरोधी विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की सर्वोच्च उपाधि प्रदान करते हुए कहा कि ब्रह्मर्षिः त्वं विश्वामित्र। जन्मना ब्राह्मण और सप्तर्षियों में परिगणित वशिष्ठ कह उठते हैं-
ब्रह्म को जानने और उसे जीने के कारण अब तुम ब्रह्मर्षि हो।
लेकिन तब तक विश्वामित्र का क्रोध दूर हो चुका था। विश्वामित्र ने क्रोध त्याग दिया था। सामाजिक स्वीकृति की लालसा छोड़ दी थी। उन्हें इस उपाधि के मिलने या न मिलने से कोई मोह नहीं रह गया था। उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। अहं के पूर्ण विसर्जन के साथ ब्रह्म की स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाना ही तो ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। और विश्वामित्र तब तक अहं के पूर्ण विसर्जन के साथ ब्रह्म की स्थिति में प्रतिष्ठित हो चुके थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से यह सिद्ध कर दिया था कि ब्राह्मणत्व कर्म और ज्ञान से प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। तप, साधना, और आत्मसंयम से कोई भी आत्मिक उच्चता प्राप्त कर सकता है।
राजर्षि से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने वाले ऋषि विश्वामित्र की यह कथा वर्ण व्यवस्था के मूल सिद्धांत को तो चुनौती देती ही है, दूसरी ओर भारतीय दर्शन की लचीलापन और शिक्षा प्राप्ति के पश्चात गुण, कर्म देखकर निर्धारित की जाने वाली वर्ण व्यवस्था अर्थात योग्यता आधारित मानवीय मूल्यों को भी समाज के समक्ष लाती है। पुरुषार्थ से किसी भी लक्ष्य को पाने की शक्ति को उजागर करती है। वेद मंत्रों के द्रष्टा, श्रीराम के गुरु, मानव आदर्श के संस्थापक पुरुषार्थ से ब्राह्मणत्व को सिद्ध करने वाले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की पौराणिक गाथाएं आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणादायी साबित हो रही हैं, जिनकी आत्मिक उन्नति और आत्मविकास के मार्ग पर चलने की इच्छा है।