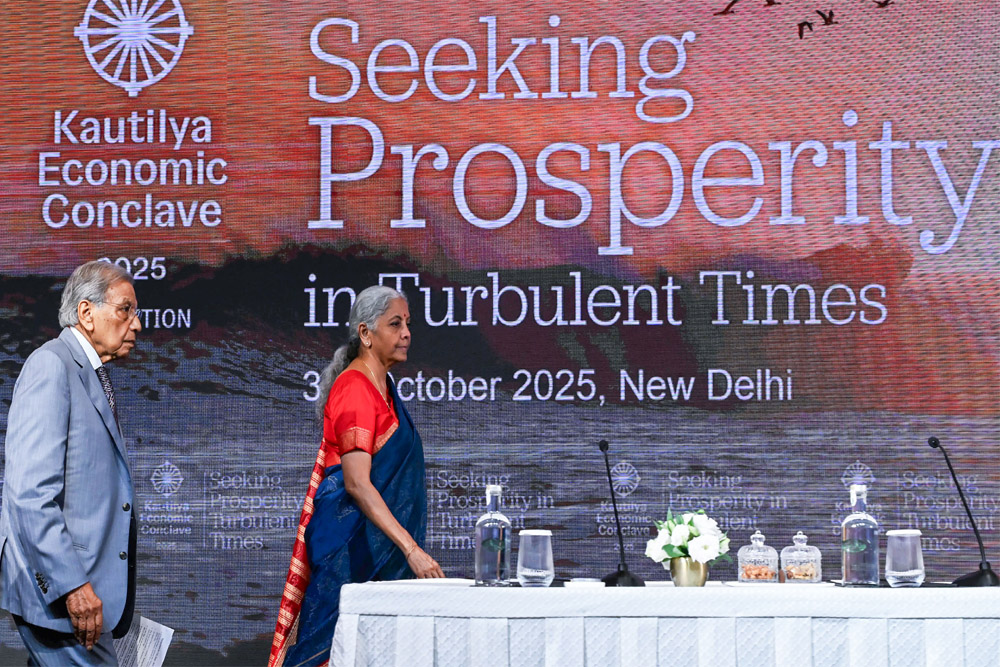प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में हर साल भारत को एक नए सवेरे का वादा मिला है! हर वर्ष का हिसाब यदि लगाए तो प्रति वर्ष नई थीम पर एक नारा, एक प्रण और शुरू एक काउंटडाउन। मतलब कल हमेशा नए नाम से, नई पैकेजिंग में लौट आता है! मानो पूरा देश एक स्थायी वेटिंग रूम में नए वादों की स्थाई इंतजारी की नियति लिए हुए हो। और ऐसा इस स्वतंत्रता दिवस पर भी हुआ। पुराना नारा नए मौसम के लिए चमका दिया गया—पुरानी शराब, नई बोतल। और सोमवार तक उसके पैकेज को सरकार ने बाकायदा और महत्वाकांक्षी, और तात्कालिक तथा लुभावना बना दिया।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नए नए जुमले के साथ नया अध्याय खोला—“100 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा”, और यह भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की तेज़ रफ़्तार यात्रा का कथित रोडमैप है। प्रधानमंत्री के लालक़िले के संकल्पों पर आधारित यह योजना पंच प्राणों का सहारा लेती है—एकता, कर्तव्य, धरोहर और औपनिवेशिक मानसिकता का त्याग। उन्होंने कहा कि हर नागरिक, इस सामूहिक सफ़र का हिस्सेदार बनेगा।
लेकिन यह सब सुनना अजीब तरह से क्या पहले जैसा ही कुछ नहीं है? वही अनुभव कि अगली पंद्रह अगस्त तक के लिए नया झूनझूना!
अब सबकों अनुभव है कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति डिलीवरी पर नहीं बल्कि लोगों की इंतज़ारी को आगे बढ़ाती हुई होती है। अब तो इंतजार का 1947 तक का समय तय हुआ है। ‘मेक इन इंडिया’ से ‘डिजिटल इंडिया’, आत्मनिर्भर भारत से अमृत काल तक—हर नारा वर्तमान को भूमिका बना देता है और असली वादा उस क्षितिज पर धकेल देता है, जो हमेशा सालो साल दूर खिसकता जाता है। कल की राजनीति देश की गति, रफ्तार का आयाम बनता है, पर अभी तक जो हुआ है, आज का हिसाब नहीं करती। यही कारण है कि “100 दिन का एजेंडा” एक नई शुरुआत से ज़्यादा एक दोहराई हुई स्क्रिप्ट लगती है। भारत यह धुन पहले भी सुन चुका है—परिवर्तन, तेज़ रफ़्तार, नियति। अगर अब हम दौड़ने का संकल्प ले रहे हैं, तो पिछले ग्यारह साल क्या कर रहे थे? अगर 2047 मंज़िल है, तो हम अभी भी एजेंडे, घोषणा की बाते ही क्यों करते हुए है? क्यों शुरुआती लाइन पर खड़े हैं?
यह याद रखने लायक है कि भारत ने पहले भी एक ऐसे दौर को जिया है जब विज़न गढ़े जाते थे। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्टील कारखानों, वैज्ञानिक संस्थानों और बाँधों को “आधुनिक भारत के मंदिर” कहा था। तब यह केवल कथा थी, दृष्टि का छलावा। पर समय बीतने के साथ प्रतीक ढाँचे बने—ईंट-पत्थर में जमी महत्वाकांक्षाएँ। प्रगति के अमूर्त विचार को आकार मिलने लगा। फ़ैक्टरी फ़्लोर पर चला जा सकता था, बाँध की दीवारें उठते देखी जा सकती थीं, आईआईटी परिसर में दाख़िला लिया जा सकता था। यह उस भविष्य के ठोस प्रमाण थे जो बन रहा था।
अब ढर्रा बदल गया है। अब अमूर्त विकसित भारत है। मोदी सरकार की “कल की राजनीति” याकि 2047 की बाते, झांकी अलग तरह की है। उनके नारे—मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अमृत काल—ठोस नींव, ठोस इमारत, ठोस निर्यात व्यापार, ठोस कल-कारखानों में नहीं बल्कि जुमलों, भावनाएँ और वादे, संकल्प लिए हुए हैं। अब योजना-काम- परिणाम की पंचवर्षीर्य योजनाएं नहीं है बल्कि इंतज़ार और काउंटडाउन की कोरियोग्राफ़ी पर पनपते हैं, जहां भविष्य हमेशा सुनहरा होता लगेगा लेकिन हमेशा टलता हुआ और टाइमलाईन बढ़ाता हुआ। जबकि नेहरू ने कम-से-कम संस्थान बनाए, वे कारखाने-बांध खड़े किए थे जिन्हें मापा जा सकता था। वही प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहानी-कथाएँ सुनाते है जिन्हे बार-बार दोहराते हुए भी यह नहीं लगता है कि वे थक रहे हो या लोग सुनते-सुनते थक गए हो।
इस स्क्रीप्ट में नया “100 दिन का एजेंडा” सटीक है। यह तात्कालिकता को दृश्य बनाता है—मानो बारहवें साल में भी सरकार अभी-अभी दौड़ शुरू कर रही हो। लेकिन अगर अब तेज़ रफ़्तार है, तो पिछले ग्यारह साल क्या थे? अगर 2047 मंज़िल है, तो स्टेशन पर क्या तब तक इंतज़ार ही करते रहना है? क्यों? यह सिर्फ़ भाषण का सवाल नहीं है, यह नई राजनीति का एक चिरस्थाई सा ढाँचा बनता लगता है। हमेशा वादा, मगर शायद ही कभी डिलीवरी और कभी खत्म नहीं होने वाला सिलसिला।
2020 का आत्मनिर्भर भारत अभियान याद कीजिए। महामारी के चरम पर जब सप्लाई चेन टूट रही थी, प्रधानमंत्री ने असुरक्षा, आपदा को ही अवसर बता बड़े सपने बनाए थे। आत्मनिर्भरता सरकार की नीति नहीं बल्कि दर्शन बना दी गई—मानो यह नियति हो। शब्दों ने आत्म निर्भरता को दृढ़ संकल्प का रूप दिया। उस क्षण में हौसला बढ़ा, पर प्रयोगशालाएँ, सप्लाई चेन, निवेश—जिनसे सच्ची आत्मनिर्भरता आती है—कभी नहीं बने। पाँच साल बाद नारे और वास्तविकता का अंतर और गहरा है। तेल से लेकर सेमीकंडक्टर तक, भारत अब भी आयात पर निर्भर है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ़ नीतियाँ—आज 25%, कल 50%—उस मायाजाल को तार-तार बना देती हैं, जो विपक्ष के बूते में भी नहीं है। समय ही बताता है कि न भारत आत्मनिर्भर हुआ है और उसके दूर-दूर तक कोई लक्षण है।
और यह नेहरू के “आधुनिक मंदिरों” बनाम मोदी के संकल्पों, एजेंडों, जुमलों और “नारों” का बुनियादी फर्क है। नेहरू के स्टील प्लांट, रिफाईनरी, सरकारी प्रतिष्ठानों, बाँधों ने लोगों का विस्थापन किया हो या सरकारी भ्रष्टाचार बनवाया हो, वे संस्थान लड़खड़ाए, बावजूद इसके वे सब आज भी खड़े हैं। उनकी आलोचना हो सकती है, समीक्षा हो सकती है, सुधार हो सकता है। मगर जुमले और नारे तो आलोचना से भी परे हैं। संकल्पों और प्रतिज्ञाओं को कोई नहीं मांप सकता है बस उन्हे दोहराते रहा जाता है।
इसीलिए “100 दिन का एजेंडा” अपने वादों से ज़्यादा सियासी डिज़ाइन को उजागर करता है। तात्कालिकता यहाँ डिलीवरी नहीं, बल्कि झांकी व दृश्य है। यह एक ऐसे शासन का आभास देता है, जो मानो नयी ऊर्जा से दौड़ रहा हो, जबकि वह असल में सत्ता में बारहवें साल में है। काउंटडाउन पॉलिटिक्स—100 दिन, 5 प्रण, 2047—मोदी युग के गवर्नेंस की वह व्याकरण है जो संख्यात्मक, लयबद्ध, दोहराने में भरपूर आसान है लेकिन रियलिटी और अनुभवों में मापने में कठिन।
वाणिज्य मंत्री गोयल ने एजेंडा विरासत, परंपरा और औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति को फ़्रेम में रखा। इससे विकास एक सभ्यतागत परियोजना में बदल जाता है, जिसमें कठिनाइयाँ “देशभक्ति का त्याग” कहलाती हैं। नौकरियाँ नहीं आतीं, अस्पताल फंड नहीं पाते, स्कूल पिछड़ते हैं—तो इसका कारण बताया जाता है कि हम औपनिवेशिक बोझ उतार रहे हैं। सो नागरिकों को सिर्फ़ लाभार्थी नहीं बल्कि त्यागी सैनिक बनना चाहिए ताकि हम एक ऐसे मार्च, एक ऐसी परेड़ का हिस्सा बने जिसका गंतव्य 2047 होगा। अर्थात हमेशा कल।
लेकिन नारों पर कविता कर सकते है लेकिन उसके लिए आंक़ड़े, अंक कैसे बनेगे? भारत तो जीडीपी का केवल 0.7% अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है। मतलब अमेरिका (3.6%) और चीन (2.4%) से बहुत पीछे। वैश्विक नवाचार सूचकांक पर भारत 39वें स्थान पर है। बेरोज़गारी रिकॉर्ड स्तर पर है, कृषि संकट हर साल गहराता हुआ है, और जलवायु आपदाएँ—बाढ़, भूस्खलन, लू—अब मौसम की परिभाषा बन चुकी हैं। इस सबकों, तमाम समस्याओं को क्या सिर्फ वादों से सुलझाया जा सकता? जाहिर है विकास ख्याली- स्मृति–कार्य नहीं है बल्कि ठोस कारखानों (कैसे बांग्लादेश ने भारत को परंपरागत वस्त्र उद्योग में भी पछाडा), ढाँचे, निवेश और नवाचार से बनता है। जब तक भारत इसकी बुनियाद पर निवेश याकि प्रयोगशालाएँ, मज़बूत सप्लाई चेन, स्वास्थ्य, शिक्षा को सुधारेगा नहीं कोई खांका नहीं बनना है।
सो कहानी सिर्फ़ अर्थशास्त्र की नहीं, राजनीति के स्वरूप की है। शासन अब कार्यक्रमों से कम और प्रदर्शन से ज़्यादा जुड़ा है। आत्मनिर्भर भारत कोई नीति दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक कथा थी। 100 दिन का एजेंडा कोई सुधार ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि एक कागजी पटकथा भर है। इसका मक़सद डिलीवरी नहीं, बल्कि ध्यान भटकाना है—आज की समस्याओं से नज़रें हटाकर कल्पित भविष्य की ओर मोड़ना।
शायद इसी कारण मोदी की राजनीति लगातार उड़ती हुई है। इससे नागरिकों को केवल नीतियाँ नहीं, बल्कि नियति, कर्तव्य और सभ्यता के बड़े आख्यान, कथाएं मिलती है। कठिनाई त्याग बन जाती है; देरी अनुशासन। जहां नीति फिसलती है, वहां कविता संभाल लेती है।
लेकिन दुनिया का मामला अलग है। वह इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होती। ट्रंप के टैरिफ़ सिर्फ़ व्यापार नीति नहीं, बल्कि आईना हैं। वे दिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता के नारे और बाहरी निर्भरता का अंतर्विरोध कितना गहरा है। और पता पड़ता हैं कि जुमलों की कथा रणनीति का विकल्प नहीं है और देश का नरेटिव कंट्रोल बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को कतई बचा नहीं सकता। भारत दुनिया की अगली कार्यशाला बनने का दावा करता है, लेकिन बिना नवाचार के वह दूसरों की डिज़ाइन का कारख़ाना भर रहेगा। 140 करोड लोगों की एक विशाल अर्थव्यवस्था, लेकिन औसत नवाचार प्रोफ़ाइल वाली।
इस तरह बात फिर कल पर आ ठहरती है। जैसे-जैसे भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, यह सवाल बनेगा कि क्या हम मंदिर बनाएँगे या टैगलाइन गढ़ेंगे? नेहरू की विरासत पर विवाद हो सकता है, पर उसने भारत को बहस करने लायक ढाँचा तो दिया था। उस नाते मोदी की विरासत कहीं ज़्यादा क्षणभंगुर न रह जाए—प्रदर्शन की राजनीति, जो वादों को हमेशा टालती रहती है। “100 दिन का एजेंडा” निस्संदेह सुर्खियाँ बटोरेगा। यह अगले 100 दिनों का आख्यान बनेगा, जब तक कि कोई नई कछा, नया नारा न गढ़ लिया जाए। पर भारत तो कुल मिला कर उसी कल (2047) की ओर मार्च करता रहेगा—जो कभी आता ही नहीं।