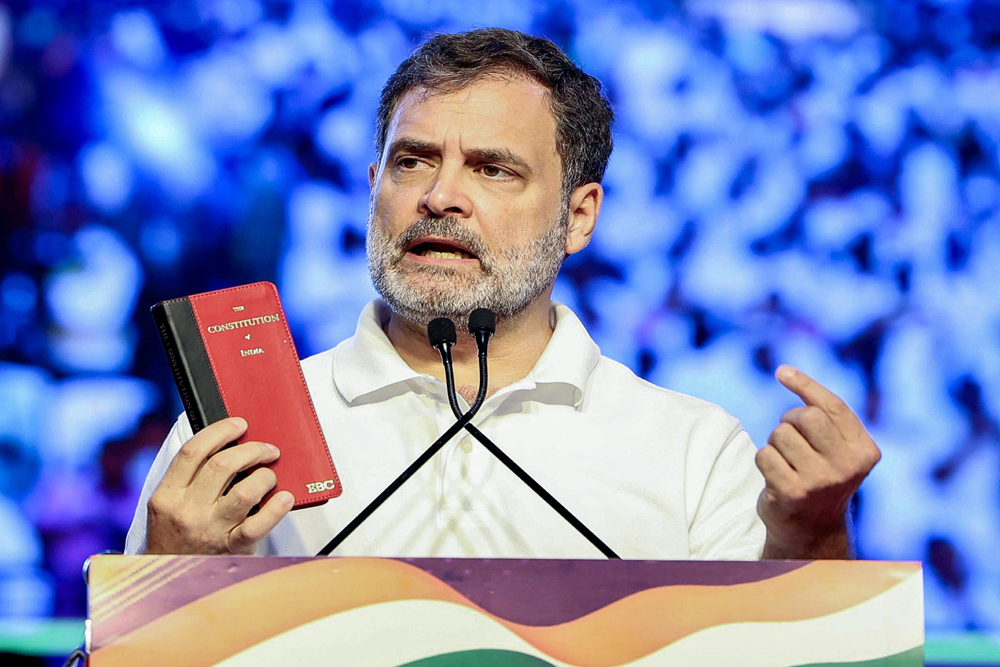कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर आपको चकाचौंध नहीं करता है बल्कि वो धीरे-धीरे आपको अपने भीतर खींच लेता है। वह आपको एक ऐसे समय में ले जाता है जहाँ भव्यता सांस थी और आस्था, श्रद्धा स्वाभाविक। जब शहर ईश्वर के लिए गढ़े जाते थे, न कि मुनाफ़े, अंहकार या दिखावे के लिए। जब वास्तुकला अहंकार नहीं, ईश्वर को एक अर्पण हुआ करता था। जब शांति युद्धों के बीच का विराम नहीं होता था बल्कि उस दुनिया की सहज एक धड़कन थी जो अभी भी भव्यता का बोध कराती, संवाद करती होती है।
मैं अंगकोर वाट मंदिर गई हूं। उसकी उसका विस्तार देख कर स्तब्ध हुई थी। वो वाला स्तब्ध होना एक अलग ही तरह का था, जो धीरे-धीरे भीतर उतरता है। स्केल चौंकाता ज़रूर है, हाँ—लेकिन जो भीतर ठहर जाता है, वो है उसकी पवित्रता (स्केल चौंकाता है, हाँ—but what lingers is the sanctity) हर गलियारा मानो एक भूली हुई सच्चाई फुसफुसाता है: कभी वह सुंदरता, दिव्यता, आस्था का पुंज था, भाषा थी।
मंदिर तब बना था जब खमेर साम्राज्य अपने शिखर पर था—9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच। तब वहा लाखों लोग बसे थे और मंदिरों का निर्माण ऐसा हुआ जो आज की अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्थाएँ भी सपना नहीं देख सकतीं। इसका हृदय था अंगकोर वाट—एक मंदिर जो मूलतः विष्णु को समर्पित था, हिंदू ब्रह्मांड की संरचना पर आधारित, खाइयों, मीनारों और पौराणिक चित्रकथाओं से सुसज्जित। इतना विस्तृत, इतना बारीक कि 19वीं सदी में जब फ़्रांसीसी प्रकृतिविद हेनरी मुहो ने इस मंदिर परिसर को “पुनः खोजा,” तो उन्होंने लिखा—“यह यूनान और रोम द्वारा छोड़ी गई किसी भी वास्तु से अधिक भव्य है।”
लेकिन हर महान सभ्यता की तरह, कंबोडिया की सभ्यता भी बाद में टूटी। युद्धों में, जंगलों में, विस्मृति में।
मगर मंदिर बचे रहे। कला ने न सिर्फ़ समय के झंझावत झेले, बल्कि उस साम्राज्य को भी पीछे छोड़ दिया जिसने उसे जन्म दिया था। अंगकोर टिका रहा—क्योंकि उसे टिकने के लिए ही रचा गया था।
और उसके बाद जो हुआ, वो दुर्लभ है—सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं, राष्ट्रीय गौरव, आस्था व श्रद्धा।
कंबोडिया ने, नरसंहार और त्रासदी के बावजूद, इस मंदिर की स्मृति को मिटाया नहीं, बल्कि उसे सचमुच पुनर्जीवित किया।
आज अंगकोर अकेला नहीं खड़ा, वह नियत और नीति से खड़ा है। प्रवेश के लिए पास, टिकट अनिवार्य है, आवागमन इलेक्ट्रिक रिक्शा से होता है, और इंस्टाग्रामmers के बीच भी यहां एक अजीब सी नीरवता बनी रहती है। यह मंदिर जैसा ही लगता है—थीम पार्क नहीं। और पूरी दुनिया से लोग उसे देखने जाते है।
लेकिन फिर, 2024 में, कंबोडिया ने सिर्फ़ अपनी धरोहर को संरक्षित नहीं किया।
उसके लिए लगभग युद्ध छेड़ दिया।
इस सप्ताह थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पाँच दिन का जो सशस्त्र संघर्ष छिड़ा है वह प्रेह विहेर को लेकर है।
और यह भी एक और प्राचीन मंदिर है, एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित। दो देशों की ताजा भिडंत में 40 लोग मारे गए है, हज़ारों विस्थापित है। गोलाबारी तब थमी जब कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौते रद्द करने की धमकी दी। दुनिया के लिए, सबके लिए चौकने वाली बात यह है कि 21वीं सदी में भी 12वीं सदी के मंदिर के लिए युद्ध! इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों में विरासत, परंपरा अब भी अर्थ रखती है।
कंबोडिया के लिए खमेर साम्राज्य द्वारा बनाए गए मंदिर उसकी आत्मा हैं—युद्धों के बचे, पहचान के साक्ष्य। थाईलैंड भी इन्हें अपना मानता है—पूर्व-औपनिवेशिक मानचित्रों का हवाला देकर। इन मंदिरों पर विवाद 2008 से चला आ रहा है, जब थाई प्रदर्शनकारियों ने प्रेह विहेर पर चढ़ाई की थी। राजनीति चाहे जितनी उलझी हो, भावना स्पष्ट है: वो अपने खंडहरों के लिए भी लड़ने को तैयार हैं।
अब फ्रेम बदलिए। भारत और पाकिस्तान की ओर आइए।
हमने भी युद्ध लड़े हैं—हाल ही में, बार-बार। लेकिन सीमाओं के लिए, न कि विरासत के लिए।
आतंकवाद पर लड़े, भूमि के लिए लड़े, मगर मंदिरों के लिए, संस्कृति-सभ्यता की धरोहर के लिए कभी नहीं। जबकि हमारा अतीत 1947 से कहीं गहरा है।
हम एक ही सभ्यता से जन्मे थे—सिंधु घाटी से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में, धोलावीरा और राखीगढ़ी भारत में। ऐसे नगर जो रोम और एथेंस से भी पहले के हैं—जहाँ की नालियाँ, भंडारगृह, और शहरी नियोजन आज की सरकारें भी पढ़ सकती हैं। लेकिन ये स्थल युद्ध में नहीं, बल्कि चुप्पी में धीरे-धीरे खो रहे हैं।
मोहनजोदड़ो, यूनेस्को टैग के बावजूद, धीरे-धीरे ढह रहा है। पाकिस्तानी पुरातत्वविद आए दिन चेतावनी देते हैं—लेकिन उन्हे पैसा, फंड्स नहीं मिलते। भारत में राखीगढ़ी मे सिर्फ़ चुनाव के समय थोड़ी धूल झड़ती है। खुदाई अधूरी, संग्रहालय योजना अधर में, और भारत के लोग अनजान।
धोलावीरा को कभी-कभार यूनेस्को से ज़िक्र मिलता है, पर देखभाल नहीं।
यहाँ एक सभ्यता है—वेदों से भी प्राचीन, विभाजन से भी गहरी लेकिन कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता। कभी नहीं उठाई। भारत और पाकिस्तान ने चार युद्ध लड़े, पर कभी हड़प्पा या मोहजोदड़ो की रक्षा के लिए, सांस्कृतिक विरासत के केंद्रों, स्मृतियों के लिए नहीं। हमें 1947 जरूर याद है लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों अपने मूल जन्मकाल के 3000 ईसा पूर्व भूल चुके हैं।
ठिक दूसरी तरफ कम से कम कंबोडिया और थाईलैंड को तो भारतीय संस्कृति से प्राप्त विरासत, उन स्मृतियों की याद है! और वे उसके लिए लड़ रहे हैं। जबकि हम, भारत के 140 करोड़ लोगों को तो यह भी ध्यान नहीं है कि हमने क्या खो दिया है।
इसलिए भारत के भीतर की कहानी भी कुछ अलग नहीं है।
यह वही देश है जिसने नालंदा को जन्म दिया, अजंता को तराशा, काशी की कल्पना की।
लेकिन हम भारतीयों ने एक कला गढ़ ली है, दिमाग में इतना भर पैंठाया है या तो इसे सड़ने दो, या नाम बदल दो, रंग पोत दो, दोबारा इस्तेमाल कर लो। और दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता की प्राचीन पांडुलिपियाँ बंद अलमारियों में दीमक के हवाले हैं।
भारत में मंदिर अब राजनीतिक फ़ोटू खिंचवाने की पृष्ठभूमि बन गए हैं। संग्रहालय वो गेस्ट हाउस बन चुके हैं जहाँ न क्यूरेटर है, न रोशनी—सिर्फ़ तब जगमगाते हैं जब कोई मंत्री फोटो-ऑप के लिए आता है।
देखिए सरस्वती नदी परियोजना को— हज़ारों साल बाद, एक नदी को डिजिटल रूप में फिर से ‘जिंदा’ करने की कोशिश। पर उसके किनारे के पुरातात्विक स्थल चुपचाप मिटते जा रहे हैं।
तारखानवाला डेरा, जो कभी प्रमुख हड़प्पा स्थल था, अब अवैध ईंट भट्टों के नीचे है।
बरोर अनियंत्रित निर्माण की भेंट चढ़ गया। 60 प्रतिशत से ज़्यादा स्थल पहले ही गायब हो चुके हैं—कभी स्थानीय अनभिज्ञता से, तो कभी सरकारी उदासीनता से।
यह संरक्षण नहीं, प्रदर्शन है। और फिर है दिल्ली।
लुटियन्स दिल्ली एक जटिल, परतदार प्रयोग थी— औपनिवेशिक जड़ों वाली ज़रूर, पर भारतीय सभ्यता के संकेतों से गूंथी हुई। मुगलों से लाल बलुआ पत्थर, यूनान से भव्य धुरी। हिंदू, जैन, बौद्ध शिल्प परंपराओं से अलंकरण। उसका दिल था—सेंट्रल विस्टा। एक लोकतांत्रिक गणराज्य की गति का दृश्य रूपक।
आज वह दृष्टि धीरे-धीरे, सोच-समझकर ध्वस्त की जा रही है। बिमल पटेल—मोदी के “नए भारत” के वास्तुकार—पहले साबरमती को सीमेंट कर चुके हैं। अब दिल्ली की आत्मा समतल की जा रही है। राजपथ से नालंदा तक, वाराणसी से जयपुर तक— पुराने को दोबारा कल्पना नहीं दी जा रही बल्कि उसे मिटाया जा रहा है। बिना कल्पनाशीलता के।
दिल्ली और हमारे ज़्यादातर शहर संकट में हैं—राजनीतिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक। और इस संकट को एक अवसर की तरह देख कर राजधानी को समावेशी और कल्पनाशील रूप देने की बजाय, हमने चुना है—मिटा देना।
वास्तुकला, अपने सर्वोत्तम रूप में, हमारी आत्मा का प्रतिबिंब होती है। सिर्फ़ इमारतें नहीं, बल्कि स्मृति और पहचान की संरचनाएँ। आज की पुनर्रचना सिर्फ़ एक शहर नहीं बदल रही— वो एक गहरा सच उजागर कर रहा है: हम क्या बना रहे हैं, यह कम महत्वपूर्ण है। हम क्या दफ़ना रहे हैं, यही असली सवाल है। इसलिए अब प्रश्न यह नहीं कि विरासत किसकी है— बल्कि यह है, क्या जब वह पूरी तरह खो जाएगी, तो हम उसे क्या पहचान भी पाएँगे?
या हम तब तक इंतज़ार करेंगे—जैसा हम करते आए हैं— जब तक संग्रहालय की आख़िरी तस्वीर धुँधली न हो जाए, आख़िरी मूर्ति काँच के पीछे टूट न जाए, और अगली पीढ़ी का कोई बच्चा एक पट्टिका पढ़े जिस पर फीकी स्याही में लिखा हो— “यह कभी हम थे।”
कंबोडिया और थाईलैंड भले ही खंडहरों के लिए युद्ध कर रहे हों— पर कम से कम उन्हें याद है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। उनकी संस्कृति, सभ्यता की भव्यता, मौलिकता क्या थी? मूल क्या था?
और भारत?
हम या तो अपनी धरोहर को दोबारा पेंट कर रहे हैं, या उसे वक़्त के हवाले चुपचाप सड़ने दे रहे हैं।