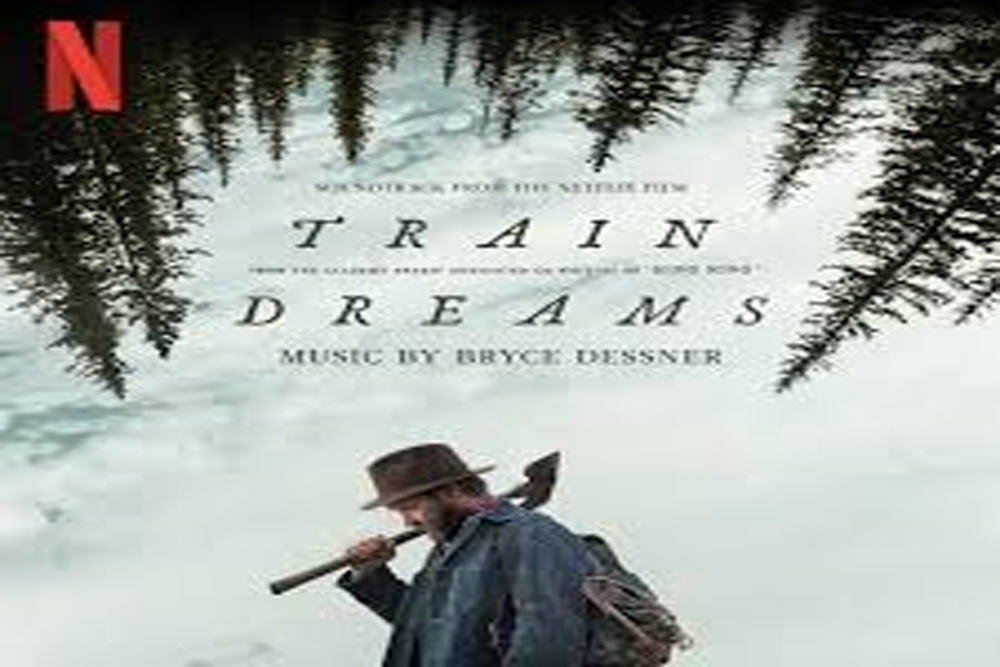हिंदी को अहिंदी राज्यों में अलगाव में थोपने के बजाए हिंदी को जोड़ने व संपर्क भाषा होना हैं। हिंसा तो सत्ता खोने के डर से या सर्वसत्ता पाने की लालसा से ही उकसाई जाती है। समाज अपने व्यवहार की भाषा जानता-समझता है लेकिन सत्ता अपनी व्यवस्था-व्यापार की भाषा कब सुधारेगी? पण सत्तेचे ध्येय फक्त सत्ता आहे।
भाषा के सदाचार से ही समाज में सदविचार और सद्भावना कायम होती हैं। इसलिए भाषा के लिए किसी के भी जीवन को दाव पर लगाना, हिंसा करना न अपनी भाषा से प्रेम जताता है। न ही मानवता से। और मानवता से प्रेम किए बिना भाषा का गर्व दर्शाना असंभव है। एक तरफ भाषा पर गर्व करना और दूसरी ओर मनुष्य को ही गरियाना, ना नैसर्गिक है। न भाषा की सभ्यता। जिसमें भाषा की सभ्यता है उसकी ही सभ्यता में भाषा टिक सकती है। फिर मुंबई में मराठी पर हिंसा क्यों हो रही है?
भाषा आपसी संचार व व्यवहार का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो अपने विचार, भावना और अनुभव को व्यक्त करने में मदद करती है। भाषा ही संस्कार और साहित्य के अलावा संस्कृति व सभ्यता के विकास में भूमिका निभाती है। अपने यहां सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली आज हिंदी है। भाषा के विद्वान मानते हैं कि एक मातृभाषा होती है और दूसरी संपर्क या व्यवहारिक भाषा। फिर ग्लोबल होती दुनिया में व्यावसायिक या धंधे की भाषा भी रही है। समय से सभी भाषाएं समान रूप से विकसित होती रही हैं। और हमें शिक्षित करती रही हैं।
आज अपन देश में भाषा के शिक्षण और विकास को कैसे देखें? मातृभाषा है जो परिवार में माता-पिता के साथ रहते हुए जन्म से सीखते हैं। वो आसपास रहने वाले समुदाय से अपने को विरासत में मिलती है। जैसे बांग्ला, मराठी, तमिल, पंजाबी या अन्य राज्य भाषाएं। राज्यों के विभिन्न भाषियों को जोड़ने वाली दूसरी संपर्क भाषा है जो अपन अपने रोजमर्रा के विचार, व्यवहार व भाव के लिए उपयोग में लाते हैं। अंग्रेजों के आने के बाद से वह अंग्रेजी हो गयी।
जबकि अनेकता में एकता की बात करने वाले अपने विद्वान स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे कि अपनी संस्कृति, संस्कार व व्यवहार को जोड़ने की भाषा हिंदी हो। अंग्रेजी से मुक्ति पाकर संपर्क की भाषा हिंदी हो। इसलिए राष्ट्रीय खेल, पक्षी व झंडे की तर्ज पर हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो सके। लगातार बदलते समय व समीकरण में यह होना असंभव रहा। फिर एक रोजगार या व्यवसाय की भाषा है जिसमें अपन देश-विदेश में व्यापार व उद्योग करते हैं जो अंग्रेजी ही रही है। यह सब समझने के लिए अपने को वैज्ञानिक नहीं होना है।
आज सभी जानते हैं कि मराठी भाषेचा इतिहास खूप जुना आहे। संस्कृत से निकली प्राकृत, और फिर उससे ही निकली मराठी। हर भारतीय अपनी विभिन्न भाषाओं की विविधता पर गर्व कर सकता है। संस्कार, साहित्य व सहजीवन का आदान-प्रदान करता है। समझने की कोशिश करता हूं तो पिता मालवा के इंदौर से तो मां राजस्थान के मारवाड़ से। दादा-दादी, बुआ-चाचा मालवी व मराठी दोनो फर्राटे से बोलते रहे। अपन जन्म के लिए इंदौर से कानपुर आए तो वहां नाना-नानी मारवाड़ी व कनपुरिया हिंदी बोलते थे। फिर शिक्षा-दीक्षा दिल्ली व चंडीगढ़ के हरियाणवी-पंजाबी माहौल में हुई। चौदह साल क्रिकेट खेलने इंग्लैंड आना-जाना चला। मुंबई में नौकरी की, और घर दिल्ली में बसाया। मातृभाषा का अपने को ‘म’ भी नहीं आता। आज जरूर कोशिश है कि जिससे संपर्क हो उसकी बोली-भाषा सीखने का। ताकि व्यवहार, व्यवस्था व व्यापार का समभाव, सद्भाव बने।
जिन गुजराती महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंग्रेजी की जगह हिंदी को संपर्क भाषा बनाने का आवाहन किया था उनके मन में देश की एकता और जनता की स्वतंत्र सोच सर्वोपरि थी। राष्ट्रीय भाषा की इमारत को राजकीय भाषाओं की नींव पर खड़ी करना चाहते थे। क्योंकि व्यवहार की एकता के बिना व्यवस्था की स्वतंत्रता संभव नहीं। सरल और सुगम राष्ट्रभाषा से धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में संपर्क साधा जा सके। खुद गांधीजी अपने अंतिम समय तक ग्यारह भाषाएं सीखने का कहते थे।
आज स्थिति दूसरी और जटिल है। सत्ता जिस विचार का व्यवहार देश में रख रही है वैसे ही व्यवहार का विस्तार राज्यों में देखा जा रहा है। विचार शून्यता व्यवहार क्षुब्धता में देखी जा सकती है। जो सत्ता के केन्द्र में चल रहा है वही राज्यों के केन्द्र में चलाया जा रहा है। हिंदी को अहिंदी राज्यों में अलगाव में थोपने के बजाए हिंदी को जोड़ने व संपर्क भाषा होना हैं। हिंसा तो सत्ता खोने के डर से या सर्वसत्ता पाने की लालसा से ही उकसाई जाती है। समाज अपने व्यवहार की भाषा जानता-समझता है लेकिन सत्ता अपनी व्यवस्था-व्यापार की भाषा कब सुधारेगी? पण सत्तेचे ध्येय फक्त सत्ता आहे।