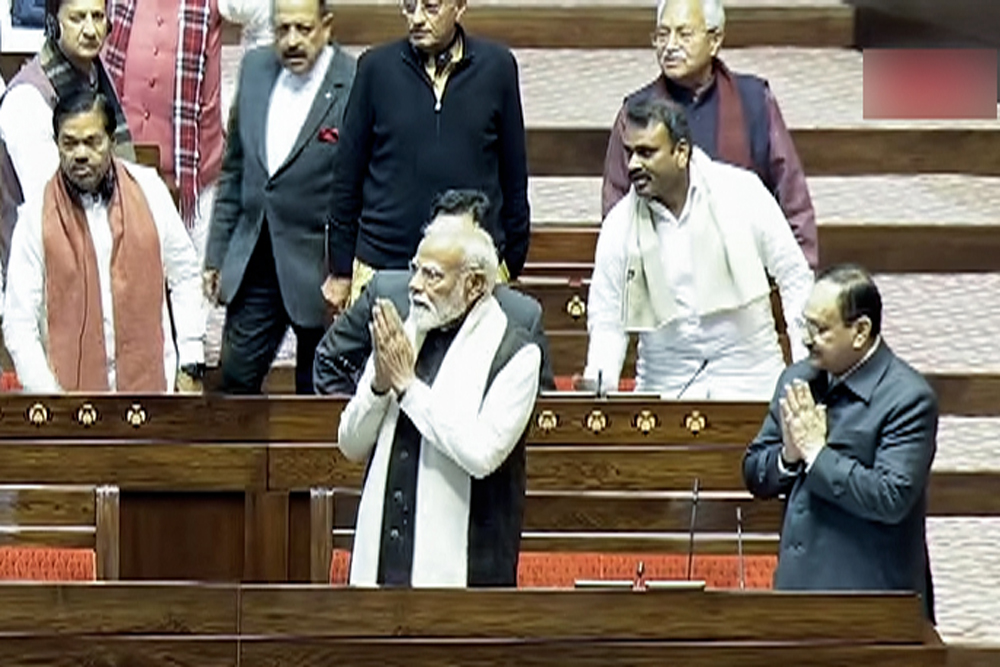आज से पचास पहले एक मई 1975 को हिंदी रंगमंच में एक नया प्रयोग किया गया। एनएसडी के पूर्व निदेशक एवं प्रसिद्ध रंगकर्मी देवेंद्रराज ‘अंकुर’ ने प्रख्यात कथाकार निर्मल वर्मा की तीन कहानियों को मिलाकर ‘कहानी का रंगमंच’ नामक नई विधा को जन्म दिया। गत 50 सालों में उन्होंने पांच सौ कहानियों के शो किए जो अपने आप में एक रिकार्ड है। इस प्रयोग के 50 साल पूरे होने पर विशेष लेख।
क्या राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के पूर्व निदेशक एवं प्रसिद्ध रंग निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर द्वारा शुरू की गई नई विधा ‘कहानी का रंग मंच’ हिंदी का ‘पुअर थिएटर’ है या उससे कुछ मिलता जुलता है। दरअसल यह सवाल पिछले दिनों इसलिए उठा क्योंकि ‘कहानी के रंगमंच’ के 50 वर्ष होने पर ‘कथा रंग’ समारोह के उद्घाटन अवसर पर प्रसिद्ध लेखक एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी ने श्री अंकुर की इस विधा का जिक्र करते हुए पोलैंड के मशहूर नाट्य सिद्धांतकार ग्रोटोव्स्की का उल्लेख किया। पहले यह बता दिया जाए कि आखिर यह ‘पुअर थिएटर’ है क्या? दरअसल इस ‘पुअर थिएटर’ की अवधारणा जेर्जी ग्रोटोव्स्की ने विकसित की थी। उन्होंने 1968 में ‘टुवर्ड्स ए पुअर थिएटर’ नामक किताब ही लिखी थी। उसके पीछे उनकी मान्यता थी कि कम से कम या न्यूनतम साधनों और उपकरणों के जरिए भी रंगमंच किया जा सकता है। उसमें किसी तामझाम की जरूरत नहीं है क्योंकि अंततः रंगमंच के जरिए हम कथ्य को ही उभारते हैं, इसलिए रंगमंच में साज सज़्ज़ा और अन्य साधन उपादान उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जितना अभिनय। हालांकि अशोक वाजपेयी ने यह भी बताया कि ग्रोटोव्स्की को इस अवधारणा के पीछे प्रेरणा भारत के संस्कृत के नाटकों से मिली थी।
देवेंद्र राज अंकुर के ‘कहानी के रंगमंच’ को देखते हुए क्या यह बात कही जा सकती है कि वह भी इस ‘पुअर थिएटर’ को हिंदी में विकसित करना चाहते हैं और पिछले 50 सालों में उन्होंने ‘कहानी का रंगमंच’ नामक नR नाट्य विधा को विकसित कर एक तरह से ग्रोटोव्स्की की अवधारणा को हिंदी में पेश किया है ।दरअसल यहां यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि देवेंद्र राज अंकुर के नाटकों में न्यूनतम साधनों का इस्तेमाल किया जाता है और वह कहानी की आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक विधा को दूसरी विद्या में इस तरह से रूपांतरित करते हैं कि जो कहानी अपने पढ़ी है, वह आपको मंच पर उसी तरह दिखाई दे जो कहानी का टेक्स्ट है। यानी कहानी का एक तरह से रंगमंच में अनुवाद किया गया। वह नाट्य रूपांतर उस तरह से न हो जैसे कई बार कृतियों का नाट्य रूपांतर किया जाता है।
देवेंद्र राज अंकुर ने एक मई 1975 को प्रख्यात कथाकार निर्मल वर्मा की तीन अलग अलग कहानियों ‘वीकेंड’, ’डेढ़ इंच मुस्कान’ और ‘धूप का एक टुकड़ा’ को मिलाकर पहली बार ‘कहानी का रंगमंच’ का प्रयोग किया था और यह मंचन संगीत नाटक अकादमी के तीसरे तल पर बने स्टूडियो थिएटर में हुआ था। इसे देखने निर्मल वर्मा भी आए थे। वे अक्सर रिहर्सल देखने भी आते थे। जब विष्णु प्रभाकर, असगर वज़ाहत आदि की कहानियों का मंचन हुआ तो वे लोग भी रिहर्सल देखने आते थे। मंन्नू भंडारी के महाभोज का मंचन हुआ तो नेमिजी ने ‘दिनमान’ में बहुत तारीफ़ भी की लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह हिंदी रंगमंच का एक नया अध्याय बन जाएगा। पिछले दिनों जब उनकी इस विधा के मंचन के 50 वर्ष पूरे होने पर सात नाटकों का समारोह ‘कथा रंग’ हुआ तो लोगों को अहसास हुआ कि यह तो एक महत्वपूर्ण इतिहास बन गया है।
इसमें सात कहानियों की रंग-प्रस्तुतियां हुईं, जिनमें `जोगिया राग’ (विजय पंडित), `उसके हिस्से का प्रेम’ और `गरीब नवाज’ (संतोष चौबे), ‘एक स्त्री के कारनामे’ (सूर्यबाला), ‘बेटियां मन्नू की’ (प्रियदर्शन द्वारा मन्नू भंडारी की कहानियों पर आधारित) `अयोध्या बाबू सनक गए हैं’ (उमाशंकर चौधरी) और ‘समाप्ति’ (रवीन्द्र नाथ टैगोर) शामिल हैं। इनमें सूर्यबाला और संतोष चौबे जैसे लोगों को भी शामिल किया गया जो हिंदी की मुख्यधारा के लेखक नहीं हैं।
अंकुर जी विभिन्न सभागारों में हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों का मंचन करते रहे हैं, जिनमें से प्रेमचंद से लेकर युवा कथाकार उमाशंकर चौधरी की कहानी शामिल है। यह अलग बात है कि उनकी निगाह राजा राधिका प्रसाद सिंह की कहानी ‘कानों में कंगना’ और शिवपूजन सहाय की कहानी ‘कहानी का प्लॉट’ तथा बेनीपुर की कहानी ‘जुलेखा पुकार रही है’ पर नहीं गई। निर्गुण की कहानी ‘साबुन’ और भगवती प्रसाद वाजपेयी की ‘मिठाईवाला’ भी मंचित हो सकती थी।
बहरहाल यह उनका चुनाव है कि वह किन कहानियों को मंचित करें या ना करें। किन कहानियों में उन्हें ‘नाट्य तत्व’ नजर आए या न आए लेकिन इस विधा के 50 साल पूरा होने के अवसर पर नाट्य जगत में उनके इस काम का स्वागत किया जाना चाहिए। वाकई उन्होंने इन पांच दशकों में एक बहुत बड़ा काम किया है जिसकी तरफ रंग प्रेमियों का ही नहीं, बल्कि मीडिया का भी ध्यान जाना चाहिए। अंकुर जी ने इन पांच दशकों में करीब पांच सौ से अधिक कहानियों का मंचन किया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूं तो कई मशहूर नाटकों के पांच सौ से भी अधिक मंचन हुए हैं लेकिन अंकुर ने कहानियों के पांच सौ शो का मंचन किया है, यह महत्वपूर्ण बात है। उनकी इस विधा पर अब शोध कार्य होना चाहिए कि कैसे कहानी को रंगमंच पर प्रस्तुत कर हिंदी रंगमंच को समृद्ध किया गया। असल में रंगमंच में लोग अक्सर शिकायत करते थे कि हिंदी में अच्छे नाटक नहीं हैं। शायद यह कारण रहा हो कि अंकुर ने हिंदी की कहानियों में ‘नाटक तत्व’ को देखते हुए उन्हें एक नाटक के फॉर्म में मंचित करने के बारे में सोचा। वैसे तो कहानी ही नहीं कविता और उपन्यासों को भी मंचित किए जाने की लंबी परंपरा हिंदी में मौजूद रही है और यही कारण है कि प्रेमचंद के ‘गोदान’, ‘रंगभूमि’ और श्रीलाल शुक्ल के ‘राग दरबारी’ से लेकर मन्नू भंडारी के ‘महाभोज’ तक को भी मंचित किया गया और वह काफी लोकप्रिय हुआ।
यशस्वी कवि रघुवीर सहाय ने एक जमाने में हिंदी की कविताओं को भी मंचित करने की शुरुआत की थी और उन्होंने दिल्ली में कई महत्वपूर्ण कविताओं का मंचन भी किया था। युवा कवि व्योमेश शुक्ल, निराला की कालजयी काविता ‘राम की शक्ति पूजा’ की मंचीय प्रस्तुति लगातार कर रहे हैं। मुक्तिबोध की ‘अंधेरे में’ धूमिल की ‘पटकथा’ के भी मंचन हुए हैं। साहित्य के लिए और कलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण बात होगी कि एक विधा को दूसरी विधा में अधिक से अधिक रूपांतरित किया जाए ताकि उसका प्रचार हो। कई बार कोई रचना दूसरी विधा में जाकर अपने ज्यादा अर्थ प्रकट करती है तो कई बार वह अपना अर्थ खो भी देती है या अर्थ को विरूपित भी कर देती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस रचना को दूसरी विधा में रूपांतरित करने वाला निर्देशक, अभिनेता और संवाद लेखक कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है।
हिंदी की कई कृतियों पर कई फिल्में बनी हैं, उनमें कुछ अच्छी भी बनी है तो कुछ बुरी भी बनी है और यही बात रंगमंच पर भी लागू होती है। पिछले दिनों रंगमंडल ने धर्मवीर भारती की कहानी ‘बंद गली का आखिरी मकान’ का मंचन किया तो अंकुर जी ने इस एक कहानी को दो शैलियों में पेश किया, जिसमे दोनों शैलियां अलग अलग ढंग से एक ही तथ्य को पेश करती हैं लेकिन दोनों की प्रस्तुति अलग है। यह भी एक नया प्रयोग था हालांकि कुछ लोगों को कोई एक प्रस्तुति पसंद आई तो किसी को दूसरी प्रस्तुति पसंद आई लेकिन सम्मुख वाली प्रस्तुति में अंकुर जी ने न्यूनतम साधनों का इस्तेमाल कर बेहतर प्रस्तुति पेश की थी। इसी तरह उन्होंने मन्नू भंडारी की कहानियों पर प्रियदर्शन के लिखे नाटक ‘मंन्नू की बेटियों’ का मंचन किया तो वह एक नया प्रयोग था और वह सराहा गया।
‘कहानी का रंगमंच’ को कैसे और लोकप्रिय बन जाए इसके बारे में रंग जगत को सोचना चाहिए। इससे न केवल हिंदी में नाटकों का अकाल समाप्त होगा, बल्कि दर्शकों को हिंदी कहानियों की सभी परंपरा को भी जाने का मौका मिलेगा क्योंकि कई बार देखा गया है कि रंगमंच की दुनिया में एक ही नाटक को बार बार खेला जाता है। चूंकि वह नाटक बहुत पहले लिखा गया होता है इसलिए उसमें सम सामयिक संदर्भ कम होते हैं लेकिन हिंदी में हर रंग की कहानी लिखी जा रही है इसलिए अपने समय को चित्रित करने वाली कहानी मिल जाएगी, जिसका मंचन करने से हम अपने समय और समाज को सही ढंग से चित्रित कर सकेंगे और दर्शकों को जोड़ सकेंगे।