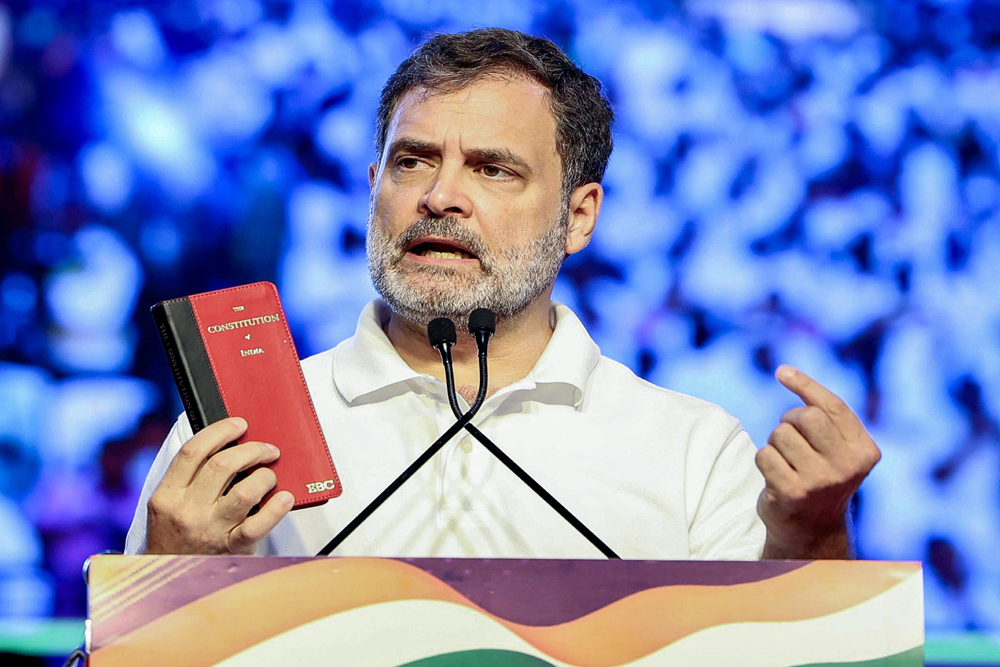साफ दिख रहा था, और वह असहज था तो चेताने वाला भी। उमस से भरी झुलसाती दोपहर में कुछ नौजवान लड़के और महिलाएं फुटपाथ पर चुपचाप खड़े थे, उनके पैरों के पास खाली डिब्बे, टेढ़ी-मेढ़ी बाल्टियाँ, प्लास्टिक की बोतलें थी। वे पानी के टैंकर का इंतज़ार कर रहे थे। न हड़बड़ी में थे, न बातचीत करते हुए- बस एक अजीब-सी ख़ामोशी, जो व्यवस्था, हालतों के आगे लाचारी से उपजी थी। हर कोई गर्दन झुकाए अपने मोबाइल की स्क्रीन में डूबा हुआ था। बड़े, चटक रंगों वाले फोन पर उनके पतले हाथों, और भी पतली ज़िंदगियों की उंगलियाँ स्वाभाविक गति से चल रही थीं—स्क्रॉल करते हुए, स्वाइप करते हुए।
मैंने गाड़ी में बैठे-बैठे अनायास ही बुदबुदाया, “पानी नहीं है, नौकरी नहीं है… पर फोन तो है! और उससे टाइमपास करने के लिए वक्त ही वक्त।”
बगल में बैठे आशीष ने कहा- “यही है टेक्नॉलजी का उदय और नए भारत का पुनर्जागरण।”
शायद वो ग़लत नहीं था।
स्वागत है नए भारत में—मोबाइल से चिपका, उसकी लत में डूबा और लगातार ऑनलाइन टाइमपास।
कहते है भारत में लोग अब औसतन पाँच घंटे मोबाइल पर बिताते हैं—ज़्यादातर सोशल मीडिया, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में। और अब यह सिर्फ़ मनोरंजन नहीं है, यह पहचान है, यह अर्थव्यवस्था है। अब बच्चों का सपना भी सरकारी नौकरी, अफ़सर, डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनना पहले नहीं है बल्कि वायरल होना पहला शगल है।
आजकल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते नौजवान ऐसे व्लॉग करते हैं जैसे वे किसी प्रेरक डॉक्युमेंट्री के नायक हों। जैसे “यूपीएससी छात्र के जीवन का एक दिन”—में सुबह पाँच बजे उठना, नींबू-शहद वाला पानी पीना, ‘द हिंदू’ को किसी थ्रिलर की तरह पढ़ना, स्किनकेयर रूटीन दिखाना और फिर कोचिंग सेंटर जाना। यदि परीक्षा में पास नहीं भी हुए , तो मेकअप ब्रश और नाश्ता तो मोनेटाइज़ हो ही सकते हैं। अब अपना रूतबा एक रेफ़रल कोड के साथ आता है।
और यह सिर्फ़ नौजवानों की बात नहीं है।
अब दादी-नानी इंस्टाग्राम पर ‘वेलनेस इन्फ्लुएंसर’ हैं—तकनीकी रूप से दक्ष पोतों द्वारा प्रशिक्षित, वे हल्दी वाला दूध, ठंडा तेल, और मुँह साफ़ करने वाला जप साझा करती हैं। वे प्यारी हैं, भरोसेमंद हैं, और एल्गोरिदम की पसंदीदा। घरेलू महिलाएं अब छुपी, अदृश्य नहीं रहीं—वे अब ‘होम एस्थेटिक क्वीन’ हैं। उनका हेयरवॉश एक फिल्म ट्रेलर की तरह एडिट होता है। उनका तड़का कंटेंट है। पति के साथ दिया गया कैंडल लाइट डिनर एक कैप्शन वाला पल है—‘ग्रेसफुल ग्रैटिट्यूड’।
जाहिर है यह मात्र कंटेंट नहीं है। ये एक नई आस्था है। हर रील के साथ। हर रील, एक आस्था।
और ये सिर्फ़ बोर होती औरतें, सपनों में खोए किशोर या छोटे शहरों के संघर्षरत कलाकार नहीं हैं—ये डॉक्टर हैं, कोडर हैं, इंजीनियर हैं। हर कोई अब आधा वक्त ऑनलाइन जी रहा है।
आज सब ऑनलाइन हैं। सब परफॉर्म कर रहे हैं।
और इसी बीच समाज चिंतित होकर पूछता है: संस्कार कहाँ गए? आज के युवा आपसी बातचीत या साथ में क्यों नहीं बैठना व गपशप चाहते है? नई पीढ़ी को संवाद, रिश्ते, अपनापन क्यों नहीं समझ आता? लेकिन सच कहें तो—ये मूल्य सिखा कौन रहा है? बूढ़े भी फोन में खोए हैं—कभी साज़िश वाले फॉरवर्ड्स, कभी फनी फ़िल्टर वाले रील्स। फैमिली डिनर अब एकसाथ खाना नहीं, एकसाथ स्क्रॉल करना हो गया है।
संस्कार नहीं ग़ायब हुए बल्कि उन्हें स्क्रीन और रील्स ने रिप्लेस कर दिया।
मुझे याद है जब सोशल मीडिया कुछ ख़ास था।
फेसबुक मेरे जीवन में इंडिया से पहले आया। यूनिवर्सिटी ईमेल से लॉगिन, चुनिंदा दोस्त, बॉस्टन और एडिनबरा के हॉस्टलों के बीच चलती बातचीत के समय। फिर आया इंस्टाग्राम—और लगा शायद मैं फोटोग्राफर बन सकती हूं। फ़िल्टर ने मेरी तस्वीरों को रोमांटिक बना दिया—जैसे जीवन कवितामय हो गया हो। मुझे लगा कि फोटो जर्नलिज़्म मेरी क़िस्मत है।
मैंने ट्विटर से कभी मोह नहीं पाला। 140 कैरेक्टर्स में व्यंग्य, ग़ुस्सा और बारीकी कैसे डालूं? लेकिन वक़्त बीतता गया। मैं एक ऐसी पत्रकार बनी जो फ़ुटनोट्स और फाइन प्रिंट्स में सच्चाई ढूंढती थी। और सोशल मीडिया भी बढ़ता गया—ज्यादा तेज़, ज्यादा तेजतर्रार, खुद से ही लती।
पहला सोशल मीडिया स्टार थे बराक ओबामा। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने पॉपस्टार की तरह प्रचार किया। फिर आए नरेंद्र मोदी—जिन्होंने सिर्फ़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, सबको इसके इस्तेमाल के लिए मजबूर कर दिया।
2014 तक, भारतीय राजनीति स्क्रीन में बदल गई थी। माध्यम ही संदेश बन गया।
2019 में सब बदल गया—रैलियाँ यूट्यूब पर लाइव, घोषणापत्र किसी आईफ़ोन लॉन्च जैसा, और ‘चाय पर चर्चा’ इंस्टा लाइव। राजनीति अब 9 बजे टीवी पर नहीं देखी जाती, ये आपके फोन में है, चाचाजी के व्हाट्सएप में है। और सबकी उंगलियाँ एक जैसी—थोड़ी झुकी हुई, स्क्रॉलिंग मोड में, जिसे कहते है आईफ़ोन फिंगर—नई लोकतांत्रिक पहचान।
2024 के चुनाव आते-आते, नेता पत्रकार नहीं, कंटेंट क्रिएटर्स ढूंढ रहे थे। इन्फ़्लुएंसर अब इंटरव्यू लेते हैं। पत्रकारिता को ‘लीगेसी फ़ॉर्मेट’ बना दिया गया। पत्रकार अब यूट्यूब शो, इंस्टा रील, ट्विटर थ्रेड्स में ख़ुद को रीपैकेज कर रहे हैं। सच नहीं, अब ‘रीच’ मायने रखती है। अब कोई नॉर्थ ब्लॉक के बाहर इंतज़ार नहीं करता। प्रेस क्लब में कानाफूसी नहीं होती। लीक हुई फ़ाइल नहीं मिलती। हर ख़बर अब व्हाट्सएप फ़ॉरवर्ड है। पहला पिंग ही पहला पोस्ट है।
न्यूज़रूम अब एक्सक्लूसिविटी नहीं, समानता के पीछे भागते हैं।
50 हज़ार फॉलोवर हों या 5 मिलियन—सब एक ही ब्रेकिंग न्यूज़, एक ही बयान, एक ही बाइट पोस्ट करेंगे—बस फ़िल्टर अलग होगा। इंटरव्यू थके हुए हैं, सवाल रीसायकल, जवाब रिहर्स्ड।
पत्रकार अब एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के बीच भाग रहे हैं। वे अब सत्य के गेटकीपर नहीं हैं, पर कंटेंट क्रिएटर हैं—ट्राइपॉड और माइक के साथ, एल्गोरिद्म की दया पर।
जानकारी अब पत्रकारिता की शुरुआत नहीं, उसका अंत बन गई है।
मीडिया संस्थानों का एकाधिकार चला गया—वो संकट नहीं है। संकट यह है कि पत्रकारिता ने अपनी कल्पना खो दी है। एक सीनियर संपादक ने एक बार कहा था—“जानकारी पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता जानकारी के बाद शुरू होती है—विचार, विश्लेषण, और व्याख्या से। फर्क है—अनुशासन का।”
और आज की हरपल चलती दुनिया में, अनुशासन ट्रेंड नहीं करता।
ग्यारह साल पहले जिस सरकार ने ‘नवीनता’ के वादे पर सत्ता पाई थी, उसने वाकई कुछ नया दिया—प्रगति नहीं, पर बदलाव। एक नया मूड, एक नई शब्दावली। जहां अब ‘रीच’, ‘ऑप्टिक्स’, ‘इन्फ्लुएंस’ जैसे शब्दों का वजन ‘सच’, ‘स्पष्टता’ और ‘परिणाम’ से कहीं ज़्यादा हो गया है। आज का भारत विचारकों या निर्माता राष्ट्र नहीं है—यह कलाकारों का देश है।
स्टेज अनंत है, तालियाँ मूक हैं, दर्शक हमेशा ऑन है। और इसीलिए, वह दृश्य सामान्य लगने लगा है—जो कभी असहज था।
जले हुए फ़ुटपाथ पर खड़े लड़के और औरतें, पैरों के पास जंग लगे डिब्बे, एक टैंकर का इंतज़ार जो शायद कभी न आए। ना विरोध, ना बेचैनी, ना पानी, ना काम—बस ख़ामोशी। और स्क्रीन। वक़्त है, पर उद्देश्य नहीं। उम्मीद नहीं, बस टाइमपास है।
यही है आज की सामान्यता।
नया भारत पूरी तरह ऑनलाइन है—सजाया-संवारा हुआ, बेचैन, और प्रदर्शनशील। यहां महत्वाकांक्षा अब उठती नहीं, बस रिफ़्रेश होती है। शांति से किसी चीज़ का इंतज़ार करने का आत्मसम्मान अब नहीं बचा—उसे जगह दी गई है देखे जाने की बेचैनी को।
और इस निरंतर चलते-फिरते डिजिटल शोर में, आप महसूस कर सकते हैं—एक चुपचाप होती क्षरण। आर्थिक नहीं, कल्पना की। राजनीति नहीं, उद्देश्य की।
तो अब मैं आपको छोड़ती हूं इसी सोच के साथ की जब फीड शांत हो जाएगी, स्क्रीन बुझ जाएगी, और ये डिजिटल शोर एकदम से चुप हो जाएगा, तब क्या बचेगा हमारे भीतर?
जब न स्क्रॉल बचेगा, न ऑडियंस, न कोई बच निकलने की योजना—तब हम क्या करेंगे? और सबसे अहम—हम लौटकर कहां जाएँगे?