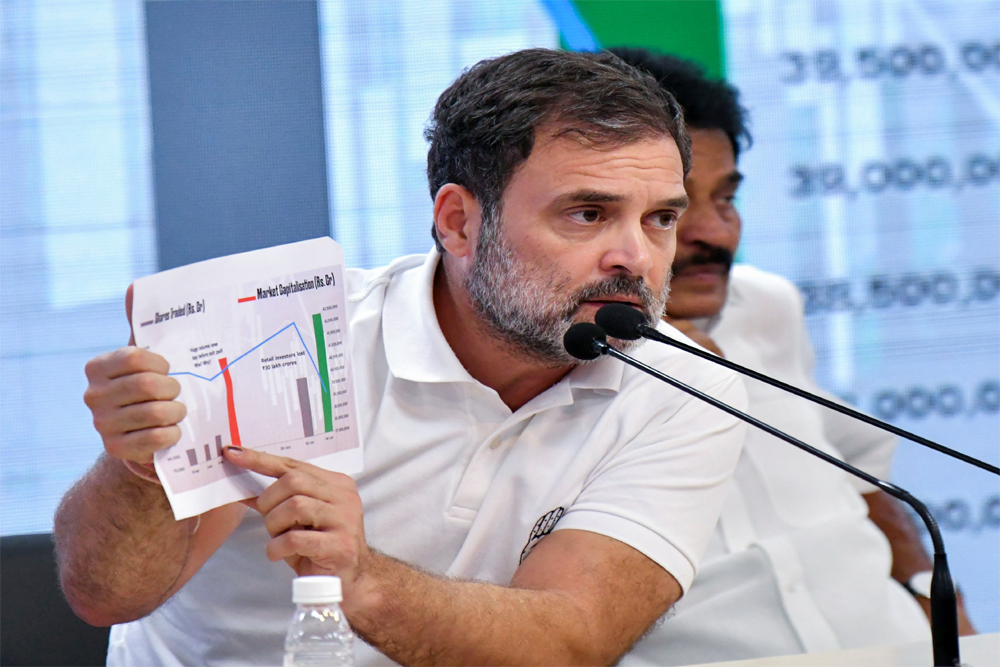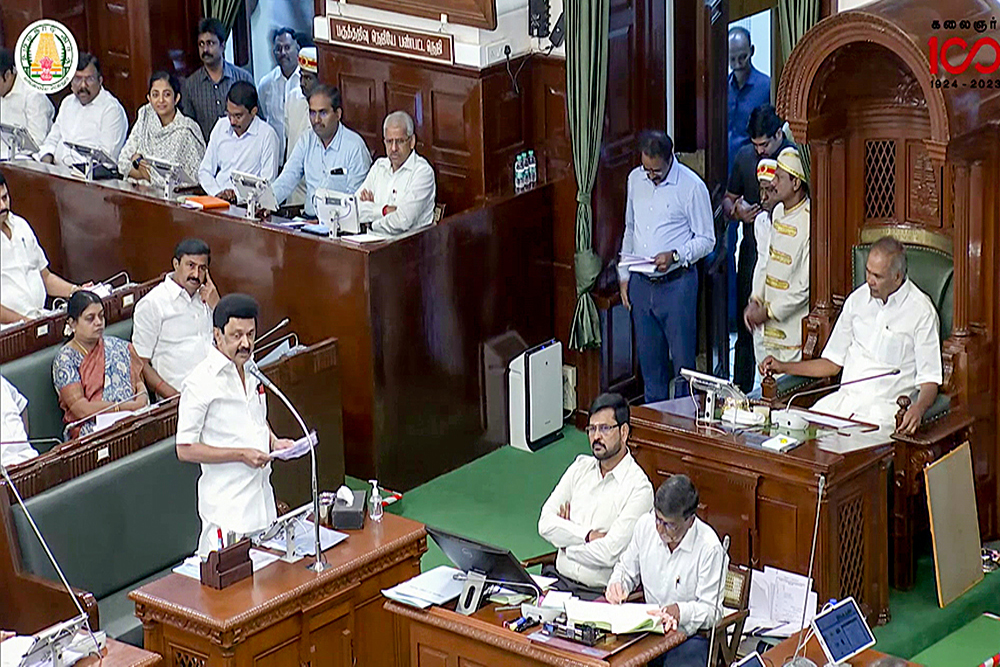पड़ोसी देशों में बेहतर संबंध हों, यह अपेक्षित है। लेकिन यह भी उतना ही अहम है कि यह किन शर्तों पर संभव है। इसलिए यह जरूरी है कि निर्णय समग्रता में और दूरदृष्टि का परिचय देते हुए लिया जाए।
खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने चीन जाएंगे। इस घटना का प्रतीकात्मक महत्त्व खुद जाहिर है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल कजाखस्तान में हुए एससीओ समिट में मोदी नहीं गए थे। इसलिए यह कहना निराधार है कि एससीओ बहुपक्षीय मंच है और उसके शिखर सम्मेलन में जाने को भारत- चीन संबंधों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। मोदी के चीन जाने को बेशक भारत- चीन रिश्तों के कथित रूप से सामान्य होने से जोड़ कर देखा जाएगा। मगर इस प्रक्रिया से कई सवाल जुड़े हुए हैँ।
भारत सरकार ने यह तो कभी नहीं माना कि 2020 में चीन ने भारत की किसी जमीन पर कब्जा किया, फिर भी वह कहती रही है कि जब तक डीएसक्लेशन- यानी सीमा पर सैनिकों का जमाव खत्म नहीं होता, संबंध बेहतर नहीं हो सकते। स्पष्टतः डीएसक्लेशन नहीं हुआ है और ना ही चीन की ऐसी कोई मंशा है। फिर पाकिस्तान को चीन के निरंतर समर्थन का मुद्दा है। दरअसल, मोदी की यात्रा की खबर आते ही यह कयास जोर पकड़ने लगा कि क्या भारत रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय (आरआईसी फोरम) वार्ता फिर शुरू करने पर राजी होगा? रूस इसके लिए दबाव बनाए हुए है। गौरतलब है कि जिस रोज मोदी के चीन जाने की खबर आई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल मास्को की यात्रा पर थे।
बहरहाल, आरआईसी फोरम पुनर्जीवित हुआ, तो चीन के साथ सर्वोच्च स्तर पर भारत का फिर संवाद बनेगा। जब संवाद टूटा था, तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच त्रिकोणीय शांति करार पर जोर दे रहे थे। अब उन्होंने यह प्रस्ताव फिर उठाया, तो उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी? दरअसल, ये सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं और इसलिए मामला उलझा हुआ है। पड़ोसी देशों में बेहतर संबंध हों, यह अपेक्षित है। लेकिन यह भी उतना ही अहम है कि यह किन शर्तों पर संभव है। इसलिए यह जरूरी है कि निर्णय समग्रता में और दूरदृष्टि का परिचय देते हुए लिया जाए। क्षणिक निर्णयों की भारत को पहले ही काफी कीमत चुकानी पड़ी है।