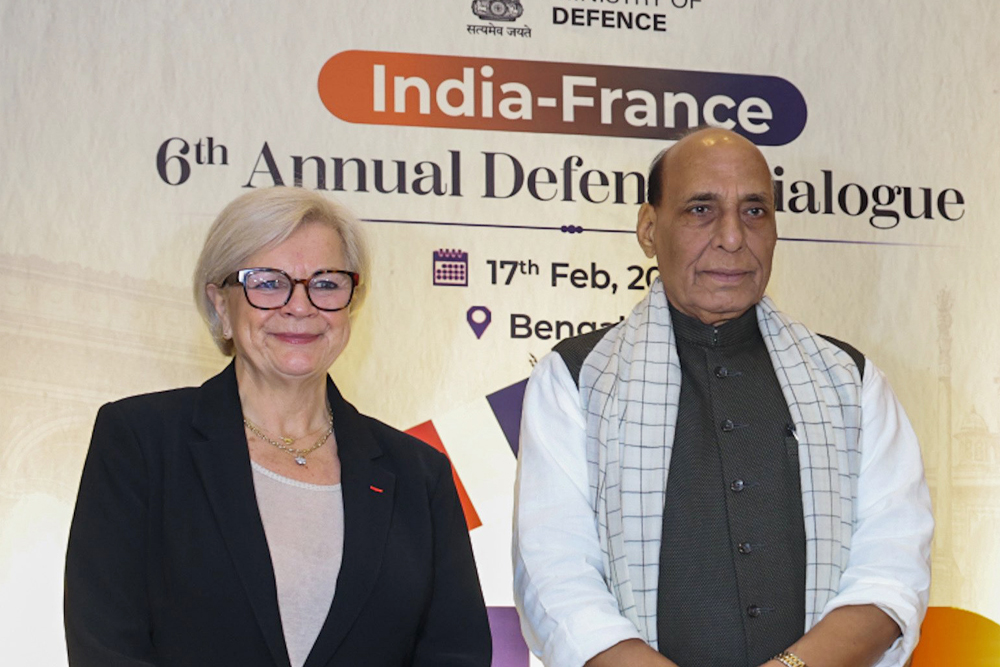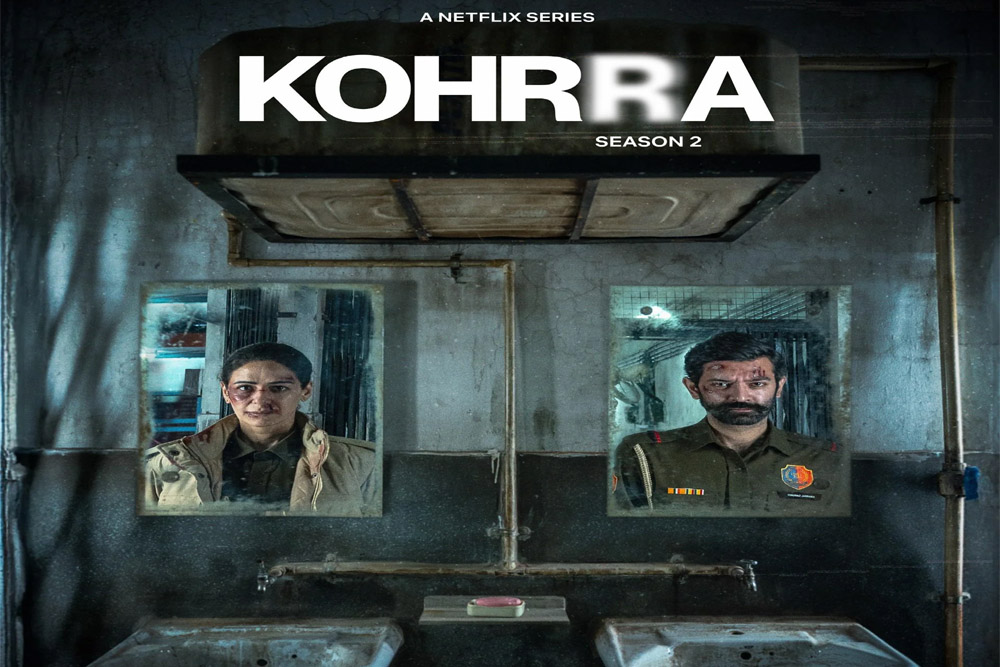लोकतंत्र भी एक अल्पतंत्रीय शासन है जो लोगों को चार या पाँच साल में एक बार, केवल यह तय करने देता है कि वह किस के हाथों बेवकूफ बनना चाहता है? इस के अलावा सारी बातें, गिनती के लोग तय करते हैं, जो स्वयं तरह-तरह की लफ्फाजी और चुनावी तिकड़मों के सिवा शायद ही अन्य योग्यताएं रखते मिलते हैं। इसीलिए जिन्हें लोक हित की सच्ची चिन्ता हो, उन्हें लोकतंत्र का नारा लगाने के बजाए, उस की कमियाँ घटाने, शासकों को उत्तरदायी बनाने, तथा योग्यता को प्रेरित करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
अभी भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता नितिन गडकरी ने कहा: ”जो लोगों को सब से अधिक मूर्ख बना सकता है, वह सब से अच्छा नेता हो सकता है।” उन्होंने बड़ी सारगर्भित बात कही। लोकतंत्र की असलियत यही है। लोक को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करना। इस प्रकार, लोकतंत्र के नेता प्रायः अलौकिक होते हैं। लोक के प्रति बेपरवाह। अपने मक्खन-मलाई की सतत सप्लाई हेतु सचेष्ट। इस में लोक की चापलूसी कर लोक को चूना लगाना मुख्य गतिविधि है।
सौ साल पहले हेनरी लुई मेंकेन की रोचक पुस्तक ‘नोट्स ऑन डेमोक्रेसी’ से अमेरिकी लोकतंत्र में वही बात मिलती है। वह कोई अपवाद भी नहीं। पश्चिमी अनुभवों से अनेक विद्वानों ने वही पाया है। हेनरी एडम की ‘डेमोक्रेसी’, एमिल फगे की ‘द कल्ट ऑफ इनकॉम्पीटेंस्’, रॉबर्ट मिचेल्स की ‘पोलिटिकल पार्टीज’, और विल ड्यूराँ की ‘प्लेजर्स ऑफ फिलॉसोफी’ से भी लोकतंत्रों की असलियत दिखती है। उन सभी बातों से नेता लोग बेहतर अवगत हैं, क्योंकि वे ही लोकतंत्र के ‘लोक’ हैं। बाकी, वही जिसे हमारे एक अन्य नेता ने ‘केटल क्लास’ कहा है। यानी, ढोर-डाँगर। जिन्हें कोई लोभ से, कोई भय से, कोई द्वेष, तो कोई दारू या सीधे नकद से हाँकता है। पर सारी गड़बड़ी का दोष जनता के माथे। एक कवि के शब्दों में: ‘शासन सुख-सुविधा में डूबा, दोष प्रजा के नाम लिखा है’।
सो, उन नेता ने ठीक ही कहा। आज सांसद, विधायक ही नहीं, पंचायत मुखिया तक के चुनाव में भी कुछ उम्मीदवार एक करोड़ रूपये तक खर्चते हैं। फिर उस की सूद समेत वसूली उन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसे रोकने के बदले सभी नेताओं ने मिलकर ऐसी भावना बनाई दी है कि इस का कुछ नहीं हो सकता। जबकि यह गलत प्रचार है। सब कुछ हो सकता है।
संसाधनों की बर्बादी रोकी जा सकती है। राजकीय पदधारियों को जबावदेह बनाया जा सकता है। सभी पदों पर केवल योग्य और निष्ठावान लाये जा सकते हैं। आखिर, संपूर्ण निजी क्षेत्र के संस्थानों, क्रियाकलाप में यह सहज ही होता है। राजकीय क्षेत्र में नहीं होता तो इसलिए, क्योंकि अलौकिक नेताओं की चिन्ता में यह शामिल ही नहीं। वे तो खुद उसी बर्बादी और गैरजवाबदेही के फल और कारक दोनों हैं। इस दुष्चक्र में लोकतंत्री व्यवस्था जैसे-तैसे चलती है। असलियत की लीपापोती कर, प्रोपेगंडा से लोगों को भ्रमित, अवश करके लूटतंत्र, धूर्ततंत्र के रूप में लोकतंत्र चल रहा है।
चूँकि यह खुल कर हो रहा है, इसलिए यह लूटतंत्र नहीं लगता। एडगर अलेन पो की कहानी ‘द परलोइन्ड लेटर’ से यह समझ सकते हैं। किसी रानी का पत्र एक मंत्री ने चुरा लिया। चोर वही है, यह मालूम है। पुलिस कैप्टन तलाशी में उस के घर जाता है। मंत्री ने सामने ही अनेक कागजों के साथ पत्र को रख दिया है। पुलिस टीम पूरा घर छान मारती है पर सोच नहीं कर पाती कि वह चीज सामने धरी है! मंत्री पकड़ा नहीं जाता।
लोकतंत्र के अलौकिक कर्णधारों की लूट वैसी ही है। हर तरह की कुव्यवस्था, बर्बादी और मनमानी पूरी न्याय प्रणाली, जाँच एजेंसियों, आदि की विस्तृत व्यवस्था, नौकरशाही सरंजाम के साथ चलती है! लोकतंत्र में लूट ऐसी खुलेआम है कि लगता ही नहीं कि यह गड़बड़ है। सीएजी की रिपोर्टों में ऐसे अनगिनत ‘परलोइन्ड लेटर’ हैं। अब कोई उस की चर्चा भी नहीं करता।
इसीलिए, लोकतंत्री नेताओं द्वारा ही दिन-रात लोकतंत्र का गीत गाना ध्यातव्य है। यह अपने आप को मक्खन लगाना है, क्योंकि लोकतंत्र के पीर-बावर्ची-भिश्ती-खर, सब वही हैं। चार या पाँच साल में एक बार, वोट देने के सिवा लोक के हाथ में किसी निर्णय का अवसर या अधिकार नहीं। जबकि नेता सदैव, हर दिन, हर स्थान पर छाए रहते हैं। हर कार्यालय में नेताओं की फोटो रहती है — न कि ‘लोक’ की। अपवाद छोड़कर सभी नेता भी लोगों पर थोपे हुए हैं। हर पार्टी के दो-चार नेता सब तय करते हैं: बड़ी से बड़ी और छोटी बात। इसे ‘जनता का शासन’ कहना जनता को ठगना है। ऐसी जनता जो कुछ नहीं कर सकती। जबकि अंततः, ‘दोष प्रजा के नाम लिखा है’ करके उसे असहाय, मायूस बनाए रखा जाता है।
सो, जब नेता लोकतंत्र का गाना गाए या रोना रोए तो यह उस के छल या अज्ञान का संकेत है। वस्तुत: वह साधारण लोगों के अहंकार की खातिर कर, उसे फु़ला या डरा कर केवल अपनी गद्दी और चमकाने, या फिर पाने का उपाय कर रहा है।
आम लोग यह सब जान कर भी लाचार देखते हैं! सारी शक्ति नेताओं के हाथ में रहती है। लेकिन वे निरंतर ‘जनता जनार्दन’ का प्रोपेगंडा चलाकर भोले लोगों, अनुभवहीन युवाओं को भरमाने में सफल रहते हैं। उन्हीं से नए लफ्फाज और अगले नेता बनाए जाते हैं।
इस प्रकार, लोकतंत्र मूलतः लोगों को बरगलाकर राज-मौज करने की प्रपंच-प्रतियोगिता है। इसीलिए प्लेटो से लेकर हाल के दार्शनिकों ने भी इसे ‘मूर्खों का शासन’ कहा है। उन की किसी बात का खंडन नहीं हो सका है। अतः लोकतंत्र को ही मानदंड मानना गलत है। आखिर, पकवान का स्वाद तो खाने में है। उदाहरण के लिए, प्रशासनिक दक्षता, ईमानदारी, जबावदेही, या न्यायिक, शैक्षिक व्यवस्था — हर क्षेत्र में गैर-लोकतांत्रिक ब्रिटिश भारत की स्थिति लोकतांत्रिक भारत से बहुत बेहतर थी। अतः लोक-कल्याण ही मानदंड हो सकता है। नेताओं की अपने-मुँह-मियाँ-मिट्ठू कोई मापदंड नहीं।
उदाहरण के लिए, सरसरी आकलन से भी ब्रिटिश राज के, या आज प्रतिष्ठित देशों की तुलना में हमारे विश्वविद्यालयों, अकादमियों की हालत बहुत गिरी है। एक्टिविज्म और प्रोपेगंडा का चलन बढ़ रहा है। अच्छे-अच्छे प्रतिभाशाली युवा राजनीतिक प्रपंचियों के हाथ पड़कर मिट्टी हो रहे हैं। शैक्षिक, अकादमिक संस्थानों को पार्टी संगठन के अड्डे बनाया जा रहा है। असुविधाजनक सचाइयों, पुस्तकों, और जानकारों से बचने का चलन बढ़ा है। यह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के विरुद्ध है। जैसा गडकरी ने ही अपने उक्त कथन में यह भी कहा था: ”हमारे कार्यक्षेत्र में अपने हृदय से सच बोलना मना है”। जब सर्वोच्च कर्णधारों की हालत ऐसी, तो शेष अनुमान सहज है।
सो, एक ओर लोकतंत्र पर गर्व, दूसरी ओर सब का मुँह बंद करना, और भिन्न विचार वाले को अपमानित करना — एक साथ चल रहा है। इसी पर इतराना, और सारा ‘दोष प्रजा के नाम’ लिखते जाना!
यह प्रवृत्ति हमें कहाँ पँहुचाएगी? इस से किसे लाभ है? ऐसे प्रश्नों पर चुप्पी भी बताती है कि लोकतंत्र अयोग्यता, मिथ्याडंबर और धूर्तता को प्रश्रय देने की व्यवस्था भी है। समाज-हितैषी लोग ऐसी मक्कारी रोकना चाहेंगे। पर नेताओं को हर जगह पार्टी-बंदी, इस के लिए दुराव, द्वेष फैलाने में वोट की फसल मिलती है। समाज को जोड़ने के बदले, अलग-अलग दलों, समूहों, समुदायों को किसी न किसी नाम पर लड़ाया जाता है। इस में ‘लोक’ की कोई चिंता नहीं है। फलत: शिक्षा, संस्कृति बिगड़ती जाती है। यही चालू लोकतंत्र है। लोक को तरह-तरह से बेवकूफ बना कर वोट खरे करने की लालसा वाली।
इसीलिए यहाँ नेताओं द्वारा ‘भारत लोकतंत्र की जननी’ कहना दोहरी गड़बड़ है। एक तो भारतीय इतिहास के गौरव में विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त, ललितादित्य, अहिल्या बाई होलकर, आदि ही आते हैं। यह सभी राजतंत्र थे। उन्हीं के राज में भारत महान रहा, न कि लोकतंत्र में। अनेक राजाओं ने लोक की सच्ची चिन्ता की थी। जबकि लोकतंत्री भारत में स्वार्थपरता, लूट-बाँट, चापलूसी को पुरस्कार, भ्रष्टाचार व मनमानी की इन्तिहा है। तुलना में ब्रिटिश राज भी प्रशासनिक सक्षमता का आदर्श, भ्रष्टाचार-मुक्त, और गुणवत्ता का आदर करने वाला था।
इसीलिए, लोकतंत्र की पाखंडी, खर्चीली, तमाशाई, बेशर्म राजनीति के तमाम उदाहरणों, अवलोकनों, और विश्लेषणों के बाद मेंकेन ने अपनी उस रोचक पुस्तक का अंत इन मार्मिक और सारगर्भित शब्दों से किया था: लोक की सच्ची चिन्ता करने वाला लोकतंत्री कैसे हो सकता है? (“हाऊ कैन एनी मैन बी ए डेमोक्रेट हू इज सिन्सियरली ए डेमोक्रेट?”)
मेंकेन ने अमेरिका की बात बताई थी। पर यहाँ भी गत अठहत्तर सालों के अखबारों में तमाम बड़े कार्टूनिस्टों, जैसे शंकर, लक्ष्मण, अबू, मारियो, काक, आदि के सतत अवलोकनों से ही असलियत सामने आ जाती है। जो उक्त सभी निष्कर्षों – मूढ़ता, धूर्तता, लूट, और अयोग्यता – की बढ़-चढ़ कर पुष्टि करती है। अतः लोकतंत्र की डींग हाँकने से अधिक उस की खामियाँ सुधारने का प्रयास ही सार्थक होता।
अन्यथा लोकतंत्र भी एक अल्पतंत्रीय शासन है जो लोगों को चार या पाँच साल में एक बार, केवल यह तय करने देता है कि वह किस के हाथों बेवकूफ बनना चाहता है? इस के अलावा सारी बातें, गिनती के लोग तय करते हैं, जो स्वयं तरह-तरह की लफ्फाजी और चुनावी तिकड़मों के सिवा शायद ही अन्य योग्यताएं रखते मिलते हैं।
इसीलिए जिन्हें लोक हित की सच्ची चिन्ता हो, उन्हें लोकतंत्र का नारा लगाने के बजाए, उस की कमियाँ घटाने, शासकों को उत्तरदायी बनाने, तथा योग्यता को प्रेरित करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ताकि पाखंडियों का स्थाई बोलबाला न रहे। यह करना संभव है।, यदि दलबंदी से ऊपर उठकर विचार हो। वरना लोकतंत्र लोगों को उल्लू बना कर — ब्रेड एंड सर्कस देकर — मूर्खों का शासन ही रहेगा।