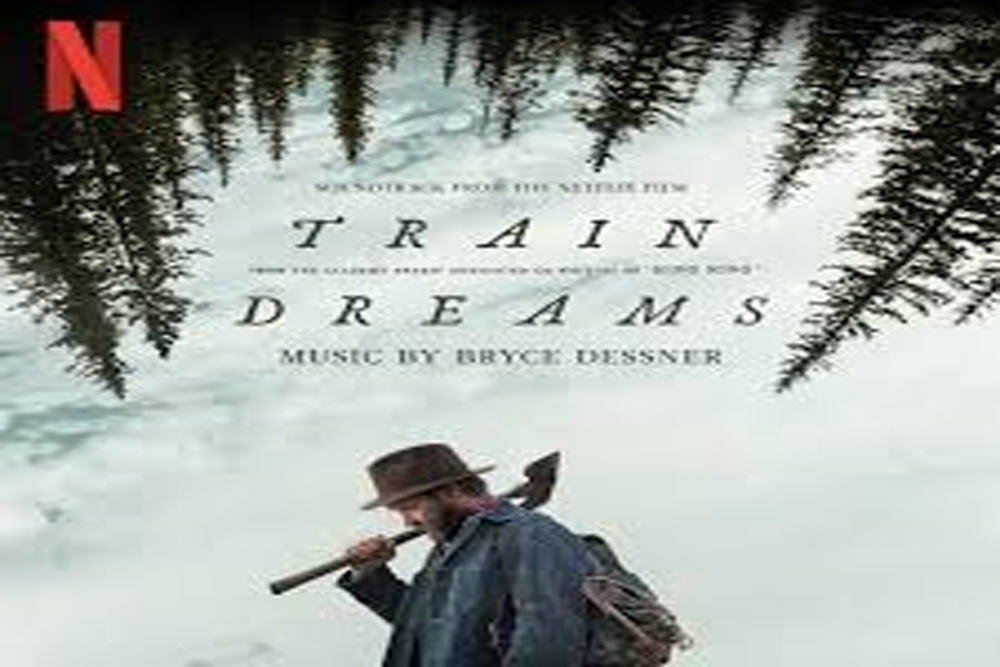क्या यह सब भारतीयों में, विशेषतः हिन्दुओं में ‘चिन्तन-फोबिया’ है — सोच-विचार से डरना? ताकि अपनी बनी-बनाई, तय की हुई विचार-प्रतिमा, नेता-प्रतिमा, मत-प्रतिमा खंडित न हो जाए? और उन प्रतिमाओं का पूजन, भजन, रंग-रोगन, झाड़-पोछ, धूपबत्ती दिखाने का नियमित अनुष्ठान बाधित, या बंद ही न करना पड़े! तब क्या होगा? फिर इतने दशकों के पाले हुए विश्वास का क्या होगा? तब क्या मानना न होगा कि वैसी असंगत बातों या झूठे निष्कर्षों में इतना समय खराब किया गया? फिर आगे क्या करने को रह जाएगा?
एक अकादमिक संस्थान में किसी ने गाँधीजी के अहिंसा और सत्य संबंधी क्रियाकलापों पर एक पर्चा पढ़ा। उस में गाँधीजी के विभिन्न विचारों को उद्धृत करके उस की विसंगतियाँ दर्शाई गई थी। साथ ही, गाँधी के राजनीतिक कैरियर से असंख्य कामों, घटनाओं, जिन में गाँधी सम्मिलित थे या सूत्रधार ही थे, की समीक्षा करके दिखाया गया था कि गाँधी या तो उन प्रसंगों में जानबूझकर असत्य कह, और अनुचित कर्म कर रहे थे, अथवा वैसे असंगत, अनुचित काम — वह भी बार-बार — करते हुए वे निरे अनजान थे। दोनों स्थितियों में, जिम्मेदार नेता या चिंतक के रूप में गाँधी की महत्ता खंडित होती है। पर्चा पढ़ने वाले ने दर्जन भर अनेक प्रसंगों के उदाहरण से अपनी सभी बातें प्रमाणिक रूप से रखी थीं। लिखित पर्चा सब को वितरित भी किया था। अर्थात, उस में रखी गई बातें यदि दुर्बल हों तो खंडित किये जाने के लिए सब के सामने प्रस्तुत थीं। वह कोई मौखिक, गोल-मोल, या केवल ओपीनियन जैसी प्रस्तुति नहीं थी।
जब पर्चा पढ़ा जा चुका तो एक शोधार्थी ने कहा कि ”पर्चे में बड़ी तर्कपूर्ण बातें हैं, जिस का मैं खंडन नहीं कर सकता। परन्तु मैं उस की किसी बात से सहमत नहीं हूँ।” वहाँ संस्थान के विद्वान प्रमुख भी मौजूद थे। उन्होंने पर्चे की प्रशंसा करते कहा, ”ऐसे ही लिखना चाहिए, प्रमाणिक रूप से, तर्क, तथ्य और संगति के साथ। चाहे मैं उस पर्चे की अनेक बातों से असहमत हूँ।” किन्तु उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया कि यदि वे बातें तथ्य-तर्क के साथ थीं, तो असहमति के बिन्दु क्या थे, और उन का निराकरण कैसे हो?
वह प्रसंग उदाहरण मात्र है। आज हर लेखक, शिक्षक, या पत्रकार को नित्य अनेक बौद्धिक सामग्री — वीडियो, वक्तव्य, बयान, लेख, टिप्पणियाँ, आदि — साझा होती रहती हैं। उन सब का आकलन करने पर कुछ बौद्धिक पैटर्न साफ झलकते हैं। वे इतने विविध स्रोतों, संस्थानों, तरह-तरह के छोटे-बड़े लोगों, आदि से आते रहते हैं कि उन का वर्गीकरण कर प्रमुख प्रवृत्तियाँ पहचान सकते हैं। वे प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं —
1-सब से बड़ी प्रवृत्ति है: आदतन राजनीतिक मानसिकता। समाज ही नहीं, साहित्य, संस्कृति, कला, और निरे समाचारों, घटनाओं, आदि को भी किसी न किसी राजनीतिक, दलीय दृष्टि से देखना।
- किसी न किसी की निन्दा करना — किसी लेखक, नेता, संस्थान, संगठन, देश, पुस्तक, आदि की। उस की बात या कार्य की किसी कसौटी पर समीक्षा करके नहीं, बल्कि पूर्व-निर्धारित जैसी निन्दा। अनोखी बात यह कि ठीक वह घटना, नीति, या वक्तव्य विचारणीय नहीं रहता जो सामने या है — अपितु वह करने, बोलने वाला (कोई नेता, देश, संस्था, या दल) ही निंदा का पात्र बनाया जाता है। मानो वह घटना या घोषणा स्वयं किसी गंभीर विमर्श का विषय नहीं! बस, वह व्यक्ति, संस्था या देश, लानत-मलामत का (या उस का प्रतिपक्षी जयकारे का) पात्र है जिस के माध्यम से वह बात आई। बस।
- उक्त बिन्दु से ही जुड़ी तीसरी प्रवृत्ति मिलती है कि किसी अनुचित स्थिति को बदलने में अपनी (यानी अपने पसंदीदा दल, नेता, संगठन, या अपने देश की भी) कोई जिम्मेदारी न समझना। किसी न किसी की भर्त्सना, कोसना और उल्टे-सीधे आरोप लगा देना, तथा उसे अमुक अनुचित स्थिति का दोषी बता देना अपने आप में संपूर्ण कर्तव्य माना लगता है। निन्दा करने वाले उस स्थिति (जैसे भारत में अंग्रेजी भाषा का बढ़ता वर्चस्व) के निराकरण के लिए किसी व्यवहारिक या वैज्ञानिक विश्लेषण, उपाय करने, उस के लिए किसी की जिम्मेदारी देखने के प्रति लापरवाह रहते हैं। मानो वह आवश्यक न हो! आग्रह करने पर, पुनः किसी न किसी (स्थिति, व्यक्ति, पार्टी, या एजेंसी) को दोष देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। जिस से इस समझ का संकेत मिलता है कि समाधान सदैव दूसरों पर निर्भर है, सो हमारा काम बस आलोचना या कोसना है। यह प्रवृत्ति स्थानीय छोटे विषयों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मामलों तक पर एक जैसी है। कहीं स्वयं, अपने संगठन, संप्रदाय, नेता, या अपने देश, सरकार, आदि का भी कर्तव्य कठघरे में नहीं मिलता। कर्तव्य दूसरों के, फतवे हमारे — यह मानो स्वयंसिद्ध जैसा लगता है। चाहे, अविचारित, बेध्यानी में ही सही।
- सुसंगतता का अभाव। जिस तरह की बात ‘क’ दल के नेता ने कही, वह निंदनीय है। किन्तु वैसी ही बात यदि ‘ख’ दल के नेता ने कही तो इसे या तो नजरअंदाज किया जाता है, या उचित ठहराया जाता है। यही दोहरापन कामों, नीतियों, घोषणाओं, गड़बड़ियों, आदि प्रसंगों में भी दिखता रहता है। अधिकांश बौद्धिक इस दोहरेपन में कोई विसंगति नहीं देखते।
- किसी न किसी की भक्ति — चाहे वह कोई नेता, लेखक, संगठन, मतवाद, निष्कर्ष, आदि या कोई पुस्तक (जैसे ‘हिन्द स्वराज’) भी। पर अधिकांशत: विचारहीन भक्ति। अर्थात्, किसी गुण, मूल्य, आदर्श, या सिद्धांत के आधार पर नहीं — बल्कि वह नेता, लेखक, संगठन, मत, निष्कर्ष, या पुस्तक ही स्वयं सर्वोपरि, सो पूज्य है। उसे किसी कसौटी, या पैमाने से परखने का सवाल ही नहीं! बल्कि पैमाने और कसौटी को ही उस नेता, लेखक, संगठन, निष्कर्ष, या पुस्तक के अनुकूल होना चाहिए। यह बाल-सुलभ मानसिकता वस्तुत: बौद्धिक चोले में निरी अंधभक्ति है! किन्तु यह आम बौद्धिकों में अत्यंत व्यापक रूप से मिलती है।
यह विचित्र, विवेकहीन भक्ति भारतीय बौद्धिकता में चौतरफा एक कैंसर की तरह फैली हुई मिलती है। उक्त प्रसंग एक उदाहरण है, जो दस अन्य नेताओं, संगठनों, मतवादों, आदि पर भी लागू दिखता है। इस मामले में सत्य, प्रमाण, शास्त्र, यहाँ तक कि राम या कृष्ण जैसे दैवी अवतारों के निर्देश या उदाहरण भी पानी भरते छोड़ दिए जाते हैं! उपनिषद, गीता ही नहीं, आज के प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ, तथा सहज नैतिकता, सहज न्याय के सीधे निष्कर्ष, आदि भी घूरे पर फेंक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह गाँधी की अपनी बनाई प्रतिमा, या अपने पसंदीदा अन्य नेता, संगठन के काम, नारे या निकम्मेपन पर आघात करते हैं। तब आम भक्त बौद्धिक उपनिषद से लेकर सामान्य विवेक और सहज न्याय तक की ऐसी व्याख्या करते हैं जो गाँधी-पूजा को यथावत रहने दे!
सो, जब सत्य, प्रमाण की धारदार कसौटियों से भक्त बौद्धिक विचलित नहीं होता, तब मामूली पर्चा पढ़ने वाला किस खेत की मूली है! उस का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया जाता है — ‘गाँधीजी पर दुनिया में सब से ज्यादा किताब लिखी गई’, या ‘स्वयं अमुक महान ने गाँधी को ऐसा अनोखा बताया था’, आदि। अथवा, इस तरह कि ‘ऐसे कितने फन्ने खाँ आए जो इतने महान व्यक्ति या संगठन को नीचा दिखाना चाहते थे, पर उस से कुछ नहीं होता’। मानो किसी प्रस्तुति को सत्य या प्रमाण से परखना ही बेकार बात है। निष्कर्ष पहले से तय है! प्रमाण या आँकड़े उस के अनुकूल हो तब तो ठीक, वरना भाड़ में जाए।
एक बुजुर्ग बुद्धिजीवी ने किसी लेखक को कहा, “आप ने गाँधी जी की ब्रह्मचर्य संबंधी बातों, कामों पर किसलिए लिखा?” वे दु:खी थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि लेखक ने कोई भी असत्य बात लिखी। वे क्षुब्ध थे कि उस विषय पर क्यों लिखा? वे भूल गये कि स्वयं गाँधी ने कहा था कि उन के हर काम का आधार ‘सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य’ है। तब उन के काम की परख करने के लिए ब्रह्मचर्य संबंधी उन के तमाम विचारों और ‘प्रयोगों’ की समीक्षा अपरिहार्य है। पर भक्त बौद्धिक इस विषय पर लिखने पर ही आपत्ति मुद्रा में आ जाते हैं!
जबकि इसी देश में भगवान बुद्ध ने कहा था कि ‘मेरी बात भी उसी तरह परख कर मानना, जैसे सोना को घिस-परख कर ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए नहीं कि मैंने कहा है।’ आज भारतीय बौद्धिक मामूली नेताओं की बातें भी बिना ना-नुच किये मानने ही नहीं, उस पर उत्साहित होने की जिद करते हैं। ऐसा न करने वाले को ब्लैकलिस्ट करते हैं।
क्या यह सब भारतीयों में, विशेषतः हिन्दुओं में ‘चिन्तन-फोबिया’ है — सोच-विचार से डरना? ताकि अपनी बनी-बनाई, तय की हुई विचार-प्रतिमा, नेता-प्रतिमा, मत-प्रतिमा खंडित न हो जाए? और उन प्रतिमाओं का पूजन, भजन, रंग-रोगन, झाड़-पोछ, धूपबत्ती दिखाने का नियमित अनुष्ठान बाधित, या बंद ही न करना पड़े! तब क्या होगा? फिर इतने दशकों के पाले हुए विश्वास का क्या होगा? तब क्या मानना न होगा कि वैसी असंगत बातों या झूठे निष्कर्षों में इतना समय खराब किया गया? फिर आगे क्या करने को रह जाएगा?
क्या यही डर अच्छे-अच्छे बौद्धिकों को वैचारिक जड़ता, सुभीता, और फिक्सेशन में बाँधे रखता है? जैसे पिंजड़े में लंबे समय से बन्द पक्षी, कभी आजाद कर दिये जाने पर भी दूर, स्वतंत्रता में उड़ जाने के बजाए, थोड़ी देर में फिर वापस आ पिंजड़े में घुस कर बैठ जाता है। उसे मालूम नहीं कि स्वतंत्रता का क्या करे!
आज भारत के अधिकांश बौद्धिक इसी अवस्था में मिलते हैं। उन में संभवतः कोई न माने कि वे किसी बौद्धिक या मतवादी पिंजड़े में स्वेच्छा से बंद पक्षी जैसे हैं। स्वतंत्र सोच विचार से भागने वाले — अर्थात प्रमाण से; सत्य, विवेक की कसौटी से; नीर-क्षीर कर देखने की चुनौती से, सहज न्याय की मानवीय दृष्टि से; यहाँ तक कि उतने ही भारी अन्य महापुरुषों के भी प्रतिकूल विचारों से — जैसे, गाँधी के संबंध में श्रीअरविन्द, टैगोर, डॉ. अंबेडकर, राजगोपालाचारी, राम मनोहर लोहिया, आदि के विचारों से। जिन महापुरुषों ने गाँधी के क्रियाकलापों और उन के परिणाम का प्रत्यक्ष और लंबे समय तक अवलोकन किया था। पर भक्त कहेगा: ‘असहमत’।
सो, तमाम तथ्य, विवेक, गवाही, आदि दरकिनार कर प्रायः हर तरह के बौद्धिक किसी प्रकार की भक्ति या दुराव में सराबोर, अपनी बनाई ऊँचाई से इस-उस को दूषते, कोसते, हीन समझते अपनी पसंद के फतवों, उदाहरणों, उद्धरणों, श्लोकों, मुहावरों, व्यंग्योक्तियों से भिन्न विचारों (बल्कि भिन्न विचार रखने वाले) को ध्वस्त कर, यानी ध्वस्त हुआ समझ कर, स्वयंतुष्ट रहते हैं। वे खुद ही फरियादी, वकील, और जज तीनों बनकर मामले को अपने पक्ष में स्वयंसिद्ध समझते हैं।
यह एक दो बौद्धिकों की बात नहीं! असंख्य लोग — जिन में क्षमता और रुचि भी है — ऐसा ही करते मिलते हैं। वैसा करते उन के बरस के बरस बीतते जाते हैं। पर उन की अर्जित जानकारी, निष्कर्ष, आदि का किसी कसौटी से परखना नहीं होता। वे अपनी भक्ति सर्वोपरि समझते हैं। सारी बुद्धि उस की पुष्टि में किताब, उद्धरण, दलील, हमराही, या अनुशंसा ढूँढने में लगाते हैं। प्रतिकूल पड़ने वाली हर चीज या लेखक को व्यंग्य या कुतर्क से ध्वस्त करने, या ध्वस्त मान लेने में संतोष महसूसते हैं। यही आज भारत की आम बौद्धिकता है। उस के रूप गाँधीवादी, नेहरूपंथी, वामपंथी, लोहियावादी, या संघी हो सकते हैं। परन्तु उपर्युक्त पाँचों प्रवृत्तियाँ सब में कमोबेश मिलती हैं। बौद्धिकता के नाम पर जड़ भक्ति, और चिंतन-फोबिया।