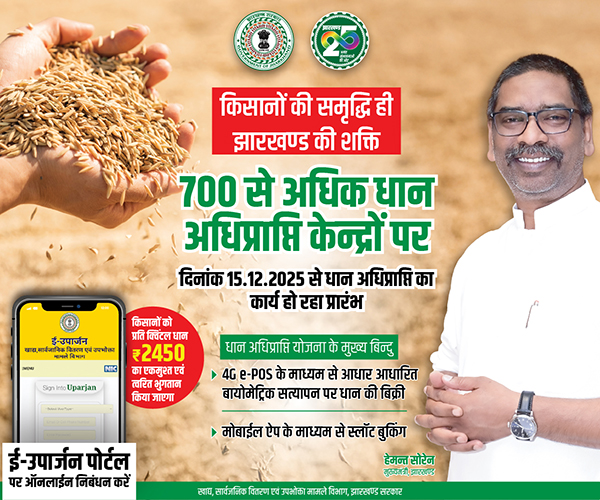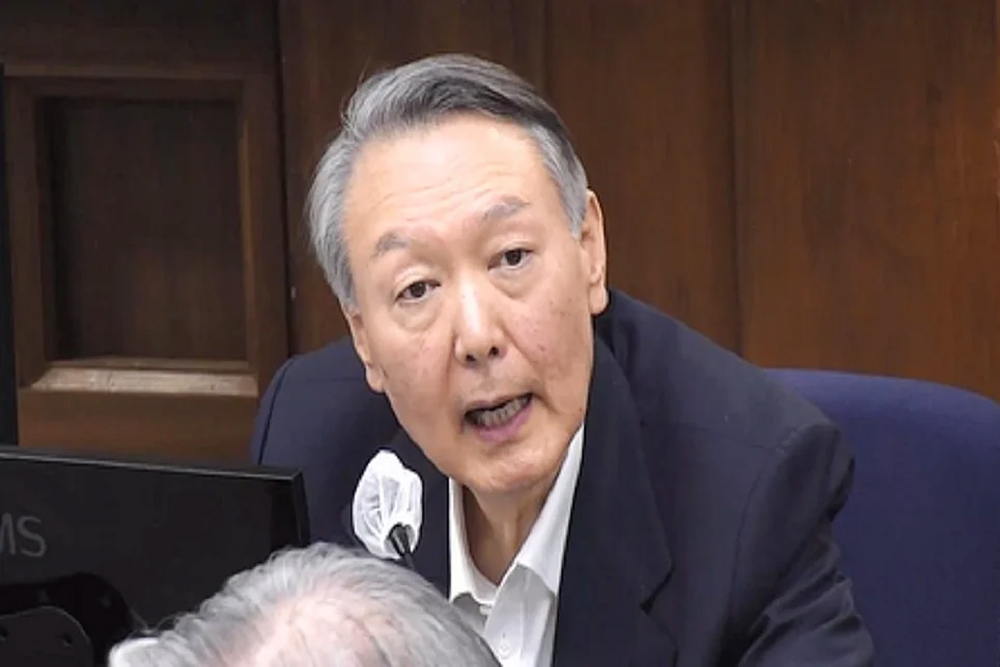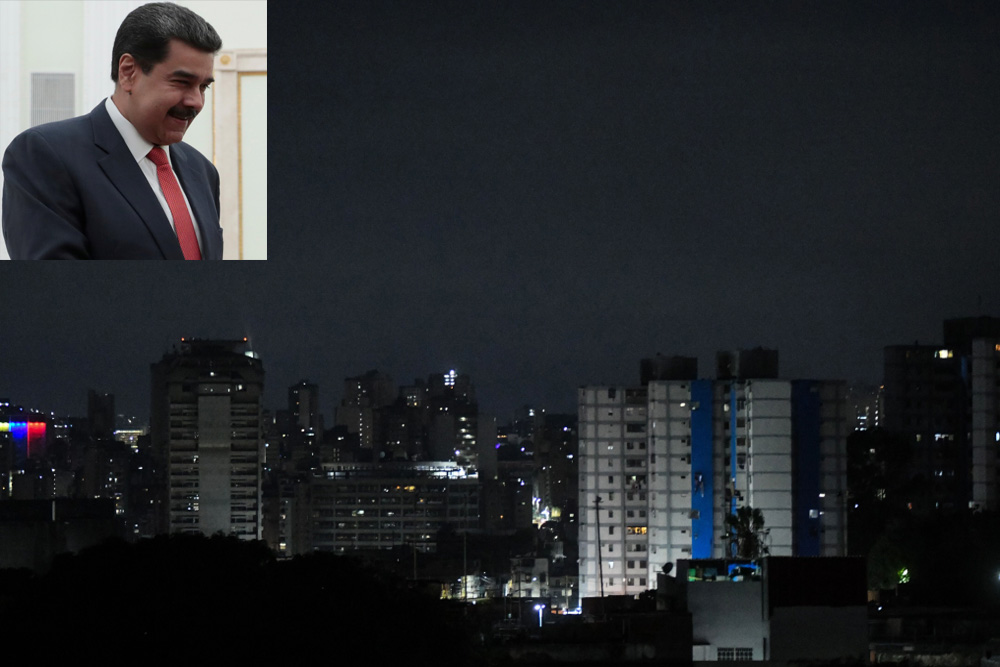तब जो समस्याएं थीं वे आज भी हैं। वही गरीबी, वही बेरोज़गारी, वही भ्रष्टाचार, वही महंगाई और वही सामाजिक व आर्थिक असमानताएं। बल्कि वोटरों की वही बेचारगी भी। इसलिए इमरजेंसी के पचास साल बाद भी मिंटो रोड पर मिले उन बुजुर्ग सज्जन की आवाज मुझे याद है। उन्होंने कहा था – ‘कुछ नहीं बदलता।‘ आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर, मैं मान गया, सचमुच कुछ नहीं बदलता
हर तरफ़ अब इमरजेंसी की कहानियां थीं। आज़ादी के बाद ऐसी कहानियां देश पहली बार सुन रहा था। कितने लोग पकड़े गए। किस नेता को कहां से पकड़ा गया। और कौन अभी तक पकड़ा नहीं गया। प्रेस को दबाने की कोशिश तो खैर कमाल थी। देश ने पहली बार अखबारों के पन्ने काले या कोरे छपते देखे।
जहां देखो, इंदिरा गांधी के बीस सूत्री और संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रमों के बड़े-बड़े होर्डिंग लगे थे। कुछ लोग कहते थे कि सब जगह तमीज़ से लाइनें लग रही हैं और सरकारी कर्मचारी समय पर दफ़्तर पहुंच रहे हैं। वे कहते, यह अनुशासन तो होना ही चाहिए। आज भी बहुत से लोग इमरजेंसी को इसके लिए याद करते हैं। यानी बसों, ट्रेनों, अस्पतालों आदि में लोग लाइन नहीं तोड़ें और कर्मचारी समय पर दफ़्तर पहुंचें, इसके लिए वे इमरजेंसी को जायज़ ठहराते हैं।
हमारे एक अग्रज धनंजय उन दिनों शाहदरा के गोरख पार्क इलाके में रहते थे। उनके घर दोस्तों का जमावड़ा लगा रहता था। हम कई-कई दिन उनके यहां जमे रहते। एक रात जब उनके यहां चाय बनाने का सामान खत्म हो गया तो हम छह-सात लोग चाय पीने के लिए बाहर निकले। लेकिन समय ज्यादा हो गया था और दुकानें बंद हो चुकी थीं। तय हुआ कि शाहदरा स्टेशन चला जाए। वहां तो कोई चाय की दुकान मिल ही जाएगी। मगर स्टेशन पर भी सन्नाटा था। हार कर हम लौट लिए।
बाबरपुर रोड पर अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि हमें पुलिसवालों की एक बड़ी टीम ने रोक लिया। एक ने पूछा, ‘कहां से आ रहे हो इतनी रात को, इतने लोग एक साथ?‘ हमने कहा- ‘चाय ढूंढ़ने निकले थे, पर कोई दुकान नहीं मिली।’ उसने सवाल किया- ‘रात के एक बजे चाय पीने निकले?’ हममें से किसी की समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। सब चुप रहे।
उन पुलिसवालों का जो बॉस था, वह बारी-बारी हममें से हर किसी के पास गया। किसी के बाल खींचे, किसी के कान उमेठे, किसी की बांह मरोड़ी और मेरे दाएं हाथ की उंगलियां बिलकुल पीछे घुमा दीं। लगा कि टूट ही जाएंगी। हम सब दहशत में आ गए। उसने सबसे पूछा, क्या करते हो। उस दिन हमारी टोली में जो लोग थे उनमें ज्यादातर कुछ नहीं करते थे। केवल एक सोम प्रकाश थे जिन्हें कुछ ही दिन पहले दनकौर के पास एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई थी।
जैसे ही उस पुलिसवाले ने सुना कि सोम प्रकाश पढ़ाते हैं तो वह बोला- ‘अब समझ में आया। ये मास्टर है और तुम सब इसके चेले हो। और ये कोई वारदात करवाने के लिए तुम्हें लेकर इतनी रात को बाहर निकला है।‘ यह सुन कर हम लोगों की हालत और ख़राब हो गई। पुलिसवाले पास खड़ी अपनी जीप में हमें बिठाने की तैयारी कर ही रहे थे कि सोम प्रकाश हिम्मत जुटा कर उनके बॉस के पास गए और बोले – ‘देखिए, आप अधिकारी हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन यह सच है कि हम लोग केवल चाय के लालच में स्टेशन तक गए थे।’ वह पुलिसवाला कुछ देर सोम प्रकाश को घूरता रहा और फिर शायद हम लोगों पर छाई दहशत से उसे तरस आ गया। उसने हमसे गोरख पार्क का पूरा पता पूछा, जो कि एक पुलिसवाले ने नोट भी किया, और फिर कई गालियां देते हुए कहा- ‘जाओ, सीधे घर जाओ। कहीं मुड़ना नहीं। मैं तुम्हारे पीछे आदमी भेज रहा हूं।‘ फिर एक पॉज़ के बाद बोला- ‘याद रखना, पकड़े गए तो छूट नहीं पाओगे।’
ऐसा बिलकुल नहीं है कि हमारी पुलिस इस घटना से पहले रात में लोगों को रोक कर ऐसा नहीं करती रही होगी या आज ऐसा नहीं करेगी। मगर इस घटना में इमरजेंसी का अहसास शामिल था। इस अहसास से यह मेरा पहला साबका था। इसके बाद हम गोरख पार्क वाले घर से इतनी रात को फिर कभी बाहर नहीं निकले।
हमारी उस टोली में से सोम प्रकाश अब नहीं रहे। अध्यापक के अलावा वे कहानीकार भी थे। उनका लेखकीय नाम सोमेश्वर था। उनके घर गाजियाबाद भी मैं जाता रहता था। खास कर रविवार को। सोमवार को वे काम पर जाते और मैं वापस अपने घर। उनके पास जाने के लिए पहले मैं बस से पुरानी दिल्ली स्टेशन जाता और वहां से ट्रेन पकड़ता था। कई शटल ट्रेनें थीं जो बहुत कम पैसे में गाजियाबाद पहुंचा देती थीं।
सर्दियों के दिन थे। चार नंबर प्लेटफार्म पर शटल खड़ी देख मैं फटाफट चढ़ गया। उस दिन मेरे हाथ में कई किताबें थीं जो मुझे सोम प्रकाश को वापस करनी थीं। उनमें एक महात्मा गांधी से संबंधित किताब थी और तो आल्बेयर कामू के ‘आउटसाइडर’ का हिंदी अनुवाद ‘अजनबी’ भी थी। किताबें बगल में रख मैं खिड़की से बाहर प्लेटफार्म की गतिविधियां देखने लगा। थोड़ी देर में ट्रेन चली। उसके चलते ही वहां दो लोग प्रकट हुए। एक मेरे सामने बैठ गया और दूसरा मेरे पड़ोस में। बगैर पूछे उन्होंने मेरी किताबें उठा लीं और उन्हें आपस में बांट कर उलटने-पलटने लगे। फिर सामने बैठे व्यक्ति ने अधिकार पूर्वक पूछा- ‘आप कहां जा रहे हैं?’
मैंने बताया- ‘गाजियाबाद।’
उसने आगे पूछा- ‘गाजियाबाद में कहां?’
मैंने कहा- ‘वहां आर्यनगर में मेरे एक मित्र रहते हैं। उनसे मिलने जाना है।‘
वह बोला- ‘उनका पूरा ऐड्रेस बताइए।‘
मैंने कहा- ‘लेकिन एड्रेस का आप क्या करेंगे?‘
सामने बैठा व्यक्ति बोला- ‘जो हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, बगैर कुछ छिपाए।‘
मैंने गौर किया कि हम तीनों के अलावा आसपास कोई नहीं था और वे दोनों इस तरह मुझे घेर कर बैठे थे कि मैं चाहूं भी तो भाग न सकूं। मैंने सोम प्रकाश का मकान नंबर बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आपका यह मित्र क्या करता है, खुद आप क्या करते हैं, आप कब-कब उसके पास जाते हैं, आपके और कौन-कौन मित्र हैं और क्या वे भी सोम प्रकाश को जानते हैं। जो व्यक्ति मेरे पड़ोस में बैठा था उसने तो यहां तक पूछा कि जब आपके सारे मित्र कहीं जुटते हैं तो उनका क्या प्रोग्राम रहता है।
तब मैं उन्नीस साल का था। मेरे जवाबों में आवारागर्दी के अलावा उन्हें शायद कोई और गड़बड़ी नहीं दिखी। इसलिए आख़िरकार उन्होंने मेरी किताबें वहीं रख दीं और उठ खड़े हुए। फिर साहिबाबाद स्टेशन पर उतर गए। उनके जाने के बाद मैंने पूरे डिब्बे में चक्कर लगाया। रविवार का दिन था, इसलिए ट्रेन खाली पड़ी थी। पीछे की सीटों पर अलग-अलग सिर्फ तीन-चार लोग बैठे दिखे। उन्हें गुमान तक नहीं था कि अभी-अभी मेरे साथ वहां क्या गुज़रा है। गाजियाबाद आने पर मैं पैदल ही सोम प्रकाश के घर पहुंचा और उन्हें छत पर ले जाकर सारी घटना सुनाई। इमरजेंसी से यह मेरी दूसरी मुलाकात थी।
आखिरकार मार्च 1977 आया और चुनाव हुए। फिर वह दिन आया जब सोम प्रकाश के साथ लगभग पूरी रात जागते हुए ट्रांजिस्टर के सिरहाने बैठ इंदिरा गांधी के चुनाव हारने की ख़बर का इंतज़ार किया। अगले दिन हम दिल्ली आए। कनॉट प्लेस में जनता पार्टी के झंडे लगाए कुछ एम्बैसडर कारें और ऑटो रिक्शा चक्कर लगा रहे थे। उन पर लगे लाउडस्पीकर चीख रहे थे – ‘धन्यवाद, धन्यवाद, जनता पार्टी पर भरोसा जताने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए धन्यवाद।’ एक अख़बार में छपा वह फोटो तब खासा पसंद किया गया था जिसमें एक सफाई कर्मचारी इंदिरा गांधी की तस्वीर वाला पोस्टर बाकी कचरे के साथ कूड़ा ले जाने वाली अपनी हाथगाड़ी में डाल रहा था।
मगर जैसा कि अक्सर होता है, धीरे-धीरे नई सरकार की सीमाएं उजागर होने लगीं। शायद सरकारें जनता की तरह सोच ही नहीं सकतीं। प्रधानमंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार दस साल में सबको रोज़गार उपलब्ध करा देगी। अगले ही दिन दिल्ली में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के पोस्टरों पर लिखा दिखा- ‘कृपया दस साल जिंदा रहिए।‘
कुछ ही महीनों में मोरारजी के बेटे कांति देसाई, उनकी पार्टी और सरकार की भीतरी खटपट और दोहरी सदस्यता यानी तरह-तरह की ऐसी ख़बरें आने लगीं जिनकी जेपी आंदोलन के समर्थक कल्पना नहीं कर सकते थे। जनता पार्टी में विलीन हुई पार्टियों के सिद्धांत और उनके नेताओं के अहम और हसरतें आपस में टकरा रही थीं। ऐसी ही कुछ हसरतों का काफ़िला एक रात पूसा रोड की 46 नंबर कोठी पर पहुंचा। मोहन मीकिंस वाले कपिल मोहन की इस कोठी पर संजय गांधी और राजनारायण मिले और एक डील करके अपने-अपने रास्ते चले गए। सरकार गिरी और अब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने जिन्हें कांग्रेस ने तिगनी का नाच नचाया। अंतत: इंदिरा गांधी फिर सत्ता में लौटीं।
आज वह सब एक मजाक सा लगता है। जेपी आंदोलन में शामिल रहे लोग आज क्या कर रहे हैं, इस पर निगाह दौड़ाएं तो इस मज़ाक की क्रूरता और बढ़ जाती है। लेकिन उनमें हर किसी के पास खुद को सही ठहराने के तर्क मौजूद हैं। इन तर्कों से वे कोई जीत नहीं जाते, पर जनता को ज़रूर हरा देते हैं। जेपी आंदोलन को आज़ादी की दूसरी लड़ाई कहा गया था। इसलिए जब अन्ना हजारे के आंदोलन को कुछ लोगों ने आज़ादी की दूसरी लड़ाई बताया तो मुझे हास्यास्पद लगा। दूसरी तो हो चुकी थी। उन्हें तो इसे आज़ादी की तीसरी लड़ाई कहना चाहिए था। मगर सवाल यह है कि हमें आज़ादी की कितनी लड़ाइयां चाहिए?
व्यंग्यकार शरद जोशी ने एक जगह लिखा था कि हमारे राजनीतिकों ने दोनों ऐसे मौके गंवा दिए जब देश किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार था। पहला मौका 1947 का था और दूसरा उसके तीस साल बाद 1977 में मिला था। मगर मुझे लगता है कि जब भी सरकार बदलती है तो हर बार लोग किसी वड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं और फिर हाथ मलते हैं। इसीलिए तब जो समस्याएं थीं वे आज भी हैं। वही गरीबी, वही बेरोज़गारी, वही भ्रष्टाचार, वही महंगाई और वही सामाजिक व आर्थिक असमानताएं। बल्कि वोटरों की वही बेचारगी भी। इसलिए इमरजेंसी के पचास साल बाद भी मिंटो रोड पर मिले उन बुजुर्ग सज्जन की आवाज मुझे याद है। उन्होंने कहा था – ‘कुछ नहीं बदलता।‘ आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर, मैं मान गया, सचमुच कुछ नहीं बदलता। (ख़त्म)