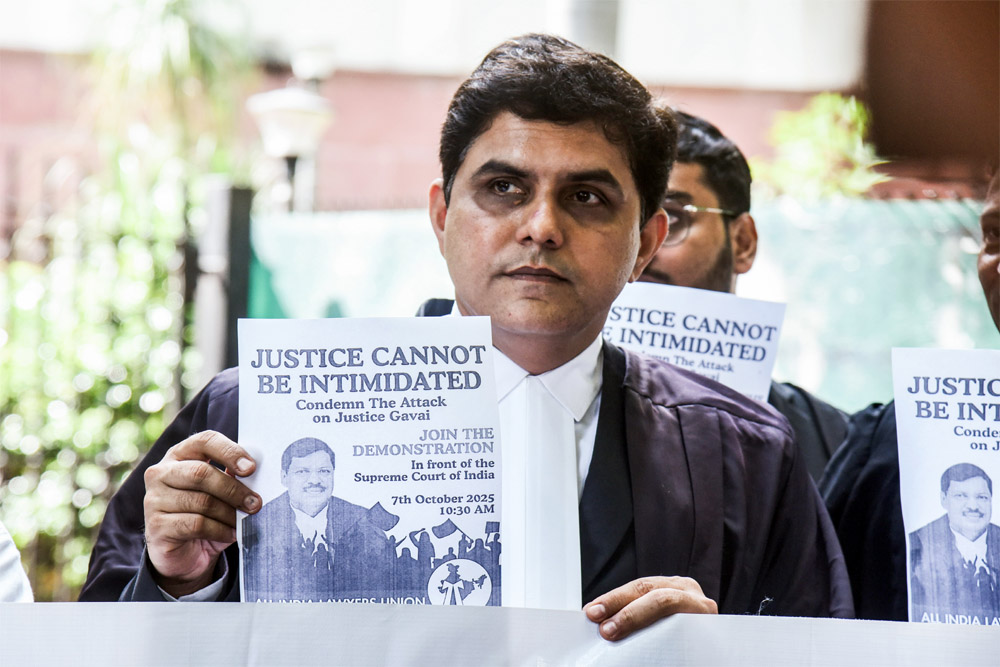आज यह क्षेत्र गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। सस्ते आयात, पावरलूम की नकली डिज़ाइन, प्राकृतिक रेशे की बढ़ती कीमत और सरकारी संरक्षण में कमी ने बुनकरों की स्थिति कमजोर कर दी है। कई लोग यह पेशा छोड़कर अन्य कामों में लग गए हैं। जो बचे हैं, वे भी उचित मूल्य और बाजार न मिलने से संघर्ष कर रहे हैं।
7 अगस्त –राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस
भारत में हथकरघा की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता की स्मृतियां। सूत, रेशम, ऊन या जूट — किसी भी रेशे से कपड़ा बुनने का हुनर यहां के कारीगरों ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी सँभाला है। लकड़ी के बने करघों पर बुनाई करना कभी सिर्फ रोजगार का साधन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक अभ्यास था, जिसमें घर के हर सदस्य की भूमिका होती थी। महिलाएं सूत काततीं, रंगाई करतीं, पुरुष करघे पर बुनाई करते, और बच्चे इस पूरी प्रक्रिया में छोटे-बड़े कामों में हाथ बंटाते। यह पेशा आत्मनिर्भर था — कपास या ऊन खेतों और पशुपालकों से आता, उसे साफ करके सूत बनाया जाता, फिर रंगाई और बुनाई होती।
प्राचीन भारतीय साहित्य में बुनाई और वस्त्र-निर्माण का उल्लेख कई जगह मिलता है। ऋग्वेद, पुराण और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में वस्त्र कला की महिमा का वर्णन है। वैदिक युग में बुनकरों को तंतुवाय कहा जाता था, और वे प्राकृतिक रंगों से कपड़ों को सजाते थे। हथकरघा शब्द भले उस समय प्रचलित न रहा हो, पर ऊन, रेशम और सूती वस्त्र निर्माण का कौशल उस समय उच्च स्तर पर था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाइयों में मिली तकलियां, रंगाई के बर्तन और बुने हुए कपड़ों के टुकड़े बताते हैं कि वस्त्र निर्माण वहां की जिंदगी का हिस्सा था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले सूती धागे और रंगाई के उपकरण इस बात के साक्षी हैं कि कपड़ा बनाना उस समय भी केवल ज़रूरत नहीं, बल्कि विकसित कला थी।
कालक्रम में इस कला ने नए आयाम पाए। मौर्य और गुप्त काल में मलमल और रेशम की बुनाई ने भारत को विश्व में विशिष्ट पहचान दी। मुगल काल में हथकरघा और निखरा, जब बनारसी ब्रोकेड, जामदानी और पश्मीना जैसे डिज़ाइन लोकप्रिय हुए। सोने-चांदी के तार, मोर और कमल के रूपांकन, खगोलीय आकृतियां और जटिल ज्यामितीय पैटर्न बुनाई में आम हो गए। इन वस्त्रों की महीनता, पारदर्शिता और कलात्मकता इतनी अद्वितीय थी कि इन्हें देखने और पहनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे।
लेकिन औपनिवेशिक दौर में हथकरघा को गहरी चोट पहुंची। ब्रिटिश शासन ने भारतीय कपड़ों पर भारी कर लगाए और मशीन से बने कपड़ों के आयात को बढ़ावा दिया। भारत कच्चे कपास का निर्यातक और मशीनी सूत का आयातक बन गया। जब बुनकरों को सूत खरीदना पड़ने लगा तो वे सूत व्यापारियों और बिचौलियों पर निर्भर हो गए। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता खत्म हुई और वे ठेके पर काम करने को मजबूर हो गए। मशीन-निर्मित कपड़ों की बाढ़ और पावरलूम के आगमन ने पारंपरिक बुनकरों को असमान प्रतिस्पर्धा में धकेल दिया।
बीसवीं सदी के आरंभ में स्वदेशी आंदोलन ने हथकरघा को आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। गांधीजी ने चरखे को आंदोलन का प्रतीक बनाया और खादी को आत्मनिर्भरता व स्वाभिमान का वस्त्र बना दिया। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए और हाथ से काता-बुना कपड़ा पहनना शुरू किया। इसने न सिर्फ बुनकरों को काम दिया, बल्कि ब्रिटिश कपड़ा उद्योग को भी चोट पहुंचाई। उस दौर में खादी केवल कपड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिरोध का ध्वज बन गई थी।
भारत के अलग-अलग हिस्सों में हथकरघा की अपनी-अपनी पहचान रही है। मध्य प्रदेश का चंदेरी प्राचीन काल से ही बुनाई का केंद्र रहा, जहां ‘बुना हुआ हवा’ कहलाने वाली महीन और पारदर्शी साड़ियां बनती थीं। इन पर सोने-चांदी की कढ़ाई, मोर, कमल और ज्यामितीय डिज़ाइन होते थे। माहेश्वर की माहेश्वरी साड़ियों की शुरुआत रानी अहिल्या बाई होल्कर ने की थी, जो पहले राजघरानों के लिए बनाई जाती थीं, फिर धीरे-धीरे आम लोगों में लोकप्रिय हुईं। बनारसी रेशमी ब्रोकेड, तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत, मछलीपटनम की छींट, आगरा और बरेली की दरियां, अमरोहा और देवबंद की खादी — हर क्षेत्र ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की, जो आज भी पहचानी जाती है।
2011 की जनगणना के अनुसार हथकरघा उद्योग ने करीब 43 लाख लोगों को सीधा रोजगार दिया। यह कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा श्रम-प्रधान क्षेत्र है और कुल कपड़ा उत्पादन में लगभग 22 प्रतिशत योगदान देता है। भारत दुनिया में हाथ से बुने कपड़ों का आधे से ज्यादा उत्पादन करता है और इनका निर्यात भी होता है। इन कपड़ों की खासियत है कि वे केवल सजावटी नहीं, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
फिर भी, आज यह क्षेत्र गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। सस्ते आयात, पावरलूम की नकली डिज़ाइन, प्राकृतिक रेशे की बढ़ती कीमत और सरकारी संरक्षण में कमी ने बुनकरों की स्थिति कमजोर कर दी है। कई लोग यह पेशा छोड़कर अन्य कामों में लग गए हैं। जो बचे हैं, वे भी उचित मूल्य और बाजार न मिलने से संघर्ष कर रहे हैं।
जरूरत है कि हथकरघा को नया बाजार, बेहतर तकनीक और आधुनिक डिजाइन मिले। ऑनलाइन प्लेटफार्म और वैश्विक फैशन बाजार से इसे जोड़ा जाए, ताकि युवा पीढ़ी भी इसे अपनाने को प्रेरित हो। प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मजबूत विपणन तंत्र के बिना यह परंपरा धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है।
इसी सोच से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है — 1905 के स्वदेशी आंदोलन के आरंभ की स्मृति में। इसका उद्देश्य बुनकरों का सम्मान करना और इस कला के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हथकरघा सिर्फ कपड़ा बनाने की प्रक्रिया नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा है। इसे बचाना केवल परंपरा को बचाना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गर्व को जीवित रखना है।
अगर इस क्षेत्र को सही समर्थन मिला, तो हथकरघा न केवल अपने गौरवशाली अतीत को संभाले रखेगा, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था और भारतीय पहचान का भी मजबूत आधार बनेगा। यह केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवित विरासत है, जिसे हमें संजोना और आगे बढ़ाना है।