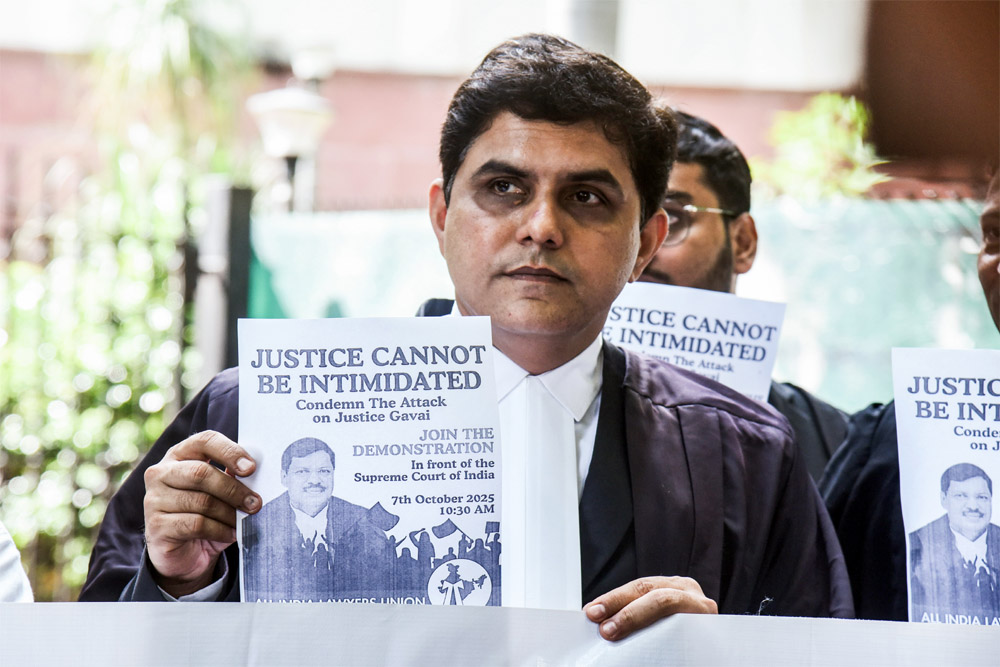आयुर्वेद की दृष्टि से नवरात्र के नौ दिन कायाकल्प की अवधि होती है। आयुर्वेद के अनुसार नवरात्र में कायाकल्प नियम का पालन किए जाने से शरीर में बीमारियों के बचाव के लिए शक्ति का संचार होता है, इम्युनिटी बढ़ती है। नवरात्र के पहले तीन दिन धीरे -धीरे आहार कम करने अथवा फलाहार लेने, चौथे दिन से निराहार रहने, फिर फलाहार और धीरे- धीरे पूर्ण आहार की ओर बढ़ने का नियम है।
भारतीय नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि तदनुसार 30 मार्च 2025 से आरंभ हो चुकी है। इसी तिथि से नवसंवत्सर का आरंभ हो चुका है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से ही सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रवर्तित विक्रम संवत 2082 का और द्वापर युग में युधिष्ठिर द्वारा आरंभ की गई युगाब्द संवत 5127 का आरंभ हो चुका है। इस वर्ष संवत्सर का नाम कालयुक्त है। भारतीय परंपरा में प्रत्येक वर्ष का कोई न कोई ग्रह राजा होता है और कोई ग्रह मंत्री। इस वर्ष के राजा सूर्य होंगे।
मंत्री का दायित्व भी सूर्यदेव स्वयं संभालेंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा अर्थात गुड़ी पड़वा सृष्टि के विकास आरंभ का दिन माना जाता है। सृष्टि के सृजन की तिथि शिवरात्रि मानी जाती है। लेकिन समय और सृष्टि की विकास प्रक्रिया चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होना मानी जाती है। भारत में इस दिन की विशेष महत्व है।
महाभारत काल में सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्याभिषेक के लिए इसी तिथि का चयन किया था। इसी तिथि को सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। इसी तिथि से युधिष्ठिर के युगाब्द संवत और सम्राट विक्रमादित्य के विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। इसी तिथि से चैत्र नवरात्र आरंभ होते हैं। यह बसंत और ग्रीष्म ऋतु के संगम की अवधि है। ऋतु संगम सदैव मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और अस्वस्थ होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है।
इसी समय मौसमी बीमारी होती हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से नवरात्र के नौ दिन कायाकल्प की अवधि होती है। आयुर्वेद के अनुसार नवरात्र में कायाकल्प नियम का पालन किए जाने से शरीर में बीमारियों के बचाव के लिए शक्ति का संचार होता है, इम्युनिटी बढ़ती है। नवरात्र के पहले तीन दिन धीरे -धीरे आहार कम करने अथवा फलाहार लेने, चौथे दिन से निराहार रहने, फिर फलाहार और धीरे- धीरे पूर्ण आहार की ओर बढ़ने का नियम है।
चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नौ दिन तक किए गए इस नियम से अद्भुत आरोग्य क्षमता उत्पन्न होती है। भौगोलिक और भूगर्भीय दृष्टि से नवरात्र का बड़ा महत्व है। पृथ्वी पर विषव की विशिष्ट स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसलिए नवरात्र पर्व में व्रत, उपवास और ध्यान के माध्यम से चक्रों और नाड़ियों का शोधन होता है।
जीव विज्ञान के अनुसार इसी समय हार्मोनल, और आंतरिक परिवर्तन के साथ जैविक चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण कई प्रकार के रोग की बाढ़ आ जाती है, जिसके शोधन के लिए दिव्य ब्रह्माण्डकीय आदिशक्ति भगवती दुर्गा के नौ रुपों को शिरोधार्य किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि दुर्गा शब्द की व्युत्पत्ति दुर्ग और आ प्रत्यय जोड़कर हुई है, जिसका अर्थ है- जो शक्ति दुर्ग की रक्षा करती हैं, दुर्गा हैं। यहां दुर्ग का अर्थ साधक के शरीर और चेतना के लिए ही है। दुर्ग की रक्षा करने वाली शक्ति दुर्गा है। दुर्ग साधक का शरीर है, और उसकी चेतना है दुर्गा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव शरीर में आसुरी प्रवृत्ति के नाश के लिए ही नवरात्र पर्व मनाने की महान परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से भारत में प्रवहमान है।
इस परंपरा में शक्ति माता दुर्गा का आह्वान कर मानव शरीर में उत्पन्न आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश किया जाता है। शक्ति के संतुलन के लिए ही नवरात्र पर्व की परंपरा स्थापित की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में पौराणिक ग्रंथों में आसुरी प्रवृत्तियों के नामकरण किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में षड्यंत्रपूर्वक इनका मानवीकरण कर स्वार्थी तत्वों द्वारा लोगों को भ्रमित कर गलत मत स्थापित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। ध्यातव्य यह भी है कि असुर का शाब्दिक अर्थ है- अ अर्थात बिना +सुर। अर्थात हमारी चेतना का ताल अथवा सुर का बिगड़ना। यही मानव में निहित असुर है, असुरत्व है।
यही आसुरी प्रवृत्ति है। महिषासुर शब्द में महिष मह शब्द से बना है, जिसका अर्थ महान होता है। और असुर प्रवृत्ति है। जिसका अर्थ है- व्यक्ति और समाज से जड़ता समाप्त करना। प्रगट रुप में महिषासुर समाज में जड़ता की निशानी है और उसके शोधन के लिए नवरात्र में व्रत रखा जाता है। जगदंबा द्वारा धूम्रलोचन का वध करने का पर्याय व्यक्ति और समाज में धुंधली दृष्टि को समाप्त करके करके दिव्य दृष्टि प्रदान करना है। रक्तबीज का आशय शरीर में उपस्थित रक्त और बीज से है, जिसमें अशुद्धि आ जाती है, तथा समाज में मनोग्रथियां उत्पन्न हो जाती हैं।
इसलिए उसे शुद्ध करने के लिए रक्तबीज का शोधन किया जाता है। चंड का अर्थ – चिंता और मुंड का अर्थ- अहंकार अथवा अज्ञानता से है। इन आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करके नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की ओर जाना ही नवरात्र पर्व का मूलाधार है। भगवती दुर्गा आदिशक्ति ही सृष्टि की संचालिका हैं और इसी से सारी शक्ति नि:सृत होती है और ब्रह्मांड का संचालन होता है।
Also Read: ऐसा लगा जैसे पंजाब अपना क्यूरेटर लेकर आई थी: जहीर खान
नवरात्र: शक्ति, साधना और विज्ञान का संगम
नवरात्र आराधना काल में ॐ ऐं ह्रीं क्लीं मंत्र की प्रासंगिकता बढ़ जाती है, और इसका वाचन, उच्चारण, जाप अत्यधिक मात्रा में भक्तों द्वारा किया जाता है। भारतीय परंपरा में ऐं अर्थात वाग्बीज (ज्ञानशक्ति), क्लीं अर्थात कामराज (क्रिया शक्ति), ह्रीं अर्थात मायाबीज (पदार्थ) के माध्यम से सृष्टि निर्माण, स्थिति और ध्वंस की विज्ञानसम्मत व्याख्या की गई है। इनसे ही सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों की व्याख्या की मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हुई है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भारत में रात्रि का विशेष महत्व है।
पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार भी दिन में अन्य तरंगों के कारण ध्वनि तरंगों में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए रात्रि काल में उपासना किए जाने की परिपाटी चल पड़ी। नवरात्र दीपावली, महाशिवरात्रि और होली आदि अनेक पर्व रात्रि काल में ही मनाए जाते हैं, ताकि ध्वनि की तरंगों का ठीक प्रकार से विस्तार हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मंत्र, तंत्र और यंत्र के साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों और शंख बजाकर वातावरण को न केवल रोगाणु मुक्त किया जाता है, बल्कि अपकारी शक्तियों के साथ आसुरी प्रवृत्तियों का भी शमन भली भाँति होता है।
उल्लेखनीय है कि एक वर्ष में चार संधि काल होते हैं। इसलिए वर्ष में क्रमशः चार नवरात्र चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ में मनाए जाने का विधान है। चार संधि कालों में सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करना ही नवरात्र का मूल आधार है। तन मन को निर्मल और पूर्णत: स्वस्थ रखने का अनुष्ठान ही नवरात्र है।
नौ रातों के समूह को नवरात्र कहा जाता है, जो शरीर के अंदर निवास करने वाली जीवनी शक्ति दुर्गा के ही स्वरुप हैं। उपनिषदों में उमा या हेमवती का उल्लेख किया है। वेदों में प्रयुक्त शब्द हिरण्यगर्भ शक्ति अथवा ऊर्जा के आलोक में जड़- चेतन की व्याख्या करता है। शिव – शक्ति का अद्वैत है। ऊर्जा से ही सब गतिमान हैं।
वैज्ञानिक रूप से ऊर्जा का अध्ययन वास्तव में आदिशक्ति का ही अन्वेषण है। आदिशक्ति त्रिगुणात्मक है। अपने तीन स्वरूपों क्रमशः ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति से सत्व, रज और तम गुणों को उदभुत करती है। तीनों गुणों के क्रियात्मक वेग के परस्पर संयोग से नौ यौगिक की व्युत्पत्ति होती है, जो सृष्टि का प्रथम गर्भ है। यही ब्रह्म है और यही सर्वत्र चराचर में व्याप्त है। व्यंजन वर्ण में प्राप्त स्थान की गणना की दृष्टि से भी शब्द ब्रह्म (ब=23,र् =27, ह=33,म =25, 23+27+33 +25 =108..1+0+8 =9) नौ की पुष्टि करता है।
भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के मानवीय रूपों के माध्यम से उनके गुणों और क्रियाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। वैदिक मत में परमात्मा की प्रतिमा नहीं होती- ना तस्य प्रतिमा अस्ति। लेकिन कालांतर में बौद्ध मत के आगमन के बाद प्रतीकात्मक रूप में विभिन्न आकृतियों का निर्माण कर शिवलिंग, शालिग्राम और पिंडी का पूजन आदि परम्पराएं शुरू हो गईं।
देवी के लिए पिंडी पूजन प्रारंभ हुई, क्योंकि वह गर्भ का द्योतक है। एक मादा गर्भधारण कर एक संतान को जन्म देती है जो पूर्ण होती है, और माता भी पूर्ण रहती है।
इसलिए माता ईश्वर का स्वरूप है। संसार की सभी मादाएं ईश्वर का ही स्वरूप है। यही मातृत्व शक्ति माता दुर्गा के रुप में सकल ब्रह्मांड में व्याप्त है। नारी शक्ति की अपरिमितता के कारण ही भारतीय संस्कृति में उनको -या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरुपेण संस्थिता, मातृरुपेण संस्थिता, नारी रुपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नम:।- कहकर नमन किया गया है।
उन्हें वंदनीय, पूजनीय माना गया है। भौतिकी विज्ञान में नौ ऊर्जाओं का क्रमशः स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का वर्णन है, जिनसे नौ प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। यही नवरात्र के मूल में वैज्ञानिक तथ्य हैं।
Pic Credit: ANI