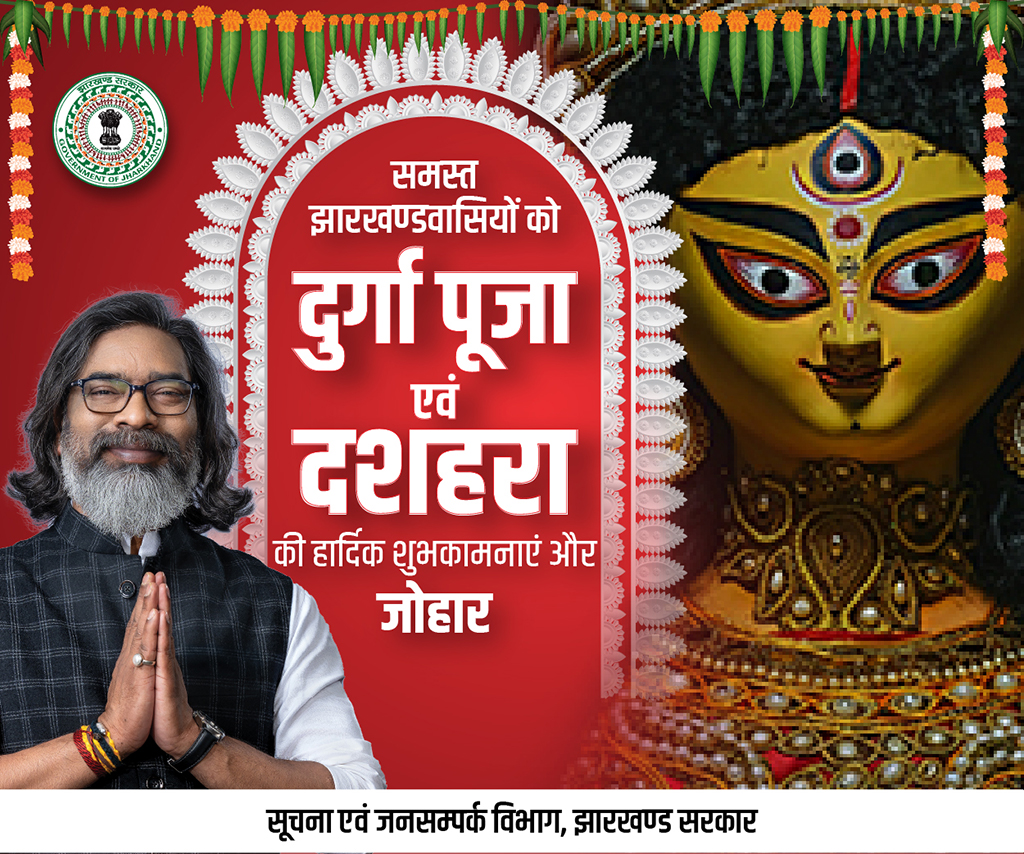झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य -पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले मुण्डा, भूमिज, हो, संथाल, उराँव आदि जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला सरहुल पर्व भारत के आदिवासी समुदायों का एक प्रमुख पर्व और महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। झारखण्ड, छतीसगढ़ आदि प्रदेशों में सरहुल महोत्सव का आयोजन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है।
1 अप्रैल 2025 -सरहुल पर्व
जनजातीय समुदाय अर्थात आदिवासी प्रकृति प्रेमी होते हैं। वे प्रकृति के अत्यंत नजदीक, काफी करीब होते हैं। उनकी समस्त गतिविधियां प्रकृति के इर्द-गिर्द ही घूमती है। आदिवासियों के प्रकृति प्रेम की अनेक गतिविधियों में से एक है सरहुल का पर्व, जिसमें प्रकृति का विधि- विधान से पूजा -अर्चना किया जाता है। वसंत ऋतु में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भारत के जनजातीय समुदाय द्वारा सरहुल का पर्व मनाए जाने की पारंपरिक व वृहत परिपाटी है।
झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य -पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले मुण्डा, भूमिज, हो, संथाल, उराँव आदि जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला सरहुल पर्व भारत के आदिवासी समुदायों का एक प्रमुख पर्व और महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है।
झारखण्ड, छतीसगढ़ आदि प्रदेशों में सरहुल महोत्सव का आयोजन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। हालांकि इस त्योहार की कोई निश्चित तिथि नहीं होती, क्योंकि विभिन्न गांवों में इसे विभिन्न तिथियों, दिनों पर मनाया जाता है।
इसलिए सरहुल का यह उत्सव कई दिनों तक चलता रहता है। लोग एक गांव से दूसरे गांव अपने संबंधियों के यहां जाकर इसे पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें प्रकृति पूजा के साथ मुख्य पारंपरिक नृत्य सरहुल नृत्य किया जाता है। झारखण्ड राज्य की राजधानी रांची में चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन सरहुल महोत्सव का मुख्य आयोजन होता है।
राजधानी के विभिन्न सरना स्थानों से आकर्षक शोभायात्रा निकाली जाती है। इस शोभायात्रा में आदिवासी समुदाय की महिलाएँ व पुरुष मांदर, ढोल, नगाड़ा आदि पारंपरिक वाद्यों की थाप पर मधुर गीतों के साथ पूरे ताल में सरहुल नृत्य कर रहे होते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित किया जाने वाला यह त्योहार धरती एवं सूर्य के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
यह नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है। जनजातियों के लिए यह नए साल की शुरुआत की निशानी है। इस वार्षिक उत्सव को बसंत ऋतु के काल में मनाया जाता है और इसमें पेड़ों और प्रकृति के अन्यान्य तत्वों की पूजा का विधान है। इस समय साल अर्थात सखुआ के पेड़ों में नवपल्लव के साथ फूल आने लगते हैं। सरहुल में साल के फूलों को शामिल किया जाता है। झारखण्ड में चैत्र शुक्ल तृतीया को सरहुल महोत्सव का आयोजन राजकीय तौर पर किए जाने के कारण इस दिन को एक राजकीय अवकाश घोषित किया गया है।
सरहुल का शाब्दिक अर्थ है -साल वृक्ष की पूजा- अर्चना। सरहुल पर्व धरती माता को समर्पित है। आदिवासियों की मान्यतानुसार इस त्योहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल मुख्यतः धान, वृक्षों के पत्ते, फूलों और फलों का उपयोग किया जाता है। भूमिज इस पर्व को हादी बोंगा के नाम से और संथाल में इसे बाहा बोंगा के नाम से मनाया जाता है। इसे बाः परब और खाद्दी परब के नाम से भी जाना जाता है। सरहुल पूजा में नई धान, ज्वार और गेहूं के फसलों को कृषि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए चढ़ाया जाता है।
इस पर्व पर आदिवासी समुदाय के लोग जल, जंगल और जमीन की पूजा करते हैं और भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। यह अनुष्ठान न सिर्फ अच्छी फसल के लिए किया जाता है, बल्कि यह प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का प्रतीक भी है। इस दिन गांव के पुरोहित अर्थात पाहन गांव के पवित्र स्थान सरना स्थल में साल के फूल चढ़ाते हैं, परंपरानुसार पूजा करते हैं। और फिर सभी ग्रामीणों के साथ सामूहिक भोज और नृत्य करते हैं। गांव के गैरआदिवासी सदान भी हर्षोल्लास के साथ शामिल होते हैं।
पूजा में धान, ज्वार चढ़ाये जाने की इस परंपरा का प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह न सिर्फ भूमि की उर्वरता और समृद्धि की कामना से जुड़ा है, बल्कि लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। आदिवासी समुदाय में साल के वृक्ष को पवित्र वृक्ष की मान्यता प्राप्त है। यही कारण है कि इस पर्व में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस पेड़ के फूल को पवित्रता, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसलिए इन्हें देवी-देवताओं को अर्पित किया जाता है।
यह पर्व जनजातीय समुदाय की एकजुटता को दर्शाता है। साल का फूल इस परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। साल वृक्ष जंगलों के संतुलन को बनाये रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस दिन जनजातीय समुदाय के पूजा स्थल सरना को साल के फूलों से सजाया जाता है।
जनजातीय संस्कृति में सरहुल का महत्व
साल के फूलों, फलों और महुआ के फलों को जायराथान अथवा सरनास्थल पर लाया जाता है, जहां पाहन अर्थात मुख्य पुजारी और सहायक पुजारी देउरी जनजातियों के सभी देवताओं की पूजा करते हैं। जायराथान पवित्र सरना वृक्ष का एक समूह है, जहां आदिवासी विभिन्न अवसरों में पूजा पाठ करते हैं। यह ग्राम देवता, जंगल, पहाड़ तथा प्रकृति की पूजा है, जिसे जनजातियों का संरक्षक माना जाता है। देवताओं की साल और महुआ फलों और फूलों के साथ पूजा की जाती है। देवताओं की पूजा करने के बाद गांव के पुजारी, पाहन एक मुर्गी के सिर पर कुछ चावल अनाज डालता है।
परंपरागत मान्यतानुसार मुर्गी के सिर से चावल के गिरने के बाद मुर्गी के द्वारा चावल खाने अर्थात चुगने पर गांव के लोगों के समृद्धि व कल्याण की भविष्यवाणी की जाती है और चावल नहीं खाने अर्थात नहीं चुगने पर गांव पर आपदा आने की संभावना व्यक्त की जाती है।
आने वाले मौसम में पानी में टहनियों की एक जोड़ी देखते हुए वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। सरहुल के समय विभिन्न गांवों में भविष्यवाणी करने की अन्य प्रक्रियाएं भी देखने को मिलती हैं। सरहुल के एक दिन पूर्व पाहन या बैगा सरना स्थल में मिट्टी के घड़े में पानी रखकर रात भर वहां छोड़ देते हैं। अगले दिन उपवास के समय सरना स्थल जाते हैं और घड़े में पानी के स्तर को देखते हैं।
और घड़े में पानी के स्तर के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं कि उस वर्ष कितनी वर्षा होगी? घड़े में पानी का स्तर कम होना इस बात का संकेत होता है कि उस वर्ष बारिश कम होगी। पानी का स्तर कम नहीं होना अथवा कुछ मात्रा में ही नीचे गिरना इस बात का संकेत होता है कि वर्षा ठीक होगी। स्पष्ट है कि घड़े के स्तर को देखकर अनुमान किया जाता है कि वातावरण में वायु में आर्द्रता कितनी है? वायु के शुष्क होने पर वह अधिक पानी सोखेगी और घड़े में पानी का स्तर नीचे जाएगा।
वायु के शुष्क होने के कारण और आर्द्रता की कमी के कारण वर्षा सीमित होगी। वातावरण में वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वह घड़े के पानी को कम सोखेगी। यह एक सामान्य अवलोकन आधारित विज्ञान है और बेहद तर्कपूर्ण है।
प्रकृति पर्व सरहुल को जनजातीय समुदाय सूर्य और धरती के विवाह के रूप में देखते है। जनजातियों की आस्था और पारंपरिक दंतकथाओं में धरती अर्थात पृथ्वी को माता के रूप में और सूर्य को एक पिता की तरह देखा गया है। वैदिक मान्यतानुसार भी सृष्टि के आदिकाल में मानव सृष्टि के लिए सूर्य ने पिता और पृथ्वी ने माता की भूमिका निभाई थी।
विवाह का अर्थ जीवन का नव सृजन होना है। यदि पृथ्वी पर जीवन है, तो उसमें सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरहुल से पूर्व पूरी धरती पलाश और सेमल के फूलों से लाल दिखने लगती है। यह लाल रंग यौवन का प्रतीक होता है।
आदिवासियों के मान्यतानुसार यह सूर्य और पृथ्वी के विवाह के समय का प्रतीक है। विवाह के समय हल्दी के पीले रंग का महत्व होने की भांति ही सखुआ के पीले फूल चारों ओर नजर आने लगते हैं। सरहुल के आने के साथ ही सखुआ पेड़ की डालियों में फूल आते हैं, नई कोपलें और नए पत्ते आते हैं।
पतझड़ के बाद वातावरण में नए जीवन का संचार होता है। जिस तरह विवाह नए जीवन की शुरुआत होती है उसी तरह सरहुल में भी सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी में नए जीवन का संचार करती है। वस्तुतः मिट्टी (पृथ्वी), जल और सूर्य के द्वारा ही नया जीवन संभव हो पाता है। इसीलिए प्रकृति और मानव के मध्य सामंजस्य का संदेश देने वाला यह पर्व पूरे समुदाय के लिए सुख- समृद्धि, कल्याण और प्रसन्नता की कामना करता है।
Also Read: क्रिकेट के बादशाह विराट कोहली ने IPL से संन्यास का ऐलान किया…..
Pic Credit : ANI