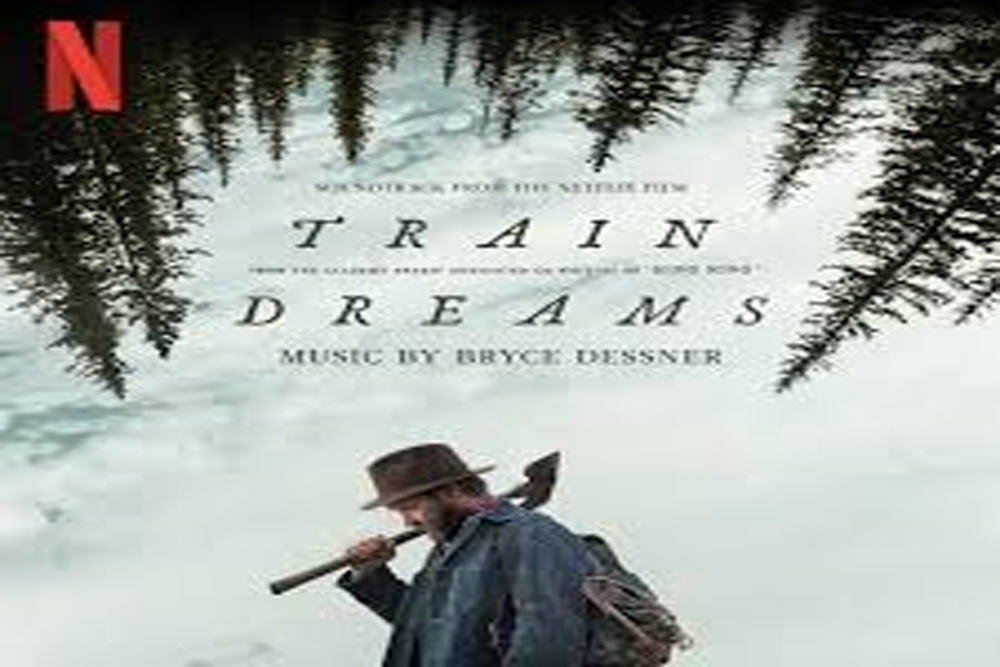चीन अभी भी रेयर अर्थ खनिजों के निर्बाध निर्यात पर सहमत नहीं हुआ है। इस मामले में उसने लाइसेंसिंग पॉलिसी जारी रखी है। इसका मतलब है कि हर कंपनी अपनी जरूरत के मुताबिक इन खनिजों के आयात की अर्जी देगी। उस पर निर्णय चीन की सरकारी एजेंसी करेगी।… दुनिया के ज्यादातर देशों ने व्यापार समझौते के लिए ट्रंप प्रशासन की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। ब्रिटेन, वियतनाम, और इंडोनेशिया ने ट्रंप की कई शर्तों को माना है, मगर जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील और यहां तक कि यूरोपियन यूनियन ने भी सीधे समर्पण करने से इनकार कर दिया।
एक दशक से अधिक समय से अमेरिका की विदेश एवं सामरिक नीतियों का मकसद चीन को घेरना और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुए इस देश के अभूतपूर्व उदय को रोकना है। इस मकसद से बराक ओबामा के समय तय की गई pivot to Asia (एशिया की ओर झुकाव) नीति हर अगले राष्ट्रपति के कार्यकाल में अधिक आक्रामक होती गई है। ओबामा ने इस नीति की घोषणा 2011 में की। 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ते हुए इसे अधिक धार देने की कोशिश की।
जो बाइडेन के प्रशासन ने इसे और आगे बढ़ाया। ट्रंप के व्यापार युद्ध को बाइडेन ने जारी रखा और साथ ही small yard, high fences की रणनीति उसमें जोड़ी, जिसके तहत चीन को सेमीकंडक्टर, हाई टेक चिप और क्वांटम कंप्यूटिंग में सहायक तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए। बाइडेन प्रशासन ने इस रणनीति में तमाम साथी और सहयोगी देशों को भी शामिल किया- उन देशों की कंपनियों पर भी चीन के साथ हाई टेक क्षेत्र में किसी तरह का संबंध रखने पर रोक लगा दी गई।
अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने वैसे तो सारी दुनिया के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ रखा है, लेकिन बारीक नजर डालें, तो यह साफ होता है कि इसमें भी मुख्य ध्यान चीन की व्यापार एवं आर्थिक ताकत को कमजोर करने पर केंद्रित है। मगर इस बार उन्हें मुश्किल इस बात से हुई है कि चीन ने जवाबी युद्ध का रास्ता अपना लिया है। ऐसा संभवतः वह इसलिए कर पाया कि इस बार उसने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी।
और जब चीन ने जवाबी हमला किया, तो अमेरिका के कदम लड़खड़ाते नजर आए हैं। गौरतलब है कि मार्च में व्यापार युद्ध शुरू करने और गुजरे दो अप्रैल को तथाकथित जैसे को तैसा (reciprocal) टैरिफ का एलान करने के बाद ट्रंप प्रशासन अब तक आधा दर्जन से भी कम देशों के साथ ही व्यापार समझौता कर पाया है। इनमें ब्रिटेन, जापान, वियतनाम, और इंडोनेशिया प्रमुख हैं। उन समझौतों से जाहिर है कि ट्रंप ने इस देशों के जरिए अमेरिका को निर्यात जारी रखने की चीनी कंपनियों की कोशिश पर खास शिकंजा कसने पर अपना ध्यान टिकाए रखा है। खास कर वियतनाम से हुए समझौते में ट्रांसशिपमेंट का प्रावधान जोड़ा गया है। जिन निर्यातों को इस श्रेणी में रखा जाएगा, उन पर दो गुना टैरिफ अमेरिका में लगेगा।
इस बीच दो दौर में हुई वार्ता के दौरान ट्रंप प्रशासन की चीन के साथ भी कुछ सहमतियां भी बनीं। मगर ये कहानी बिल्कुल अलग है। चीन के साथ अब तक भावी व्यापार के किसी मूलभूत सिद्धांत या शर्तों पर सहमति बनी है। सिर्फ कुछ व्यावहारिक सहमतियां बनी हैं, जिन्हें किसी रूप में अमेरिका की जीत नहीं कहा जा सकता। बल्कि चीन के साथ जिन शर्तों पर ट्रंप प्रशासन राजी हुआ, उसे अमेरिका की कदम वापसी के रूप देखा जाएगा।
इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं। चीन के जिस प्रतिबंध ने अमेरिका में (और वैसे तो दुनिया के बहुत से दूसरे देशों में भी) हलचल मचा दी, वह रेयर अर्थ खनिजों का निर्यात रोकने का उसका फैसला था। अमेरिका ने चिप, सेमीकंडक्टर, और अन्य उच्च तकनीक का चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। तो चीन ने उसके जो जवाब दिए, उनमें रेयर अर्थ खनिज सबसे कारगर साबित हुए हैं।
इसके दबाव में ट्रंप प्रशासन चीन से वार्ता की पहल करने पर मजबूर हुआ। यहां तक कि खुद ट्रंप ने अपनी पहल पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन किया। उसके बाद व्यापार वार्ता का दूसरा दौर हुआ। हर व्यापार समझौते का तुरंत अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ब्योरा देने वाले ट्रंप ने चीन के साथ बनी सहमति की कोई जानकारी साझा नहीं की। सिर्फ यह बताया कि सहमति बनी है। क्यों?
असल बात अब जाहिर हुई है। ध्यान देः चीन अभी भी रेयर अर्थ खनिजों के निर्बाध निर्यात पर सहमत नहीं हुआ है। इस मामले में उसने लाइसेंसिंग पॉलिसी जारी रखी है। इसका मतलब है कि हर कंपनी अपनी जरूरत के मुताबिक इन खनिजों के आयात की अर्जी देगी। उस पर निर्णय चीन की सरकारी एजेंसी करेगी। अगर इस एजेंसी को लगेगा कि संबंधित निर्यात का इस्तेमाल सैन्य मकसद के लिए भी हो सकता है, तो ऐसे निर्यात को इजाजत नहीं दी जाएगी। बाकी अर्जियों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने चीन को इतने पर रजामंद कर लेने को अपनी कामयाबी बताया है।
बहरहाल, बदले में ट्रंप प्रशासन ने क्या मंजूर किया, वह कहीं ज्यादा अहम है। उसने चिप निर्यात पर प्रतिबंध की नीति में ढील दे दी है, जिसे small yard, high fences की नीति के तहत बाइडेन प्रशासन ने लागू किया था। अब अमेरिकी कंपनियां कई प्रकार के उन्नत चिप्स का निर्यात चीन को कर सकेंगी। यह फैसला होते ही दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी एनविडिया के प्रमुख जेनसेन हुआंग चीन की यात्रा पर पहुंच गए। इस वर्ष तीसरी बार चीन पहुंचे हुआंग ने वहां एलान किया कि उनकी कंपनी एच20 एआई चिप के निर्यात की तैयारी में है। उधर एएमडी कंपनी ने एमआई308 एआई चिप का चीनी कंपनियों को निर्यात करने का इरादा जता दिया है। और इस तरह high fences (ऊंचे घेरों) में कुछ fences (घेरे) ढह गए हैँ।
(https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3318471/how-easing-ai-chip-controls-could-reshape-us-china-trade-talks)
हुआंग ने चीन यात्रा के दौरान जो कहा, उससे यह और साफ हो गया है कि प्रतिबंध की अमेरिकी नीति लगभग नाकाम रही है। अमेरिकी नजरिए से देखें, तो इस नीति का उलटा नतीजा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप चीन ने अपनी राष्ट्रीय शक्ति चिप और अन्य हाई टेक में आत्म निर्भर होने में झोंक दी। अब जो स्थिति है, उसके संबंध में एनविडिया प्रमुख की ये टिप्पणी गौरतलब हैः ‘चीन के पास विशाल, गतिशील और आविष्कारक क्षमता से अति संपन्न बाजार है। साथ ही यह एआई शोधकर्ताओं का घर बन चुका है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि अमेरिकी कंपनियां चीन में अपनी जड़ें जमाएं। एआई का चीन में तेजी से विकास हो रहा है।’ हुआंग ने यह उल्लेख भी किया कि इस समय अमेरिका से (ट्रंप के नीतियों के कारण) हो रहा ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन) चीन के लिए खास लाभदायक साबित हो रहा है।
यह आम समझ है कि इस वक्त दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है। इस दौर की तकनीकें आम रहन-सहन, कामकाज, एक दूसरे से संपर्क के तौर-तरीके बदल रही हैं। तकनीकों के मिलन की वजह से भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों में पहले से मौजूद रहीं सीमाएं ढह रही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल नेटवर्किंग के जरिए साइबर- भौतिक सिस्टमों का विकास, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण हेल्थ केयर, कृषि आदि क्षेत्रों में ऐसे नए आविष्कार हो रहे हैं, जो इस दौर की पहचान बन गए हैं। इनमें से ज्यादातर तकनीकों में चीन ने अपनी अग्रणी भूमिका बना ली है।
इसके अलावा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन ने विशेष भू-अर्थनीति के जरिए अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुंच में जिस हद तक विस्तार किया है, उसने उसे पश्चिम के व्यापार युद्ध एवं प्रतिबंधों का मुकाबला करने में और अधिक सक्षम बना दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिटिएव (बीआरआई) के तहत चीन को निवेश, निर्माण एवं अपनी उत्पादक क्षमताओं का अन्य देशों में प्रसार करने के व्यापक अवसर मिले हैं। तकरीबन 140 देश आज बीआरआई का हिस्सा हैं। इनके साथ विश्व विकास पहल (GDI), विश्व सुरक्षा पहल (GSI) एवं विश्व सभ्यता पहल (GCI) के जरिए चीन ने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अपनी कूटनीतिक पहुंच को सशक्त किया है।
इन सबसे दुनिया में बिल्कुल नई परिस्थिति बनी है। नतीजतन, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के दांव आज उस तरह कारगर नहीं हो रहे हैं, जैसा अभी डेढ़ दशक पहले तक हो जाता था। मगर ‘पश्चिम’ इस बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। अपनी शक्ति एवं प्रभाव के क्षय के प्रति उसने इनकार का नजरिया अपना रखा है। नई परिस्थितियों से आंख मिलाने को वह तैयार नहीं है और इस विभ्रम का शिकार बना हुआ है कि दुनिया पर अब भी उसका पहले जैसा ही शिकंजा है।
अपने दक्षिणपंथी नजरिए, मगर यथार्थवादी प्रस्तुति के लिए जानी जाने वाली अमेरिकी वेबसाइट- American Affairs Journal पर अपनी एक हालिया टिप्पणी में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पॉलिटिकल इकॉनमी और अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय के प्रोफेसर ली जॉन्स ने लिखाः ‘आज का सबसे महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम क्षय हैः चीजें बिखर रही हैं और केंद्र उसे संभालने में अक्षम है। ट्रंप और उनके साथी खुद क्षयशील नव-उदारवादी व्यवस्था का परिणाम है। यह व्यवस्था अपने अंतर्विरोधों के दबाव में ढह रही है। ट्रंप का उदय और वापसी प्रातिनिधिक लोकतंत्र में हुए व्यापक क्षय का संकेत है। आज नागरिकों और उनका प्रतिनिधि होने का दावा करने वालों के बीच रिश्ता टूट गया है, जिससे वह खालीपन पैदा हुआ है, जिसमें सस्ती जनप्रियता (populist) जुटा लेने वाले नेता पनप रहे हैं। अन्य देशों की तरह अमेरिका की राजनीतिक पार्टियां भी खोखली हो गई हैं। इसी वजह से ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी पर कब्जा जमाने में सफल हुए। न्यू डील व्यवस्था को ध्वस्त किए जाने के बाद से अमेरिकी राज्य भी कमजोर हुआ है। आज इसमें अपने नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने की क्षमता नहीं रही, जबकि यह अत्यधिक विनियामक कर्त्तव्यों के बोझ तले दबा हुआ है।…
पुरानी व्यवस्था से चिपके लिबरल्स के विपरीत ट्रंप समर्थकों की ताकत यह है कि उनमें नव-उदारवादी व्यवस्था के अंतर्विरोधों को देख पाने, उस बारे में बोल पाने और उस पर प्रतिक्रिया जताने की आंशिक क्षमता है। मगर क्षय का सार्थक समाधान पेश करने के बजाय असल में ट्रंप इसकी गति और तेज कर रहे हैं। इसे ट्रंपवादी विश्व-दृष्टि की वैचारिक सीमा के रूप में समझा जा सकता है। इस सीमा के कारण समस्याओं का जो समाधान वे पेश कर रहे हैं, उनमें निहित अंतर्विरोधों को स्पष्ट रूप से वे नहीं देख पा रहे हैं। ये समाधानों से अमेरिकी वर्चस्व के पुनर्स्थापित होने की संभावना कम है, जबकि इसमें लगे घुन के और सघन हो जाने की संभावना अधिक है।’
(https://americanaffairsjournal.org/2025/05/trumps-tariff-gamble-and-the-decay-of-the-neoliberal-order/)
इसीलिए अनेक विशेषज्ञों ने हालिया वर्षों में विभिन्न अमेरिकी प्रशासनों की तरफ से दुनिया पर दबदबा जताने के लिए उठाए गए कदमों को denial, disavowal और delusion से ग्रस्त माना है। denial और disavowal (यानी इनकार) बदले समीकरणों के प्रति है, जबकि delusion (विभ्रम) यह मानना है कि आज भी अमेरिका अपने हित और अपनी इच्छाओं को दुनिया पर थोपने में सक्षम है। टैरिफ वॉर को इसी delusion का परिणाम समझा गया है।
नतीजा यह हुआ कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने व्यापार समझौते के लिए ट्रंप प्रशासन की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। ब्रिटेन, वियतनाम, और इंडोनेशिया ने ट्रंप की कई शर्तों को माना है, मगर जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील और यहां तक कि यूरोपियन यूनियन ने भी सीधे समर्पण करने से इनकार कर दिया।
और बात सिर्फ इतनी नहीं है। सत्ता में आने के छह महीनों के भीतर ट्रंप को अहसास हो चुका है कि व्लादीमीर पुतिन को एक फोन कर यूक्रेन युद्ध रुकवा देने की उनकी खुशफहमी का कोई ठोस आधार नहीं था। तो उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने की नई योजना बनाई। इसके तहत उन्होंने यूरोपीय देशों से कहा कि वे अमेरिकी कंपनियों से हथियार खरीद कर यूक्रेन को भेजें। मगर इस पर जर्मनी, इटली, और चेक रिपब्लिक सहित कई देशों की प्रतिक्रिया उनके मनमाफिक नहीं रही है।
साफ है कि पिछले कुछ वर्षों में बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के आकार लेने की जो परिघटना आगे बढ़ी है, उसे ट्रंपवादी तरीके से पलटने की अमेरिकी शासक वर्ग की मंशा कहीं पूरी होती नहीं दिखती। इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल हडसन ने कहा है कि चीन ने पश्चिमी नव-उदारवादी व्यवस्था का एक विकल्प पेश कर दिया है, जिससे ग्लोबल साउथ के देशों को अमेरिका केंद्रित वित्तीय उपनिवेशवाद के शोषण को चुनौती देने एक आधार मिल गया है।
(https://geopoliticaleconomy.com/2025/07/17/michael-hudson-global-majority-us-financial-colonialism/)
तो आज की असल कहानी यही है। सदियों तक कायम रहे पश्चिमी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बरक्स समाजवाद का एक नया प्रयोग सफलता की कहानियां लिख रहा है। इसका असर ठीक वैसा ही हुआ है, जैसा वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन की परिघटना से हुआ है। इस ऐतिहासिक बदलाव को ना समझना अमेरिकी शासक वर्ग, खास कर ट्रंप और उनके साथियों की सबसे बड़ी नाकामी है। नतीजा यह है कि अमेरिकी शासक वर्ग ने उन्हें अपना ट्रंप कार्ड मान कर उन पर अपना दांव जरूर लगाया, मगर असल बाजी में इस दांव के हर पत्ते पिट रहे हैं।