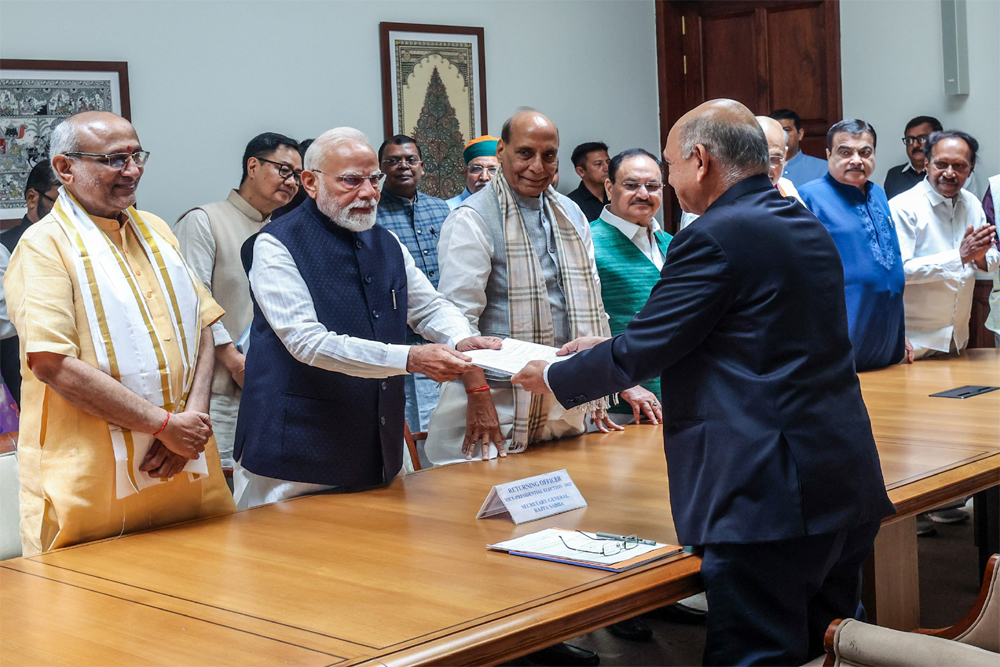गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरुकुलों में दीक्षांत समारोह आयोजन किए जाते थे। गुरु पूर्णिमा की मंगल बेला में ही छात्रों को स्नातक उपाधियां प्रदान की जाती थीं। गुरु की सभी शिक्षाओं को आत्मसात कर लेने वाले विद्यार्थी, जिनकी कुशलता व क्षमता पर गुरु को संदेह नहीं रहता था, उन्हें इस दिन उपाधियां प्रदान की जाती थीं।
भारतीय सभ्यता- संस्कृति, धर्म- दर्शन, श्रुति- वांग्मय में गुरु को ब्रह्म से भी ऊंचा स्थान व अधिक महत्व प्रदान किया गया है। गुरु को प्रेरक, सत्य ज्ञान प्रदाता, प्रथम आभास देने वाला, सच्ची लौ जगाने वाला और कुशल आखेटक कहा गया है, जो अपने शिष्य को अज्ञान रुपी अंधकार से दूर करके सत्य ज्ञान से प्रकाशित कर उसमें सन्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है, मार्ग दिखाता है। अपने उपदेश की वाणों से बिंध कर उसमें प्रेम की पीर संचरित कर देता है। साधक को अपनी आध्यात्मिक साधना में, व्यक्ति को अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कोई भी विघ्न उपस्थित होने पर किसी विद्वान से मार्ग निर्देशन प्राप्त करने की अनिवार्यता होने के कारण साधक, व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की प्राप्ति द्वारा साधक अथवा व्यक्ति के ह्रदय से संशय व आशंका की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं।
उसे साधना अथवा व्यक्तिगत लक्ष्य के मार्ग में एक मददगार अर्थात सहायक मिल जाता है, जो उसे विघ्नों और बाधाओं से परे निकाल सकता है। उसके पैर डगमगाने पर उसे सहारा दे सकता है। उसके साधना अथवा कार्य में निराश होने पर उसमे आत्मविश्वास जगाकर आगे बढ़ा सकता है अथवा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। गुरु का योग्य होना उतना ही आवश्यक है जितना कि शिष्य का। क्योंकि यदि गुरू स्वयं ही अयोग्य होगा तो वह तो शिष्य को ही ले डूबेगा। गुरु की सेवा में शिष्य को भी सर्वात्मना समर्पित हो जाना चाहिए। गुरु की असीम कृपा शिष्य पर होती है। वस्तुतः वह ब्रह्म की कृपा पर उतना नहीं आश्रित रहता जितना गुरु की। वैदिक मतानुसार सत्य राह दिखने वाला परमात्मा का ही उसके अनंत दिव्य गुणों के कारण असंख्य नामों में से एक नाम गुरु भी है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं माना गया है।
गृ शब्दे इस धातु से गुरु शब्द बना है। निरुक्त में कहा गया है -यो धर्म्यान् शब्दान गृनात्युपदिशति स गुरुः स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात। योग जो सत्य धर्म प्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। गुरु तो माता, पिता, आचार्य और अतिथि होते हैं। उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या, शिक्षा लेनी-देनी शिष्य और गुरु का कार्य है। गुरु की व्युत्पति करते हुए कहा गया है- गारयति ज्ञानम् इति गुरुः । गुरु उसे कहते हैं, जो ज्ञान का घूंट पिलाए।
ज्ञान का मानव जाति के लिए अति महत्व होने की भांति ही ज्ञान का वितरण करने वाले का भी मनुष्य जाति मात्र के लिए महत्व है। ज्ञान की प्राप्ति में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यही कारण है कि वेदों से लेकर वर्तमान भारतीय साहित्य में गुरु की अपार महिमागान की गई है। वेदों में स्पष्ट रूप से गुरु का वर्णन नहीं है, लेकिन वेद में अनेक स्थानों पर विभिन्न देवताओं की स्तुतिगान करते हुए उनसे ज्ञान दान की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें गुरु माना गया है तथा उनके महत्व को स्वीकार गया है। उपनिषद ग्रंथों में भी सर्वत्र गुरु की महिमा गान की गई है। आत्मा साधारण बुद्धि वाले पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेद्दर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किये गये इस आत्मा में कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा दुर्विज्ञेय है। उपनिषदों में गुरु के सुविज्ञ और शिष्य के लगनशील होने पर बहुत जोर दिया गया है। वेदांत के मतानुसार आत्मा का साक्षात्कार कर चुके सिद्ध पुरुषों द्वारा जो जीवन्मुक्त (जीवित रहकर भी मुक्त) रहते हैं, विधिपूर्वक वेद-वेदांग पढ़े हुए, नित्य, नैमितिक, प्रायश्चित और उपासना नामक कर्मों द्वारा समस्त पापों से रहित साधक को ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। वेदान्त के ही नहीं, समस्त विद्याओं को पढने के लिए प्रारंभ में ही अधिकारी तथा उसके उद्देश्य की चर्चा की जाती थी।
रामायण में वशिष्ठ मुनि के गुरुत्व का एक महान गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन अंकित है। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजा के कुलगुरु वशिष्ठ ने त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र, रोहिताश्व आदि को सतयुग में ज्ञान दान किया था और बाद में वही त्रेता में दिलीप, रघु, अज, दशरथ और राम आदि के भी गुरु थे। इतने लम्बे काल तक एक व्यक्ति का जीना असम्भव है। यही कारण है कि विद्वतजन वशिष्ठ को एक व्यक्ति नहीं वरन एक परंपरा मानना ही उचित समझते हैं। इसी भांति व्यास भी एक परंपरा है। वेदों के विभक्तिकार और अठारह पुराणों के रचयिता कदापि एक नहीं हो सकते। मनु महाराज ने विद्यार्थियों (शिष्यों) को धर्म का उपदेश करते समय माता-पिता एवं गुरु की महिमा गाई है। मनुस्मृति में अनेक प्रकार से गुरु को महान बत्ताते हुए कहा है कि गुरु की सेवा द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से इस सत्य का सत्यापन होता है कि भारतीय संस्कृति में अनेक महानुभावों को गुरु के आशीर्वाद एवं सानिध्य से ही देवत्व की प्राप्ति हुई है। शांतनु नन्दन देवव्रत को भीष्म बनाने में ऋषि परशुराम की अहम भूमिका रही थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समर्थ स्वामी रामदास ने शिवाजी महाराज को राष्ट्रवादी राजा बनाया था। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा ली थी एवं उनके सानिध्य में ही अपना जीवन प्रारम्भ किया था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन महानुभावों को देवत्व प्राप्त करने के लिए गुरु के श्रीचरणों में जाना पड़ा है। इस प्रकार के कई उदाहरणों से हमारा भारतीय इतिहास भरा पड़ा है।
अपने गुरु को देवता के समान मानने वाले आरुणि अथवा उद्दालक ने अपनी गुरु-भक्ति से गुरु धौम्य को भी अमर बना दिया, जो खेत से बहते पानी को रोकने की गुरु की आज्ञापूर्ति के लिए पानी न रुकता देखकर मेड़ पर ही लेट गया था। भवभूति ने गुरु के बारे में कहा है- गुरु बुद्धिमान और जड़ दोनों ही प्रकार के शिष्यों को समान रूप से विद्या प्रदान करता है, परन्तु जड़ शिष्य दुर्भाग्य से बुद्धिमान की अपेक्षा कम ग्रहण कर पाता है। सच्चे गुरु की खोज में भगवान बुद्ध कई वर्षों तक जंगलों में विचरते रहे और अंततः उन्हें अपना गुरु स्वयं बनना पड़ा था। बुद्ध कुक्कुट मिश्र की भांति नहीं थे, जो गुरु की वाणी का पांच दिन अध्ययन कर, वेदान्त शास्त्रों का तीन दिन मनन कर तथा तर्कशास्त्र को सूंघकर ही अपने को अद्वितीय ज्ञानी समझने, मानने लगे थे।
प्राचीन ग्रंथों में पराशर नन्दन व्यास को महाशाल शौनकादि कुलपतियों तथा गुरुओं के भी परम गुरु साक्षात वादरायण माना गया है। पुराणों में व्यास परमपूज्य घोषित किये गए हैं। कतिपय विद्वानों के अनुसार कृष्ण द्वैपायण वेदव्यास वेद, पुराण, महाभारत, वेदान्त-दर्शन (ब्रह्मसूत्र), सैंकड़ों गीताएँ, शारीरिक सूत्र, योगशास्त्र के साथ ही कई व्यास स्मृतियों के रचयिता हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान का सम्पूर्ण विश्व विज्ञान एवं साहित्यिक वांग्मय भगवान व्यास का उच्छिष्टत है। कहा है- व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्। कृष्ण द्वैपायण वेदव्यास का जन्म आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ माना जाता है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है।
भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को आदिगुरू, प्रथम गुरु की संज्ञा प्राप्त है। पौराणिक मान्यतानुसार भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को योग की दीक्षा देना भी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा की तिथि के दिन से प्रारम्भ किया था। प्राचीन काल में भारत के गुरुकुलों में गुरु पूर्णिमा को महोत्सव का स्वरूप देते हुए एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता था। गुरूकुल से सम्बंधित अनेक मुख्य कार्य गुरु पूर्णिमा के दिन ही सम्पन्न किए जाते थे। गुरु पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर ही नए छात्रों को गुरूकुल में प्रवेश प्रदान किया जाता था। इसलिए गुरु पूर्णिमा दिवस गुरूकुल में छात्र प्रवेश दिवस के रूप में मनाया जाता था। सभी जिज्ञासु छात्र इस दिन पूज्य गुरुदेव के समक्ष आकर हाथों में समिधा लेकर और स्वयं को समिधा रूप में अर्पित करने का संकल्प लेते हुए पूज्य गुरुदेव के समक्ष आकर अंतर्मन में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आदरपूर्वक प्रार्थना करते थे।
गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरुकुलों में दीक्षांत समारोह आयोजन किए जाते थे। गुरु पूर्णिमा की मंगल बेला में ही छात्रों को स्नातक उपाधियां प्रदान की जाती थीं। गुरु की सभी शिक्षाओं को आत्मसात कर लेने वाले विद्यार्थी, जिनकी कुशलता व क्षमता पर गुरु को संदेह नहीं रहता था, उन्हें इस दिन उपाधियां प्रदान की जाती थीं। वे गुरु चरणों में बैठकर प्रण लेते थे कि हे गुरुवर, आपके सान्निध्य में रहकर, आपकी कृपा से हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, उसे लोक हित और कल्याण के लिए ही उपयोग करेंगे। अपने परम पूज्य गुरुदेव को दक्षिणा देकर छात्र अपने कार्य क्षेत्र में उतरते थे। इस प्रकार प्राचीन काल में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुकुलों में गुरु का कुल बढ़ता भी था और विश्व में फैलता भी था। जैन एवं बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए भी गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व का माना जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में भगवान महावीर 24वें व परम तीर्थंकर के रूप में परिगणित हैं।
भगवान महावीर ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इंद्रभूति गौतम को अपने प्रथम शिष्य के रूप में स्वीकार किया था अर्थात भगवान महावीर ने गौतम को दीक्षित कर उसे अपना प्रथम शिष्य बनाने का गौरव प्रदान किया था। यही कारण है कि जैनी लोग गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाते हैं कि इस दिन उन्हें भगवान महावीर गुरु रूप में मिले थे। बौद्ध पंथ के अनुसार बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद प्रथम बार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही पांच परिव्राजकों को धम्मोपदेश दिया। बौद्ध सम्प्रदाय की मौलिक शिक्षाएं इसी दिन अस्तित्व में आई।