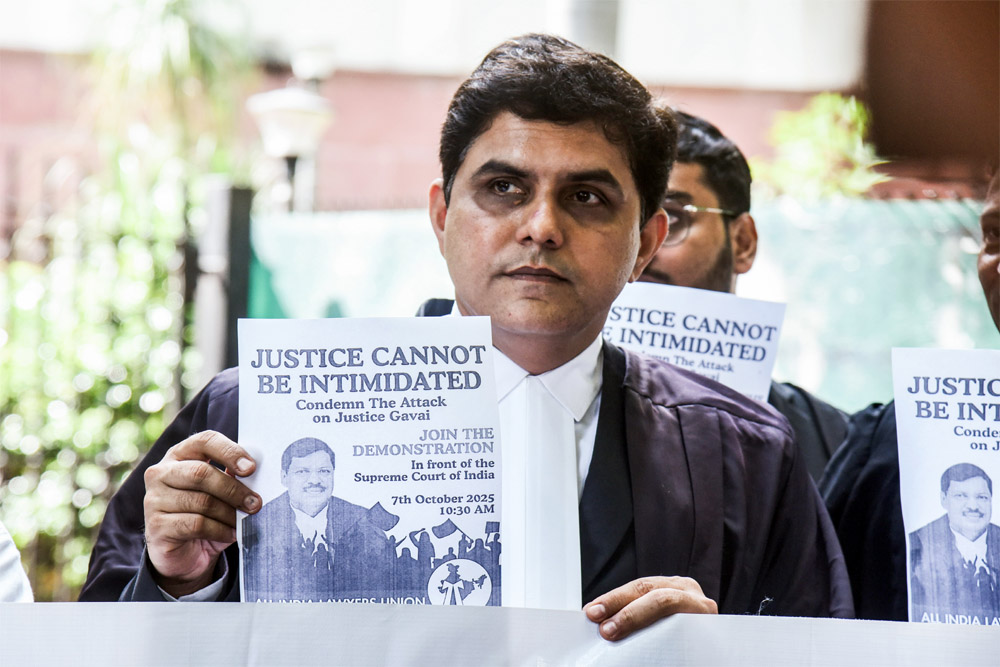जैसे वेदों की ऋचाएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति से आगे बढ़ती थीं, वैसे ही किसान अपने अनुभव और ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। इन अनुभवों ने धीरे-धीरे कहावतों और लोकोक्तियों का रूप ले लिया। ‘घाघ’ और ‘भड्डरी’ जैसे लोकज्ञानी आज भी किसानों की जुबान पर हैं — उनकी कही बातें आज भी वैज्ञानिक परीक्षण में खरी उतरती हैं। पुराने समय में गांवों की संरचना ही ऐसी होती थी जिसमें सिर्फ मनुष्य नहीं, पशुओं के लिए भी जगह होती थी — चारागाह, गोचर, तालाब, पोखर। हर गांव में अनाज, दाल, तिलहन, सब्जी और फल — सब कुछ पैदा होता था। मडुआ, ज्वार, कोदो, तिवड़ा, कुल्थी, अलसी, कुट्टू जैसे मोटे अनाज पोषण से भरपूर होते थे और कम पानी में उग जाते थे।
भारत को सदियों से कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। यहां खेती न केवल जीवन का आधार थी, बल्कि एक पारिवारिक परंपरा और सांस्कृतिक उत्तराधिकार भी थी। जैसे वेदों की ऋचाएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति से आगे बढ़ती थीं, वैसे ही किसान अपने अनुभव और ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। इन अनुभवों ने धीरे-धीरे कहावतों और लोकोक्तियों का रूप ले लिया। ‘घाघ’ और ‘भड्डरी’ जैसे लोकज्ञानी आज भी किसानों की जुबान पर हैं — उनकी कही बातें आज भी वैज्ञानिक परीक्षण में खरी उतरती हैं।
लेकिन आज हम उस ज्ञान परंपरा से कट चुके हैं। विदेशी शिक्षा, पद्धति और जीवनशैली को अपनाने की अंधी दौड़ में हमने अपनी पारंपरिक कृषि, जीवनचर्या और आत्मनिर्भरता को पीछे छोड़ दिया है। नतीजा यह हुआ कि आज जब अन्न संकट की आहट सुनाई देती है, तो देश के लोग राशन कार्ड के लिए महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, घंटों दुकानों की कतार में खड़े होकर अंगूठा लगाते हैं — उस देश में, जिसकी पारंपरिक कृषि कभी ‘अन्नपूर्णा’ कहलाती थी।
पुराने समय में गांवों की संरचना ही ऐसी होती थी जिसमें सिर्फ मनुष्य नहीं, पशुओं के लिए भी जगह होती थी — चारागाह, गोचर, तालाब, पोखर। हर गांव में अनाज, दाल, तिलहन, सब्जी और फल — सब कुछ पैदा होता था। मडुआ, ज्वार, कोदो, तिवड़ा, कुल्थी, अलसी, कुट्टू जैसे मोटे अनाज पोषण से भरपूर होते थे और कम पानी में उग जाते थे। तब के लोग आज की तरह बीमारियों से घिरे नहीं थे। गांवों में कपास से कपड़ा, चरखा-करघा, तेल पेरने की घानी, लकड़ी के औज़ार, साबुन, दवा, जूते, रस्सी — सब कुछ स्थानीय रूप से बनता था। यह पूरी व्यवस्था बिना बिजली के, सिर्फ मानवीय श्रम और पशुशक्ति पर आधारित थी।
लेकिन अंग्रेजों ने जैसे हमारी भाषा, इतिहास और धार्मिक परंपराओं को तोड़ने का काम किया, वैसे ही हमारी कृषि व्यवस्था को भी निशाना बनाया। भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया गया — कपास, नील, गन्ना जैसी नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया गया, अनाज पीछे छूट गया। अकाल आए, तो बाहर से बौने बीज लाकर देश में हरित क्रांति के नाम पर उनकी खेती शुरू कराई गई। इन बीजों की उपज बढ़ाने के नाम पर रासायनिक खाद, कीटनाशक और भारी यंत्रों का इस्तेमाल किया गया — जिससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हिल गई।
खेती महंगी होने लगी, पशुधन खत्म हुआ, मजदूर शहरों की ओर भागे और गांव खाली होते चले गए। जिसे हमने ‘विकास’ समझा, वह असल में हमारी परंपरा से दूरी थी। आज भी किसान स्थानीय बीज, खाद या औज़ार नहीं बना पाते — उन्हें सब कुछ बाहर से खरीदना पड़ता है। बीज से लेकर ट्रैक्टर और बैंक ऋण तक — सब पर निर्भरता बढ़ती चली गई।
1960 के बाद हाईब्रिड बीजों की शुरुआत हुई, जिसमें ज्यादा सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों की जरूरत होती थी। इससे गेंहू और धान की पैदावार बढ़ी जरूर, पर जल, भूमि और पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ा। नलकूपों से अंधाधुंध सिंचाई के कारण भूजल स्तर गिरा। मिट्टी की उर्वरता खत्म होने लगी। यह सब प्राकृतिक चक्र से छेड़छाड़ का नतीजा था।
आज भारत की कृषि योग्य जमीन का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर है। ऐसे में सिंचाई की सही व्यवस्था न होने से उत्पादन में अस्थिरता बनी रहती है। जहां कभी देश की 82% से अधिक आबादी खेती से जुड़ी थी, आज यह आंकड़ा घटकर 45% से भी नीचे चला गया है। यह गिरावट हमें सोचने पर मजबूर करती है — आखिर कृषि की दशा इतनी क्यों बिगड़ी?
आज सरकारें कृषि को लाभदायक बनाने की बात कर रही हैं। किसानों को साल में छह हजार रुपये देकर खेती से जोड़े रखने की कोशिश हो रही है। पर सवाल यह है कि क्या खेती को सम्मान और स्थायित्व दिलाने के लिए यही काफी है? जब तक किसानों को उनकी ज़मीन पर खेती करने के बदले सुनिश्चित आय नहीं मिलेगी, जब तक कृषि उत्पादों का सही मूल्य और बाजार नहीं मिलेगा — तब तक किसान खेत से जुड़े नहीं रह सकते।
परंपरागत कृषि को केवल अन्न उपजाने की प्रक्रिया मानना भूल होगी। यह एक समृद्ध सांस्कृतिक प्रणाली थी — जिसमें बागवानी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई कार्य जुड़े होते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इन क्षेत्रों की योजनाएं और नीतियां भी अब ऐसे अफसरों के हाथों में हैं जिन्हें न खेत की जानकारी है, न मिट्टी की पहचान। आज देश भर में कृषि से जुड़ी योजनाओं और मंत्रालयों में सैकड़ों पदों पर ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिन्हें खेती का व्यावहारिक अनुभव नहीं है।
देश की लगभग 57% श्रमिक जनसंख्या अब भी किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ी है। लेकिन कृषि की ढांचागत व्यवस्था, भूमि उपयोग नीति, जल प्रबंधन और विविधीकरण जैसे बुनियादी सवालों पर ठोस काम नहीं हो रहा। भूमि का क्षरण हो रहा है, खेती की लागत बढ़ रही है और ज़मीन घट रही है। बीते दो दशकों में देश में कृषि योग्य भूमि में 28 लाख हेक्टेयर की कमी आई है।
आज ज़रूरत इस बात की है कि भारतीय कृषि को उसकी पारंपरिक समझ और समृद्ध जैव विविधता के साथ जोड़ा जाए। भारत में छह ऋतुएं हैं, दर्जनों प्रकार की मिट्टी है, हर फसल के अनुकूल जलवायु है — हमें अपनी उस विरासत को पुनः जीवित करना होगा। केवल रासायनिक खाद और ट्रैक्टर से खेती को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता।
आज का खाद्यान्न संकट और महंगाई केवल नीति से नहीं, खेती से ही सुलझ सकती है — वह खेती जो सिर्फ ‘उत्पादन’ नहीं, बल्कि जीवन का आधार हो। हमें यह समझना होगा कि कृषि सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, सभ्यता की नींव है — और अगर यह नींव कमजोर होगी, तो देश की आत्मा भी डगमगाएगी।