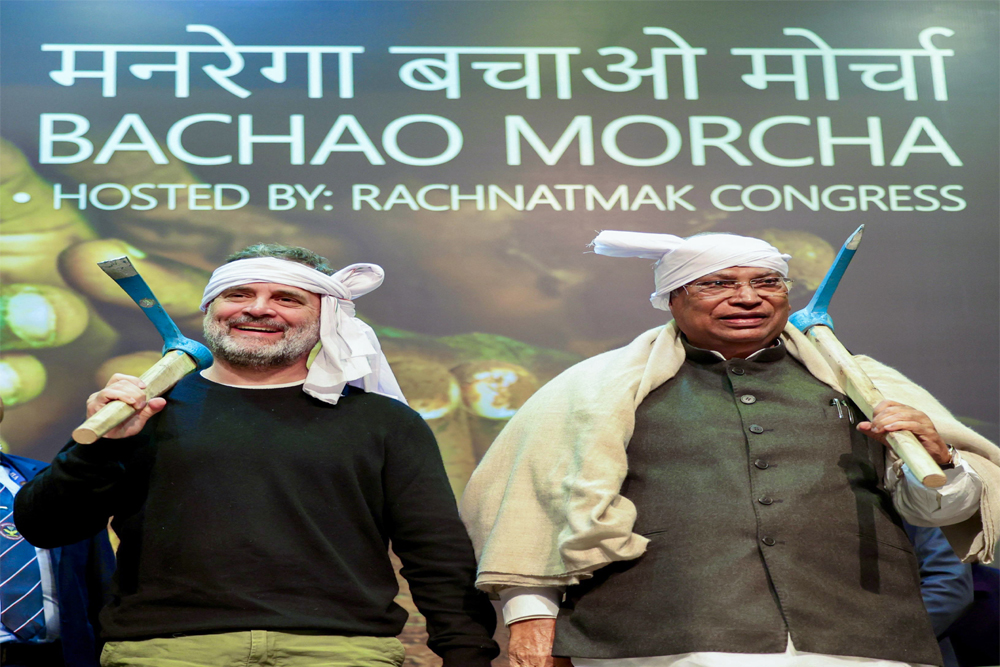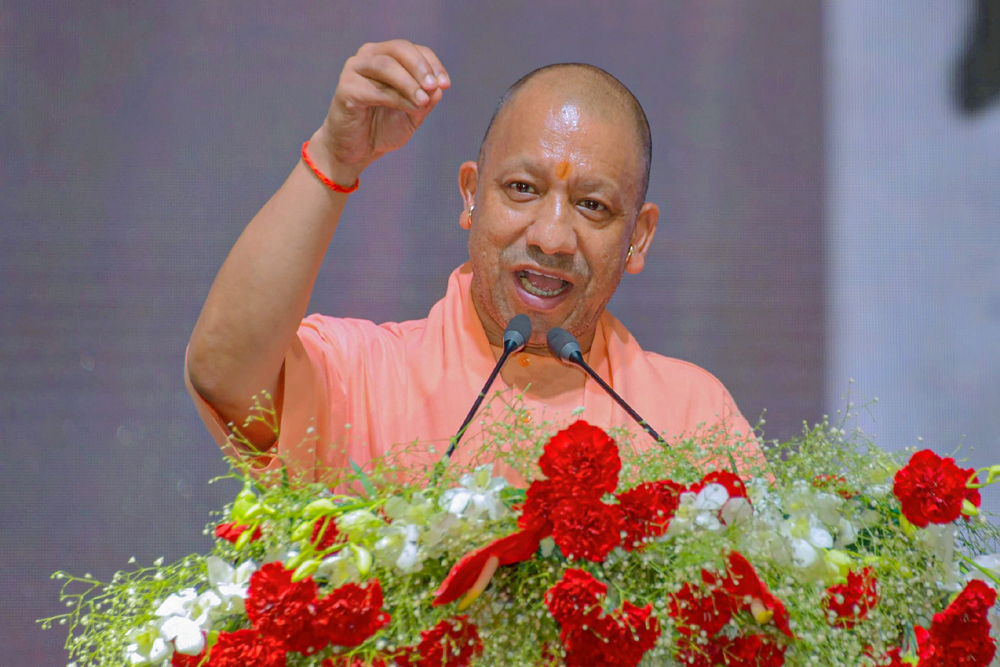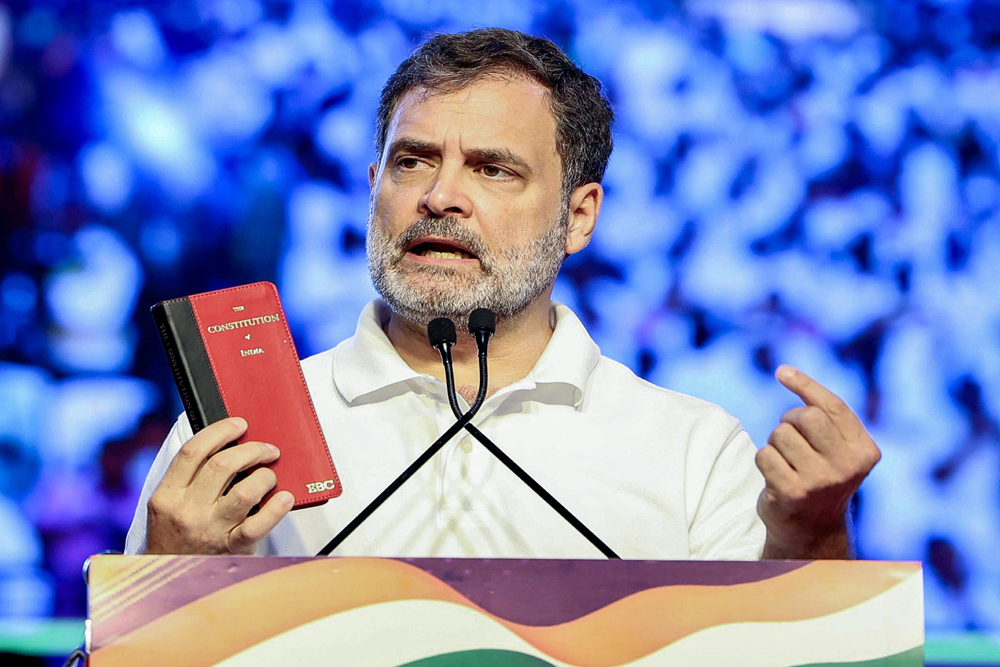स्वतंत्र भारत ने ज्यादातर समय इज़राइल से एक दूरी रखी। इतना नाता जरूर रखा कि आपात स्थिति में मदद मिल जाए और उसकी इमेज पर भी असर नहीं पड़े। भारत ने 1950 में इज़राइल को मान्यता दी थी लेकिन जवाहरलाल नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय अरब दुनिया के साथ एकजुटता थी। फ़िलिस्तीनी मुद्दा महज़ नैतिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि रणनीतिक था। भारत के लिए यह तब फायदेमंद था कि उसे औपनिवेशिक विरोधी और फ़िलिस्तीन-समर्थक के रूप में देखा जाए। ताकि अरब तेल तक पहुंच बनी रहे और अरब देश कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में नहीं झुके।
इज़राइल, तब, एक मौन, शांत मित्र था। ऐसा जिसे सार्वजनिक मंच पर नहीं बुलाया जाता था। पर संजीदा, संकट में भरोसेमंद, और सार्वजनिक नजरों से ओझल।
यह संतुलन शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी चलता रहा। 1992 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने औपचारिक राजनयिक रिश्तों की शुरुआत की। हथियारों के अनुबंध हुए—रडार, यूएवी, मिसाइल सिस्टम—लेकिन वह रिश्ता भी सार्वजनिक प्रदर्शन से दूर था। रणनीति वही रही: पर्दे के पीछे इज़राइल से सहयोग, लेकिन सार्वजनिक रूप से फ़िलिस्तीनी समर्थन का प्रदर्शन और मध्य पूर्व के अन्य देशों से आर्थिक रिश्ते बनाए रखना।
असल में यह रिश्ता, “राज़” कभी राज़ था ही नहीं। 1962 के चीन युद्ध में, और 1965 व 1971 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में इज़राइल ने भारत को हथियार दिए थे। 1968 में जब भारत की खुफिया एजेंसी ‘रॉ’ बनी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसके प्रमुख आर.एन. काव को इज़राइल की ‘मोसाद’ से रिश्ते बनाने का काम सौंपा। 1999 के कारगिल युद्ध में—जब परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका क्योंकि भारत पर पाबंदियां लगाए हुए था तब इज़राइल ने भाषण नहीं दिया लेकिन वह दिया जो दिल्ली को चाहिए था: अचूक निशाने के प्रिसीजन बम, यूएवी और निगरानी उपकरण। यह पैकेज—बिना राजनीतिक हल्ले के, बिना डिलीवरी में देरी के था। इज़राइल वह सोर्स था जहां से भारत वह तकनीक ले सकता था जिसे बाकी देश बेचने में हिचकते थे।
फिर भी, दशकों तक भारत ने इस रिश्ते को नपे-तुले ढंग से पेश किया। सार्वजनिक बयान फ़िलिस्तीन-समर्थक जबकि निजी सहयोग इज़राइल के साथ। लेकिन 2008 के मुंबई आतंकी हमलों ने भारत में इज़राइल को देखने का नजरिया बदल दिया। हमलों के बाद सुरक्षा विशेषज्ञ खुलेआम कहने लगे कि भारत को “इज़राइली तरीका” अपनाना चाहिए—निर्णायक, बिन माफ़ी, बिन रोक-टोक। लेकिन इस राजनीतिक नज़दीकी की जड़ें इससे भी पुरानी थीं। भाजपा ने मुंबई हमलों से बहुत पहले ही इजराइल से खुले रिश्ते का समर्थन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में रिश्ते ज़्यादा खुले तौर पर बढ़े। सन् 2000 में लालकृष्ण आडवाणी पहले भारतीय गृह मंत्री थे जो इज़राइल गए। एक साल बाद विदेश मंत्री जसवंत सिंह पहुंचे, और 2003 में एरियल शेरॉन दिल्ली आए—पहली बार कोई इज़राइली प्रधानमंत्री भारत आया। इससे दोनों देशों की साझेदारी परदे से बाहर आई।
असली बदलाव 2017 में हुआ, जब नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जो इज़राइल गए लेकिन फ़िलिस्तीन क्षेत्र नहीं गए। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रिश्ता व्यक्तिगत रंग भी ले गया—दो राष्ट्रवादी नेता, “बिना माफ़ी के आतंकवाद-विरोध” की साझा कथा में खड़े। मोदी के दौर में रक्षा सौदे—जो पहले ही अरबों डॉलर के थे—संयुक्त मिसाइल रक्षा परियोजनाओं, सीमा निगरानी प्रणालियों और हथियारबंद ड्रोन तक फैल गए।
फिर आया 7 अक्तूबर 2023। और हमास के हमले के कुछ घंटों में ही मोदी ने इज़राइल के प्रति एकजुटता का ट्वीट किया—हमास का नाम लेकर, और दशकों पुराना संतुलन तोड़ते हुए। उन्होने फ़िलिस्तीनी राज्य की बात को छोड़ दी। उसके बाद के महीनों में भारत ने चुपचाप इज़राइली हथियार प्रणालियों के पुर्जे भेजे, खुफिया साझेदारी बढ़ाई, और ‘आयरन डोम’ जैसी रक्षा प्रणाली का अध्ययन तेज हुआ।
इसी पृष्ठभूमि में, पिछले हफ़्ते चुनिंदा भारतीय पत्रकारों का एक दल इज़राइल ले जाया गया। उन्हें हमास के हमलों से प्रभावित जगहें दिखाईं गईं, टूटे घरों के बीच घुमाया गया, और हैफ़ा युद्ध स्मारक ले जाया गया—जहां 1918 की लड़ाई में मारे गए भारतीय सैनिक दफ़न हैं। आख़िरी दिन, उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की, जिन्होंने “ग़ाज़ा पर नियंत्रण लेकिन कब्ज़ा नहीं” का अपना प्लान बताया। उन्होने याद दिलाया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इज़राइली हथियार इस्तेमाल किए थे। तब यह नहीं बताया गया कि इज़राइल की सुरक्षा कैबिनेट ने अभी-अभी ग़ाज़ा के सबसे बड़े शहर पर ज़मीनी हमले की मंज़ूरी दी है—एक ऐसा कदम जो लगभग दस लाख फ़िलिस्तीनियों का भविष्य तय करेगा और जिसने पहले से ही वैश्विक आलोचना भड़का दी थी।
यह यात्रा इत्तफ़ाक नहीं थी। आज का इज़राइल कूटनीतिक रूप से पहले से ज़्यादा अकेला है—ब्रिटेन, फ़्रांस, कनाडा और यूरोप के कई हिस्सों ने ग़ाज़ा हमलों की निंदा की है; वॉशिंगटन का समर्थन घरेलू विरोध और संसदीय दबाव के बीच आ रहा है। वहा भी डोनाल्ड ट्रंप के दायरे के बाहर, खुले समर्थन वाले नेता अब कम हैं।
ऐसे माहौल में, भारत के साथ साझेदारी, इज़राइल के लिए जीवनरेखा है। 2018-2022 के बीच, इज़राइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था—कुल आयात का 11 प्रतिशत। 30 से अधिक कृषि “उत्कृष्टता केंद्र” इज़राइली जल और खेती तकनीक पर चलते हैं। साइबर डिफेंस और सीमा सुरक्षा में इज़राइली प्रणालियां इतनी गहराई से शामिल हैं कि अधिकारी निजी तौर पर कहते हैं—“इन्हें तुरंत बदला नहीं जा सकता।”
भारत के लिए भी, यह साझेदारी कथा-निर्माण का खेल है—“सर्जिकल स्ट्राइक” से “विकसित भारत” और “ऑपरेशन सिंदूर” तक। इज़राइल, अपने सबसे बड़े पीआर संकट में, इस हकीकत को जानता है। इसलिए उसे भारत में भी अपना नैरेटिव चाहिए।
पर भारत में वैसे ही इजराइल की ब्रांडिग जबरदस्त है। इससे प्रधानमंत्री मोदी की छवि को भी बल मिलता है – एक ऐसे समय में जब अमेरिका की टैरिफ मार को भारत झेल रहा है। चीन से रिश्तों में अनिश्चितता है, और ट्रंप प्रशासन फिर से पाकिस्तान के जनरल से नज़दीकियां बढ़ा रहा है। इस नए सिनेरियों में, इज़राइल एक साझेदार है और एक राजनीतिक प्रतीक भी। खासकक हाई-टेक हथियारों का भरोसेमंद सोर्स, आतंकवाद-विरोधी सहयोगी, और ऐसा देश जिसकी नज़दीकी सुरक्षा व ताकत का मजबूत संकेत देती है। बावजूद इसके इज़राइल की कथा में खुद को सहयोगी बनाकर, भारत खुद एक ऐसे संघर्ष में एक पक्ष बना है जिसका कोई साफ़ अंत नहीं है।
हालांकि यह रिश्ता महज़ युद्ध में बना गठजोड़ नहीं है, यह मोदी और नेतन्याहू की निजी सहजता में जुड़ा हुआ है। इसकी केमेस्ट्री से रिश्ते मुखर और ज़्यादा फ़ोटो-फ्रेंडली बनते है।
सवाल है यदि नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो गए, उनका उत्तराधिकारी वैश्विक दबाव में झुकता है, या ग़ाज़ा पर इज़राइल को प्रतिबंध झेलना पड़े तब उस माहौल में क्या होगा? या जब मोदी का कार्यकाल खत्म होगा, क्या उनके उत्तराधिकारी रिश्तों की निकटता को रणनीतिक संपत्ति मानेंगे या एक विरासत में मिली परेशानी?
खतरा यह है कि व्यक्तिगत निकटता और युद्धकालीन एकजुटता पर बना रिश्ता, भविष्य के नेताओं के लिए आसान नहीं हुआ करता। चाहकर भी आसानी से बदल नहीं जा सकता। इसलिए अंहम सवाल यह है कि तब दोनों देशों के रिश्तों में रणनीतिक दूरदृष्टि कितनी प्रभावी होगी या दिल्ली की आवाज़ किसी और की पटकथा में बस एक गूंज बनकर रह गई?